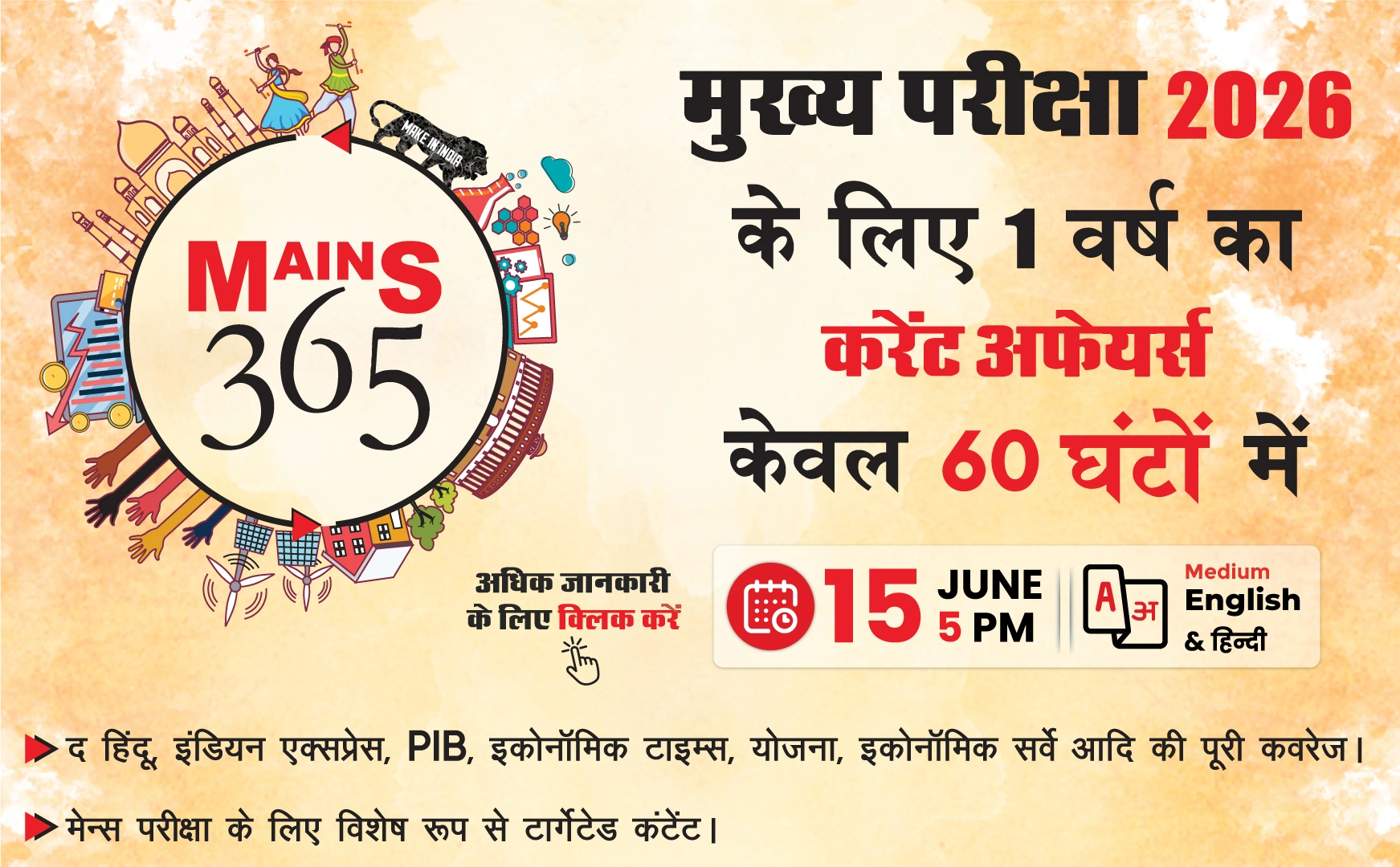औद्योगिक आधुनिकता का ऐतिहासिक संदर्भ
औद्योगिक क्रांति से लेकर आधुनिक समय तक औद्योगिक शक्ति का विकास परिशुद्ध विनिर्माण पर आधारित है। प्रमुख ऐतिहासिक प्रगतियों में शामिल हैं:
- ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति से कपास मिलों और मशीन उपकरणों में प्रगति हुई ।
- जॉन विल्किंसन की बोरिंग मिल और हेनरी माउडस्ले की स्क्रू-कटिंग लेथ जैसी महत्वपूर्ण नवीनताएं।
- जर्मनी में पॉलिटेक्निक संस्थानों और व्यावसायिक संघों का एकीकरण अपने औद्योगिक ढांचे में शामिल करना।
- अमेरिका द्वारा अमेरिकी विनिर्माण प्रणाली का विकास तथा विनिमेय भागों का विस्तार।
- जापान का 1945 के बाद का सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण संयोजन काइज़ेन और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट (टीक्यूएम) जैसी लीन उत्पादन तकनीकों के साथ ।
- 1978 के बाद चीन में परिशुद्धता इंजीनियरिंग पर ध्यान केन्द्रित करने से मशीन टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स और अर्धचालकों में वृद्धि को बढ़ावा मिला ।
भारत का अलग रास्ता
औद्योगीकरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण विशिष्ट रहा है, जिसकी विशेषता यह है:
- स्वतंत्रता के बाद उदारीकरण ने औद्योगिक क्षमताओं को सक्रिय रूप से गहरा नहीं किया।
- मजबूत औद्योगिक नीति के बजाय सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था पर समय से पहले जोर दिया जाना।
- 2011 में राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि विनिर्माण क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा 2022 तक 16% से बढ़ाकर 25% किया जाए, जो 2025 तक लगभग 17% ही रहेगा।
परिशुद्ध विनिर्माण में संरचनात्मक चुनौतियाँ
भारत को परिशुद्ध विनिर्माण को आगे बढ़ाने में कई संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है:
- व्यावसायिक प्रशिक्षण: भारत के केवल 4.1% कार्यबल के पास औपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण है, जबकि जर्मनी और दक्षिण कोरिया में यह आंकड़ा 70% से अधिक है।
- फर्म का आकार: 'बौनी फर्मों' का प्रचलन जो विस्तार नहीं करती हैं, तथा मध्यम आकार के आपूर्तिकर्ताओं की एक विरल मध्य परत होती है।
- श्रम विनियम: अपूर्ण एवं असमान श्रम संहिता समेकन, जिसके लिए एक व्यापक रोजगार संहिता की आवश्यकता है।
- अवसंरचना: उच्च रसद लागत और अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति के कारण उच्च औद्योगिक टैरिफ के साथ सटीक उद्योग प्रभावित हो रहे हैं।
- गुणवत्ता विनिर्माण: महत्वपूर्ण मशीन उपकरणों के लिए आयात पर निर्भरता और माप-पद्धति में अपर्याप्त घरेलू क्षमताएं।
- गुणवत्ता प्रबंधन: प्रक्रिया प्रबंधन और सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण विधियों को कम अपनाया जाना।
- अनुसंधान एवं विकास निवेश: अनुसंधान एवं विकास पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% है, तथा शिक्षा-उद्योग सहयोग कमजोर है।
निष्कर्ष
वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी बनने की भारत की आकांक्षा के लिए इन चुनौतियों पर विजय पाना आवश्यक है। आर्थिक संप्रभुता और प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करने के लिए कौशल अंतराल, कंपनी विस्तार, श्रम कानूनों, बुनियादी ढाँचे, गुणवत्ता पहलों और अनुसंधान एवं विकास निवेश को संबोधित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।