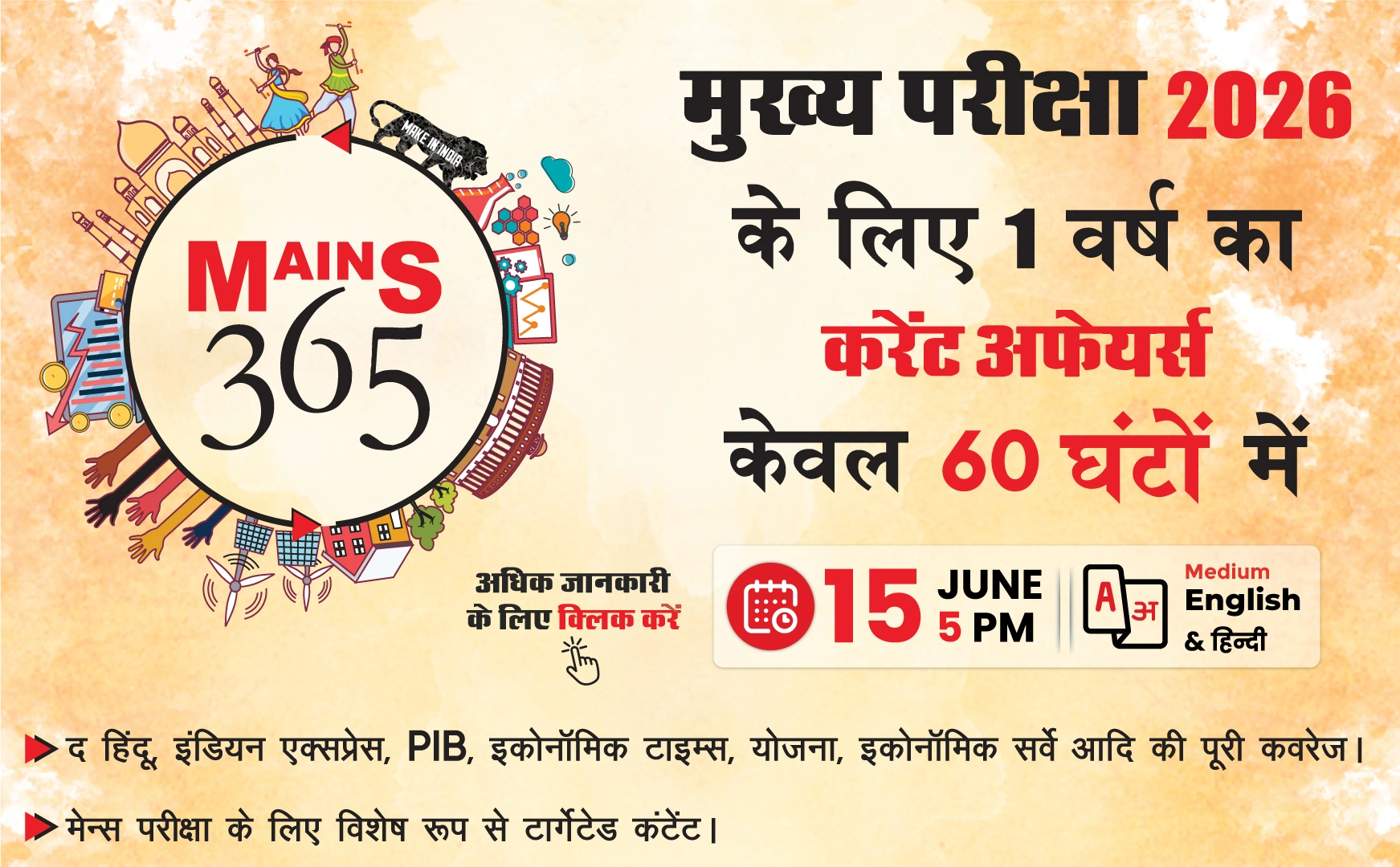भारत में शहरी प्रवास: अवसर और चुनौतियाँ
भारतीय शहरों की भूमिका
भारतीय शहर ऐतिहासिक रूप से अवसरों के केंद्र रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से लाखों लोगों को आकर्षित करते रहे हैं। मुंबई की कपड़ा मिलों से लेकर बेंगलुरु के टेक पार्कों तक, प्रवासियों ने भारत के शहरी परिवर्तन को गति दी है और देश के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई है।
आंतरिक प्रवास का स्तर
- 2011 की जनगणना के अनुसार, 450 मिलियन से अधिक आंतरिक प्रवासी थे, जो कुल जनसंख्या का 37% हैं।
- एक दशक पहले की 30% की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि।
- ग्रामीण से शहरी प्रवास एक प्रमुख घटक है; कुछ राज्यों में शहरी आबादी में 30% की वृद्धि देखी गई है।
अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
- प्रवासी अनौपचारिक और औपचारिक दोनों क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 45% का योगदान देती है।
- शहरी क्षेत्रों में उत्पादकता और मजदूरी अधिक होती है तथा शहरी मजदूरी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में लगभग दोगुनी होती है।
प्रवासन की चुनौतियाँ
औपचारिक प्रतिबंधों के अभाव के बावजूद, भय-आधारित शासन प्रवासन में बाधाएँ पैदा करता है। इन मुद्दों में शामिल हैं:
- प्रशासनिक और सामाजिक बाधाओं में वृद्धि।
- विशिष्ट समूहों को लक्ष्य करके की जाने वाली राजनीतिक बयानबाजी से बेचैनी बढ़ती है।
- 2020 के कोविड-19 लॉकडाउन ने शहरी प्रवासियों की कमजोरियों को उजागर किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया।
भय-आधारित शासन के परिणाम
- प्रवासी श्रम पर निर्भर क्षेत्रों में व्यवधान।
- शहरी प्रशासन में विश्वास का दीर्घकालिक क्षरण।
- शहरों में सांस्कृतिक विविधता और विश्वव्यापीकरण का नुकसान।
शहरी क्षेत्रों में विश्वास बहाल करना
- विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा सामाजिक लाभों की पोर्टेबिलिटी पर जोर दिया गया है।
- नौकरशाही बाधाओं को दूर करने और विनियमों में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है।
- शहरी बुनियादी ढांचे के लिए अगले 15 वर्षों में 840 बिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता है।
निष्कर्ष
प्रवासन शहरी जीवन शक्ति को बढ़ाता है और इसे समस्या के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। समृद्धि बनाए रखने के लिए, भारतीय शहरों को विश्वास का वाहक बनना होगा। भय अल्पकालिक राजनीतिक लाभ तो प्रदान कर सकता है, लेकिन दीर्घकालिक आर्थिक नींव को कमजोर कर सकता है।