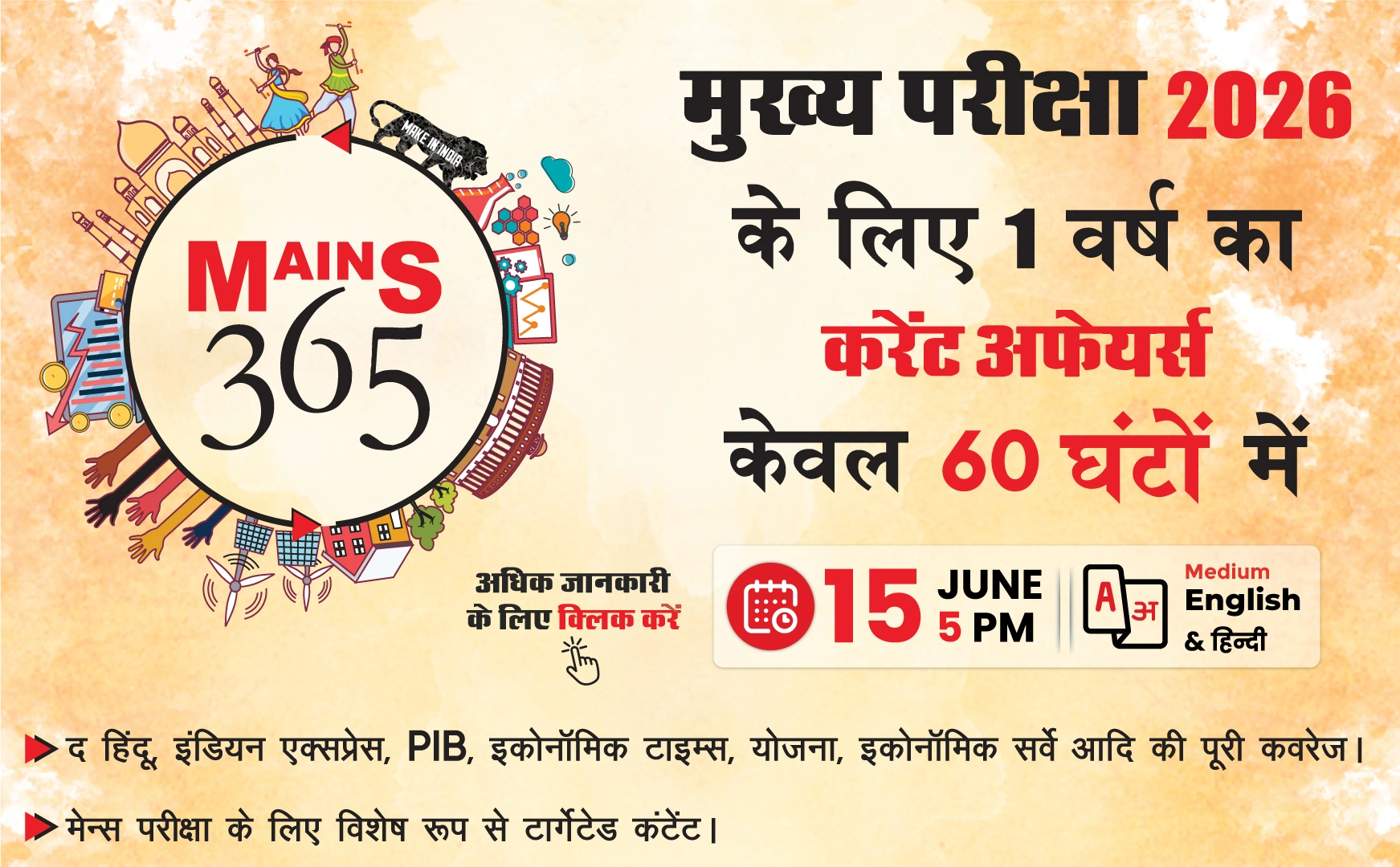हरित आर्थिक ग्रामीण-शहरी विभाजन
भारत में हरित अर्थव्यवस्था शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाती है। शहरी क्षेत्रों को हरित निवेश, इलेक्ट्रिक वाहन अवसंरचना, सौर छतों और हरित रोज़गारों से लाभ होता है। इसके विपरीत, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा, कुशल सिंचाई और टिकाऊ आजीविका तक पहुँच का अभाव है, साथ ही तकनीक अपनाने की गति भी धीमी है।
भारत की जैव-अर्थव्यवस्था वृद्धि
भारत की जैव-अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2014 में 10 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में 165.7 अरब डॉलर हो गई है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.25% है। यह वृद्धि 10,000 से अधिक जैव-अर्थव्यवस्था स्टार्टअप्स द्वारा संचालित है। प्रमुख योगदानकर्ताओं में शामिल हैं:
- औद्योगिक जैव अर्थव्यवस्था (जैव ईंधन और जैव प्लास्टिक) - 47%
- फार्मास्यूटिकल्स - 35%
- अनुसंधान और IT जैसे उभरते क्षेत्र
प्रमुख उपलब्धियों में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करना तथा मात्रा के आधार पर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक बनना शामिल है।
रोजगार सृजन और आर्थिक प्रभाव
- 2030 तक 35 मिलियन नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है।
- ग्रामीण उपभोक्ता व्यय शहरी की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रहा है, जो ग्रामीण क्रय क्षमता में सुधार का संकेत है।
हरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की चुनौतियाँ
वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद, भारत ऊर्जा सुरक्षा और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए हरित अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देता है। हालाँकि, चुनौतियाँ इस प्रकार हैं:
- जलवायु परिवर्तन मुद्रास्फीति और ग्रामीण जैव अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं।
- अवसंरचना, शहर-केन्द्रित एवं खंडित हैं।
- महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताएं, कुछ राज्य जैव अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान दे रहे हैं।
लैंगिक असमानता
- रूफटॉप सौर ऊर्जा क्षेत्र में महिलाओं के पास केवल 11% नौकरियां हैं।
- प्रमुख भूमिकाओं में कम प्रतिनिधित्व: परिचालन में 1%, निर्माण में 3%।
व्यापार-नापसंद और नीतिगत विचार
भारत को जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी देते हुए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर औद्योगिक विस्तार हरित प्रौद्योगिकी निवेश पर दबाव डाल रहा है। चुनौतियों में शामिल हैं:
- वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा निवेश का 85% उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में जाता है, जबकि केवल 15% भारत और विकासशील बाजारों में जाता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों और कमजोर समूहों पर असमानुपातिक प्रभाव का जोखिम।
क्षेत्र-विशिष्ट प्रभाव
- कृषि 58% ग्रामीण आजीविका का आधार है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है।
- खाद्य मील के कारण परिवहन क्षेत्र का कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है।
आगे की राह: एकीकृत परिदृश्य दृष्टिकोण
एक एकीकृत भू-दृश्य दृष्टिकोण पारिस्थितिक और मानवीय दोनों लाभों को बढ़ा सकता है। प्रमुख रणनीतियों में शामिल हैं:
- पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय प्राधिकारियों का लाभ उठाते हुए सहभागी योजना बनाना।
- लैंगिक मुख्यधारा के साथ चक्रीयता, हरित ऊर्जा और जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
- लक्षित राजकोषीय प्रोत्साहन, स्पष्ट प्रवर्तन भूमिकाएं, और स्थानीय क्षमता निर्माण।
यह दृष्टिकोण भारत को जलवायु और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है, जिससे विकास के नए इंजन और लचीलापन सामने आ सकते हैं।