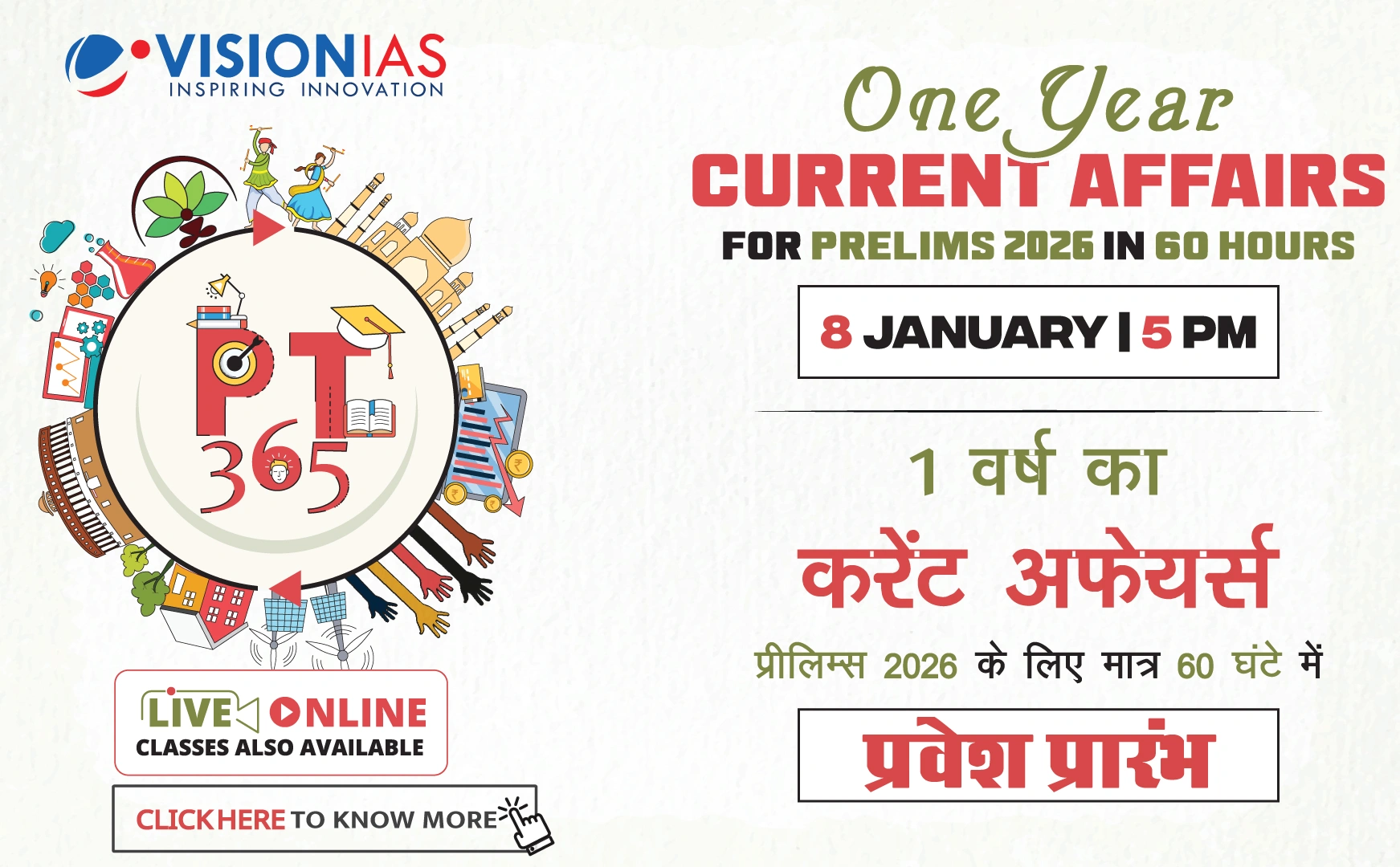भारत में समावेशी शिक्षा और निर्मित पर्यावरण
भारतीय शहरों के निर्मित परिवेश में, खासकर दिव्यांगजनों के लिए, अक्सर समावेशिता का अभाव होता है। इस स्थिति में सुधार के प्रयास में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के सहयोग से एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों और सुगम्यता की अवधारणा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना है।
उद्देश्य और महत्व
- समझौता ज्ञापन का उद्देश्य बच्चों को विकलांगता और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016 के बारे में शिक्षित करना है।
- समावेशन को न केवल एक नियामक आवश्यकता के रूप में देखा जाता है, बल्कि एक सांस्कृतिक मानदंड के रूप में भी देखा जाता है, जिसे छोटी उम्र से ही सिखाया और अपनाया जाना चाहिए।
- यह शैक्षिक सुधार विशेष रूप से वास्तुकला, इंजीनियरिंग और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है जो हमारे भौतिक पर्यावरण को आकार देते हैं।
सुगम्यता में वर्तमान चुनौतियां
- दिल्ली में पहुंच की कमी का उदाहरण दिया गया है, जहां 30% सरकारी भवनों में रैम्प की सुविधा नहीं है, 82% सार्वजनिक शौचालय पहुंच से बाहर हैं, तथा 94% स्वास्थ्य सुविधाएं विकलांग लोगों के लिए नहीं बनाई गई हैं।
- इंजीनियरिंग और वास्तुकला के पेशेवरों को अक्सर विकलांगता समावेशन के संबंध में अपर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त होता है।
- सुगम्यता को प्रायः एक बाद की बात समझा जाता है, जबकि अग्नि सुरक्षा को पाठ्यक्रम में अच्छी तरह से शामिल कर लिया गया है।
शैक्षिक अंतराल
- IIT दिल्ली में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में बी.टेक. तथा स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली में बी.आर्क. जैसे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में सुलभ प्रौद्योगिकी और समावेशी डिजाइन में आधारभूत प्रशिक्षण का अभाव है।
- इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण को अनिवार्य के बजाय वैकल्पिक माना जाता है, जो व्यापक प्रणालीगत परिवर्तन में बाधा डालता है।
कानूनी ढांचा और प्रवर्तन
- RPWD अधिनियम, 2016 और सामंजस्यपूर्ण दिशा-निर्देश, 2021 सुलभ बुनियादी ढांचे के लिए स्पष्ट दायित्व निर्धारित करते हैं।
- दिल्ली के UBBL में सुगम्यता संबंधी आवश्यकताएं तो शामिल हैं, लेकिन अक्सर प्रभावी प्रवर्तन तंत्र का अभाव होता है।
- कानूनी और दंडात्मक उपाय मौजूद हैं, जैसे कि RPWD अधिनियम और दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत जुर्माना, लेकिन व्यावहारिक प्रवर्तन कमजोर बना हुआ है।
शैक्षिक सुधार की आवश्यकता
- निपुण मल्होत्रा बनाम GNCTD जैसे न्यायालयीन मामलों ने सुगम्यता मानकों में प्रशिक्षण और शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
- एनसीईआरटी और NIOS के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का समझौता ज्ञापन उच्च शिक्षा में सुगम्यता को एकीकृत करने के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और वास्तुकला परिषद जैसी संस्थाओं को सुगम्यता को एक मुख्य डिजाइन क्षमता के रूप में शामिल करने की आवश्यकता है।
निष्कर्ष
सुगम्यता को एक बुनियादी स्वभाव के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, न कि अनुपालन के बोझ के रूप में। कानूनी उपायों के साथ-साथ शैक्षिक सुधार के बिना, निर्मित परिवेश में समावेशिता एक अधूरा लक्ष्य बना रहेगा। स्कूली पाठ्यक्रम में सुधार की पहल एक अधिक समावेशी समाज की दिशा में एक कदम है, लेकिन भारत में सुगम्यता को वास्तविक रूप से बदलने के लिए इसके साथ उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है।