ऊर्जा व पर्यावरण परिषद (CEEW) द्वारा किए गए एक अध्ययन में भारत के 734 जिलों में गर्मी के खतरे का आकलन किया गया। इस अध्ययन का शीर्षक है- ‘अत्यधिक गर्मी भारत को कैसे प्रभावित कर रही है: जिला-स्तरीय गर्मी के खतरे का आकलन।’
हीट रिस्क बनाम हीट वेव्स और हीट स्ट्रेस को समझना
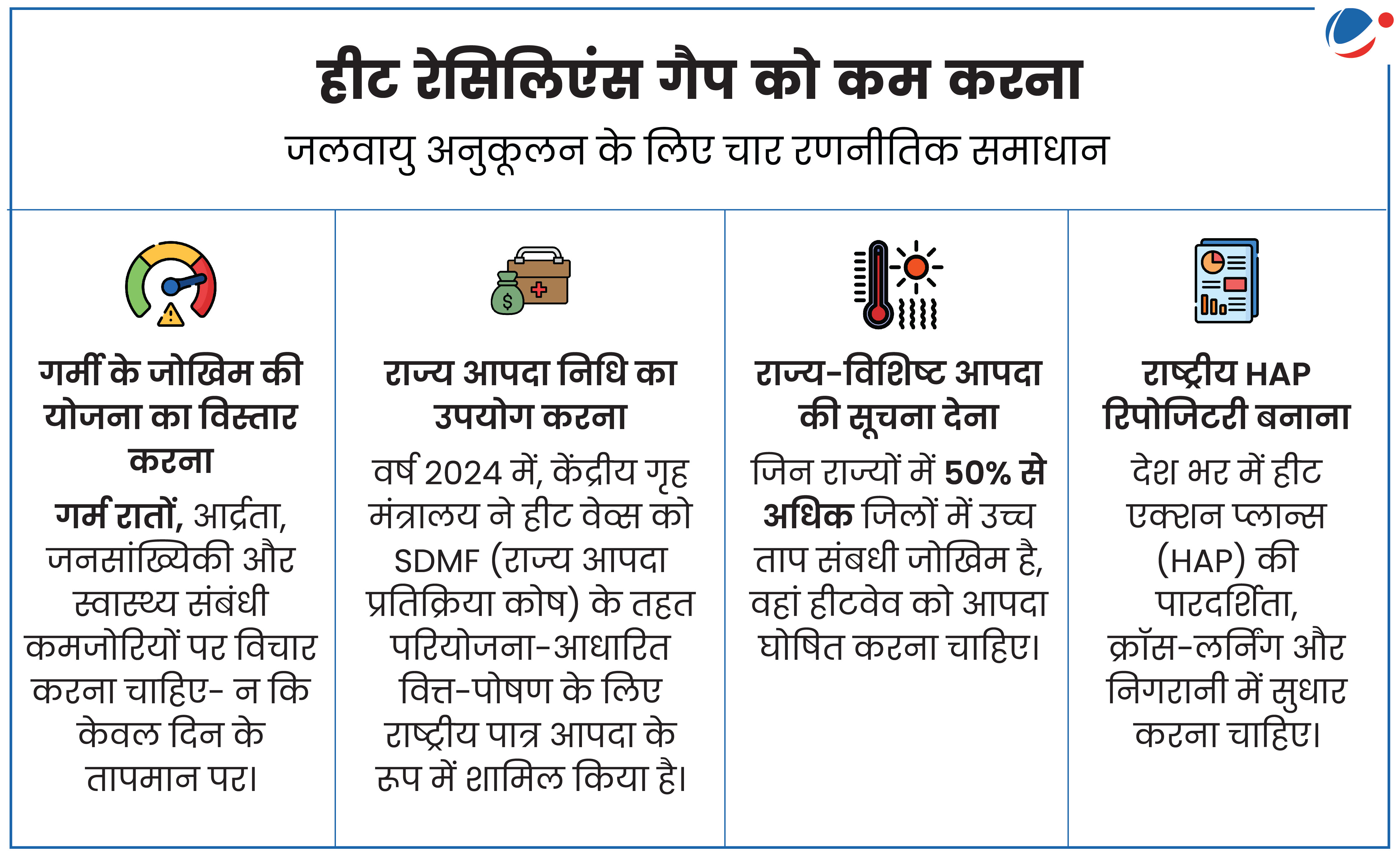
- हीट वेव्स: ये किसी विशिष्ट क्षेत्र (जैसे- मैदान, तटीय क्षेत्र, पहाड़ियां आदि) में असामान्य रूप से उच्च तापमान की दीर्घ अवधि को संदर्भित करती हैं।
- हीट स्ट्रेस: यह तब होता है, जब शरीर का तापमान 37°C से अधिक हो जाता है। इससे बेचैनी, ऐंठन और संभावित रूप से घातक हीट स्ट्रोक होता है।
- हीट रिस्क: यह अत्यधिक तापमान के संपर्क में आने के कारण गर्मी से संबंधित बीमारियों या मृत्यु की संभावना को संदर्भित करता है। यह निम्नलिखित पर निर्भर करता है:
- गर्मी की तीव्रता (आर्द्रता से और भी बढ़ गई);
- प्रत्यक्ष संपर्क में आने का जोखिम; तथा
- प्रभावित समुदायों की सुभेद्यता।
गर्मी के जोखिम को बढ़ाने वाले कारक
- गर्म रातों में वृद्धि (2012-22): बहुत गर्म रातों की आवृत्ति गर्म दिनों की तुलना में तेजी से बढ़ी है।
- यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि रात के समय तापमान अधिक होने से दिन की भीषण गर्मी के बाद शरीर को ठंडा होने में कठिनाई होती है, जिससे हीट स्ट्रोक की घटनाएं बढ़ जाती हैं।
- उत्तर भारत में आर्द्रता में वृद्धि: उत्तर भारत में आर्द्रता 1982-2011 के दौरान 30-40% थी। यह बढ़कर 2012-2022 के बीच 40-50% हो गई है। तापमान और आर्द्रता में इस वृद्धि के कारण पसीने के माध्यम से शरीर के ठंडा होने की क्षमता सीमित हो गई है और हीट स्ट्रेस बढ़ गया है।
- उच्च जनसंख्या घनत्व और तीव्र गति से शहरीकरण: मुंबई, दिल्ली, पुणे और गुरुग्राम जैसे शहरों में 'अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट' पैदा हुआ है।
- अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट: ऐसी घटना जहां कंक्रीट वाली अवसंरचना गर्मी को अवशोषित करती है और बनाए रखती है।



