यू.एन. ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) के अनुसार, प्रत्यर्पण (Extradition) का अर्थ है “किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को दूसरे देश को सौंपना, ताकि वहाँ उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सके।” हालांकि, इसमें एक शर्त यह है कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध प्रत्यर्पण योग्य अपराध (Extraditable offence) की श्रेणी में आता हो।
- प्रत्यर्पण योग्य अपराध वह होता है जो या तो किसी देश के साथ हुई प्रत्यर्पण संधि में उल्लिखित हो, या अगर कोई संधि नहीं हुई है, तो ऐसा अपराध जिसके लिए भारत या संबंधित देश में कम-से-कम 1 साल की सजा का प्रावधान हो।
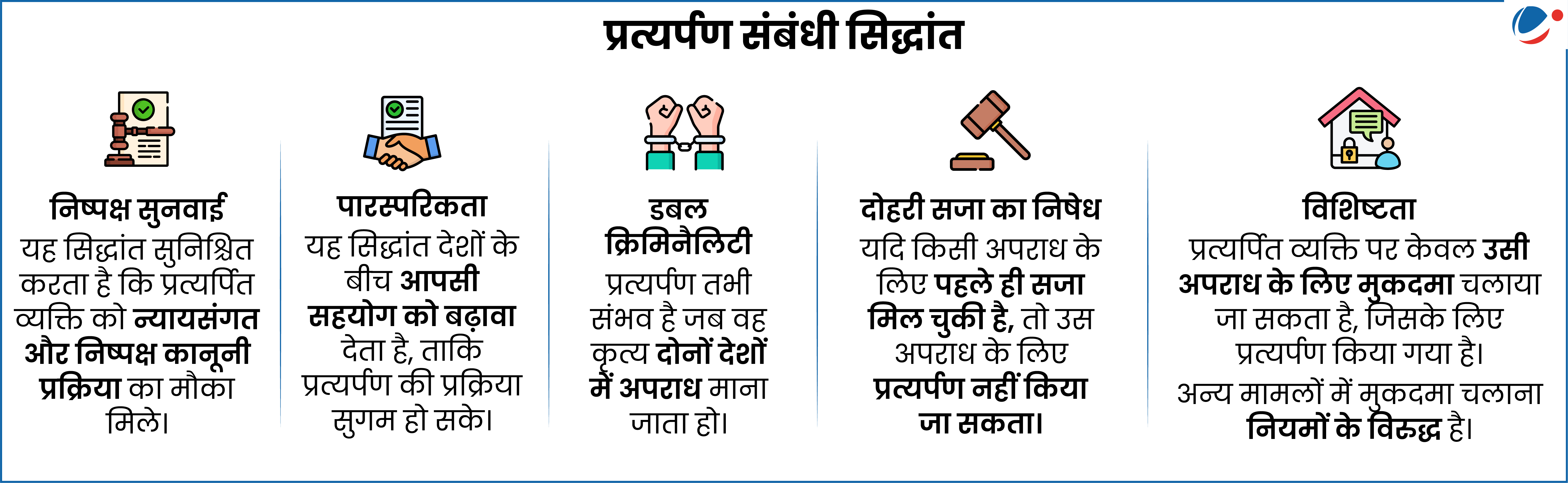
प्रत्यर्पण से जुड़े फ्रेमवर्क
- भारत में:
- प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 (1993 में पर्याप्त संशोधन): यह कानून भारत से विदेशों में अपराधियों को सौंपने और उन्हें विदेशों से भारत लाने के नियमों को निर्धारित करता है।
- विदेश मंत्रालय भारत में प्रत्यर्पण संबंधी मामलों के लिए नोडल प्राधिकरण है।
- भारत ने बांग्लादेश और अमेरिका सहित 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां की है।
- प्रत्यर्पण से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने की अंतिम शक्ति भारत सरकार के पास है, लेकिन सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
- प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 (1993 में पर्याप्त संशोधन): यह कानून भारत से विदेशों में अपराधियों को सौंपने और उन्हें विदेशों से भारत लाने के नियमों को निर्धारित करता है।
- प्रत्यर्पण से जुड़े मामलों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रावधान:
- प्रत्यर्पण पर संयुक्त राष्ट्र मॉडल संधि (1990),
- प्रत्यर्पण पर संयुक्त राष्ट्र मॉडल कानून (2004),
- सीमा-पारीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (2000), आदि।
प्रत्यर्पण कानून में चुनौतियां
|




