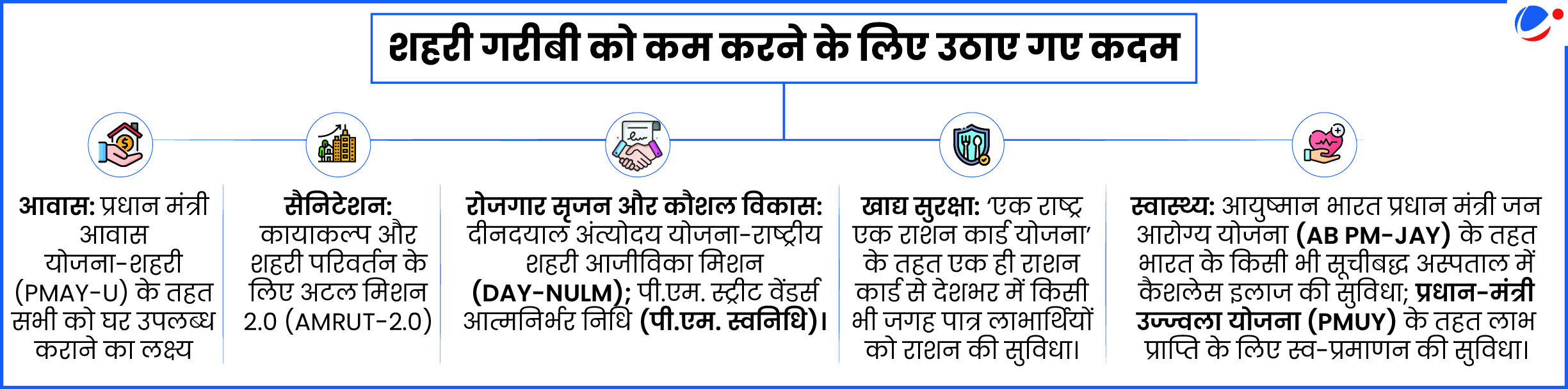ओडिशा सरकार की ‘सहयोग’ पहल के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
- शहरी गरीब समुदायों में पात्र लाभार्थियों की पहचान करना और उन्हें जन जागरूकता के माध्यम से उपयुक्त योजनाओं से जोड़ना,
- पात्र लाभार्थियों के घर तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाना, आदि।
भारत में शहरी गरीबी
- ग्रामीण गरीबी की तरह ही शहरी गरीबी भी रोजगार, भोजन, स्वास्थ्य-देखभाल सेवाएं और शिक्षा प्राप्ति में समस्याओं से जुड़ी हुई है। साथ ही, जिन समुदायों के बीच शहरी गरीब निवास करते हैं वहां भी उन्हें उपेक्षा का सामना करना पड़ता है।
- हाल में जारी विश्व बैंक की “पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ” रिपोर्ट के अनुसार, शहरी भारत में चरम गरीबी की दर 17.2% है, जबकि ग्रामीण भारत में यह मात्र 2.8% है।
शहरी गरीबी में जीवन अधिक चुनौतीपूर्ण क्यों है?
- अधिक दयनीय जीवन-यापन: शहरी गरीब बड़ी संख्या में झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। इन बस्तियों में शौचालय, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और वेंटिलेशन जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी होती है।
- शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य-देखभाल सेवा, शिक्षा, परिवहन और आवास महंगे होते हैं। ज्यादातर लोग इन सेवाओं को वहन करने में सक्षम नहीं होते हैं।
- कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में समस्या: पहचान पत्र या आवास प्रमाण पत्र नहीं होने से शहरों में रहने वाले प्रवासी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं।
- इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में मनरेगा जैसी आय समर्थन योजना भी नहीं चलाई जा रही है।
- असमानता: ग्रामीण गरीबी की तुलना में शहरी गरीबी तुरंत दिख जाती है क्योंकि शहरी गरीबों की आबादी घनी और झुग्गी बस्तियों में केंद्रित होती है। इससे गरीबों को अपनी गरीबी और सामाजिक उपेक्षा का अधिक एहसास होता है।
- उदाहरण: मुंबई की धारावी मलिन बस्ती के पास बनी लग्जरी और ऊंची इमारतें इस गहरी असमानता को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं।
- सामाजिक सहायता में कमी: ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सामुदायिक जीवन जीते हैं। इसके विपरीत, शहरों में मजबूत सामुदायिक संबंध और पारंपरिक सामाजिक नेटवर्क नहीं होते। इससे अकेलेपन और मानसिक बीमारियों का खतरा बना रहता है।
- उपेक्षित नगरीकरण: प्रायः शहरी योजना-निर्माण में झुग्गियों जैसी अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाली आबादी की उपेक्षा कर दी जाती है।