परिचय
1960 के दशक के मध्य में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारत की स्वतंत्रता के बाद के विकास के लिए एक स्वदेशी वैचारिक ढांचा प्रस्तुत किया, जिसे एकात्म मानववाद (एकात्म मानव दर्शन) कहा गया। जैसे-जैसे हम आधुनिक विश्व की जटिलताओं से गुजरते हैं, एकात्म मानववाद का दर्शन एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करता है, जो हमें एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण में मानवीय गरिमा, सद्भाव और एकजुटता के आंतरिक मूल्य की याद दिलाता है।
एकात्म मानववाद दर्शन के बारे में
- एकात्म मानववाद का लक्ष्य व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं को संतुलित करते हुए प्रत्येक मनुष्य के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है।
- यह मानव जीवन के आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के एकीकरण पर जोर देता है, जिसका उद्देश्य एक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करना है।
- एकात्म मानववाद के केंद्र में पुरुषार्थ की अवधारणा निहित है। इसमें मानव अस्तित्व के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र को निर्धारित करने वाले चार मूलभूत उद्देश्य हैं।
- धर्म (धार्मिकता), अर्थ (धन/ समृद्धि), काम (सुख/ इच्छा) और मोक्ष (मुक्ति)।
- 'एकात्म मानववाद' का सिद्धांत इस सोच से उत्पन्न हुआ कि स्वतंत्र भारत को पश्चिमी विचारधाराओं की बजाय भारत की अपनी परंपराओं और मूल्यों पर आधारित विचारों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।
- प. दीनदयाल उपाध्याय ने अत्यधिक पूंजीवादी व्यक्तिवाद और कठोर मार्क्सवादी समाजवाद के दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया।
- एकात्म मानववाद का दर्शन निम्नलिखित तीन सिद्धांतों पर आधारित है:
- समष्टि की प्रधानता, न कि उसके किसी भाग की;
- धर्म की सर्वोच्चता; और
- समाज की स्वायत्तता।
समकालीन समय में एकात्म मानववाद के मूल सिद्धांत
- सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (भारतीयता): एकात्म मानववाद विकास का एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो स्वदेशी ज्ञान, परंपराओं और जीवनशैली का सम्मान करता है और साथ ही आधुनिक प्रगति को भी आत्मसात करता है।
- सामाजिक एकीकरण और सद्भाव: यह सामाजिक सद्भाव और जातिगत भेदभाव के उन्मूलन का आह्वान करता है, ताकि समानता और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना की जा सके।
- अंत्योदय (अंतिम व्यक्ति का उत्थान): इसका तर्क है कि आर्थिक नीतियों का लक्ष्य केवल औद्योगिक या शहरी विकास नहीं, बल्कि समाज के सबसे गरीब वर्गों का पहले उत्थान होना चाहिए।
- 'सभी के लिए शिक्षा' और 'हर हाथ को काम, हर खेत को पानी' जैसे विचार उनके आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा में समाहित थे।
- नैतिक शासन: आदर्श राज्य (धर्म राज्य) की अवधारणा केवल धार्मिक अनुष्ठानों की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह धार्मिकता, नैतिक मूल्यों और पारदर्शी शासन को भी दर्शाती है।
- विकेंद्रीकरण: इस दर्शन में एक आत्मनिर्भर ग्राम-आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया गया है। यह समुदायों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और संसाधनों के आधार पर अपने स्वयं के विकास का प्रबंधन करने की अनुमति देता है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में (1916-1968)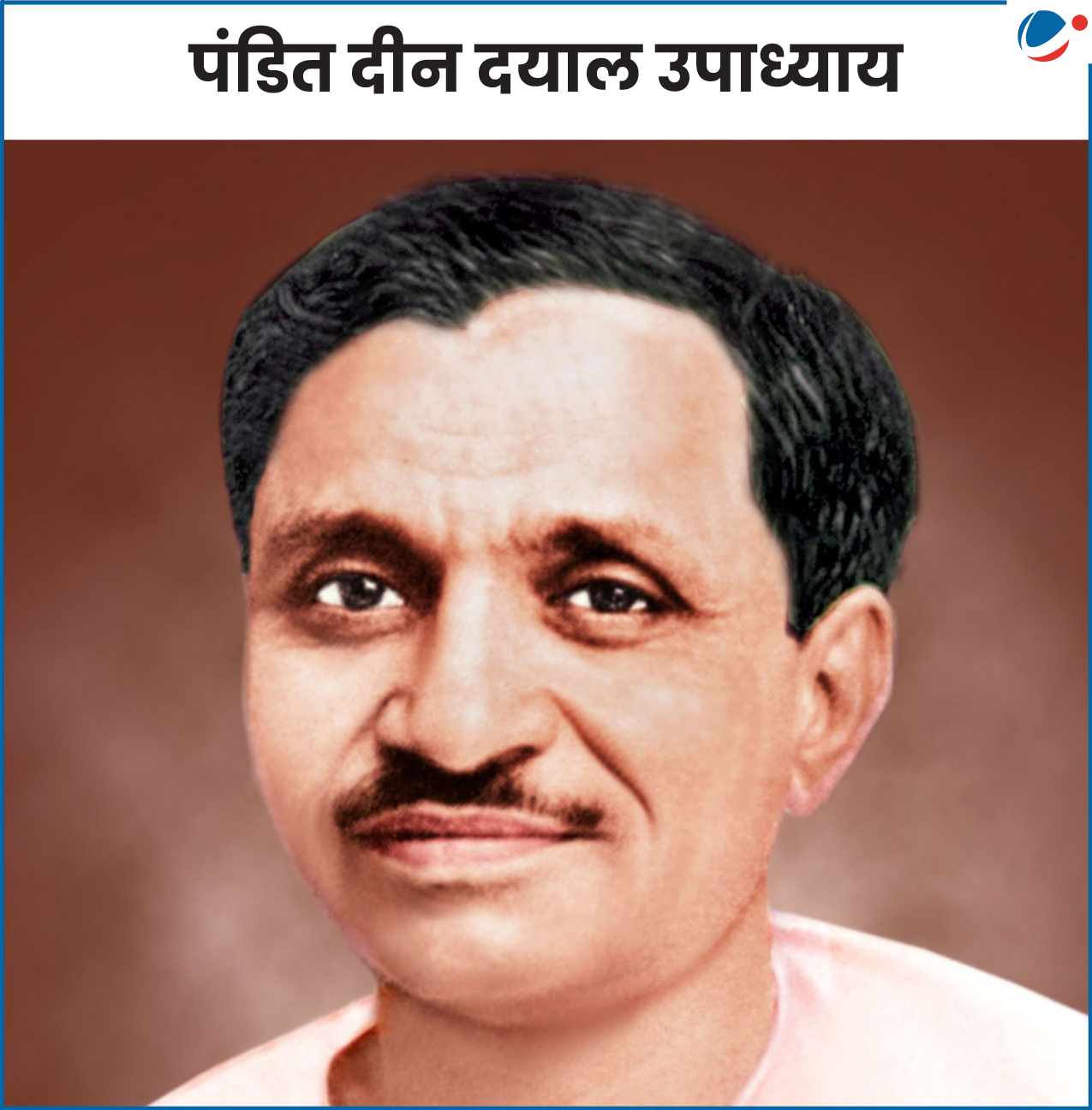
|




