सुर्ख़ियों में क्यों?
25 जून, 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, जो 21 मार्च, 1977 तक प्रभावी रहा था। इस वर्ष (2025) इस घटना को 50 साल पूरे हुए हैं।
1975 में आपातकाल क्यों लगाया गया था?
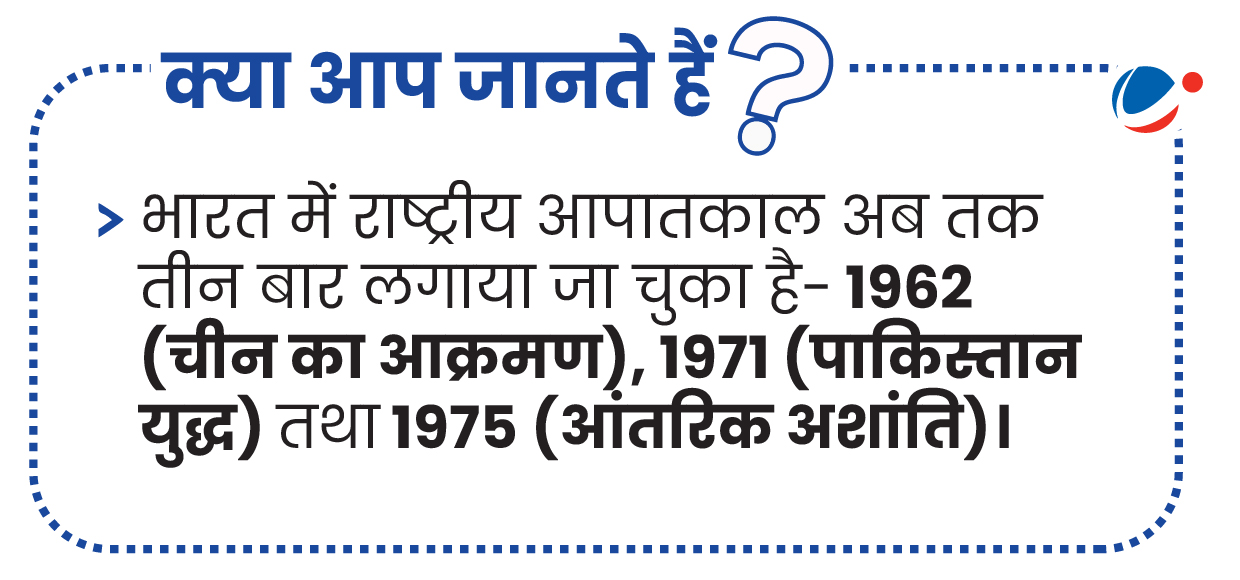
- सामाजिक अशांति: उस समय देश में सरकार के खिलाफ व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन, हड़तालें और आंदोलन हो रहे थे। इनमें जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ जेपी आंदोलन विशेष था। इस आंदोलन ने इंदिरा गांधी की सरकार पर गंभीर सवाल उठाए थे। इन सब के चलते सरकार ने दावा किया कि देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपातकाल लगाना जरूरी है।
- 1971 के युद्ध के बाद आर्थिक संकट: युद्ध के बाद देश गंभीर आर्थिक समस्याओं, जैसे- महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक ठहराव से जूझ रहा था। वैश्विक तेल संकट ने इस स्थिति को और बिगाड़ दिया।
- राजनीतिक कारण: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण' वाद में इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया। साथ ही, उन पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप भी लगा था। न्यायालय के इस फैसले और बढ़ती राजनीतिक अशांति के चलते इंदिरा गांधी ने सत्ता को अपने हाथ में रखने के उद्देश्य से आपातकाल की घोषणा कर दी।
आपातकाल के दौरान हुए प्रमुख संविधान संशोधन
- 38वां संशोधन (1975): इस संशोधन ने राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया। इसमें उपबंध किया गया कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय 'अंतिम एवं निर्णायक' होगा।
- 39वां संशोधन (1975): इसने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और लोक सभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों को तय करने के तरीके में बदलाव किया।
- अब ये विवाद संसद द्वारा निर्धारित किसी प्राधिकरण द्वारा तय किए जाने थे। इसका अर्थ था कि इन पदों को न्यायपालिका के न्यायिक दायरे से प्रभावी ढंग से बाहर कर दिया गया।
- 42वां संशोधन (1976): इसे 'लघु संविधान' भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा संविधान में कई बड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे:
- अनुच्छेद 31C के तहत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता दी गई।
- सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स की शक्तियों को कई तरह से कम किया गया:
- संविधान में अनुच्छेद 32A जोड़ा गया, जिसने सुप्रीम कोर्ट को राज्य के कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार करने की शक्ति से वंचित कर दिया। (हालांकि, इसे 43वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया था)
- अनुच्छेद 131A और 226A के तहत हाई कोर्ट्स को केंद्र सरकार के कानूनों की समीक्षा से वंचित किया गया था।
- लोक सभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था।
- इसने संसद को संविधान में संशोधन करने की लगभग असीमित शक्ति दे दी। इसके लिए अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 शामिल किए गए थे।
- आपातकाल के दौरान, नागरिकों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था उदाहरण के लिए- ADM जबलपुर वाद। मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (MISA) जैसे कानूनों के तहत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई थी।
आपातकाल के बाद सुधार
- शाह आयोग: मई 1977 में शाह आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का मुख्य कार्य आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच करना था। इनमें जबरन बंध्याकरण, सरकारी कर्मचारियों को ज़बरदस्ती रिटायर करना, न्यायालय व संसद पर विविध निषेध आदि सत्ता दुरुपयोग शामिल थे।
- आंतरिक आपातकाल के बाद 44वां संविधान संशोधन अधिनियम (1978):
- अनुच्छेद 352 में संशोधन (आपातकाल की घोषणा से संबंधित):
- आपातकाल लगाने के पुराने आधार "आंतरिक अशांति" को बदलकर व्यापक व स्पष्ट शब्द "सशस्त्र विद्रोह" किया गया। यह बदलाव इसलिए किया गया, ताकि "आंतरिक अशांति" जैसी अस्पष्ट अर्थ वाली शब्दावली का भविष्य में गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सके।
- भविष्य में जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर रोक लगाने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय शामिल किए गए। अब राष्ट्रपति के लिए आपातकाल की उद्घोषणा करने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से लिखित में सहमति लेना जरूरी कर दिया गया।
- आपातकाल की घोषणा को एक माह के भीतर विशेष बहुमत द्वारा संसद से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया।
- मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 359 का दायरा सीमित किया गया। इसका अर्थ यह था कि आपातकाल के दौरान भी नागरिकों के अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 20) तथा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21) आपातकाल के दौरान लागू रहेंगे अर्थात् इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकेगा।
- संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया।
- अनुच्छेद 257A का निरसन: यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को किसी भी राज्य में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए केंद्र के किसी भी सशस्त्र बल या अन्य बल को तैनात करने की अनुमति देता था। इस अनुच्छेद को हटा दिया गया।
- लोक सभा का कार्यकाल: अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करके लोक सभा का कार्यकाल 6 साल से घटाकर वापस 5 साल कर दिया गया।
- न्यायिक समीक्षा की बहाली: इस संशोधन ने न्यायपालिका की उस शक्ति को वापस बहाल कर दिया, जिसके माध्यम से वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों की न्यायिक समीक्षा कर सकती थी।
- अनुच्छेद 352 में संशोधन (आपातकाल की घोषणा से संबंधित):
राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के बारे में
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के प्रभाव
|
निष्कर्ष
आपातकाल से मिली सीख आज भी बहुत प्रासंगिक है। राष्ट्रीय हित या स्थिरता के नाम पर सत्ता के दुरुपयोग का खतरा हमेशा बना रहता है, जिससे असंतोष की अभिव्यक्ति को दबाया जा सकता है और संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए सतर्कता बनाए रखना जरूरी है, ताकि संवैधानिक सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रताएं बनी रहें।




