सुर्ख़ियों में क्यों?
हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने 'द स्टेट ऑफ़ सोशल जस्टिस: ए वर्क इन प्रोग्रेस' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।
अन्य संबंधित तथ्य
- यह रिपोर्ट दोहा में सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन (नवंबर 2025) से पहले जारी की गई है। यह शिखर सम्मेलन 1995 में डेनमार्क में हुए कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के 30 साल पूरे होने का प्रतीक है।
- इस शिखर सम्मेलन में सामाजिक विकास पर कोपेनहेगन घोषणा-पत्र और कोपेनहेगन प्रोग्राम ऑफ एक्शन को अपनाया गया था।
- इन दस्तावेज़ों में दस प्रमुख प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया गया था। इनमें गरीबी उन्मूलन, पूर्ण और उत्पादक रोज़गार प्राप्त करना तथा पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक एकीकरण और समानता को बढ़ावा देना शामिल है।
- 2025 की रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर सामाजिक न्याय की स्थिति का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। यह कई प्रमुख स्तंभों पर प्रगति और निरंतर बनी हुई चुनौतियों का परीक्षण करती है।
सामाजिक न्याय क्या है?
- परिभाषा: "यह सभी मनुष्यों को, चाहे उनकी नस्ल, जाति, पंथ या लिंग कुछ भी हो, स्वतंत्रता और सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और समान अवसर की स्थिति में अपने भौतिक कल्याण और आध्यात्मिक विकास दोनों को आगे बढ़ाने का अधिकार है"।
- यह स्थायी समावेशी विकास, शांति और स्थिरता के लिए विश्वास बनाने में मदद करता है, वैधता को बढ़ाता है और पूर्ण उत्पादक क्षमता का उपयोग करता है।

सामाजिक न्याय में मुख्य उपलब्धियाँ (रिपोर्ट के अनुसार)
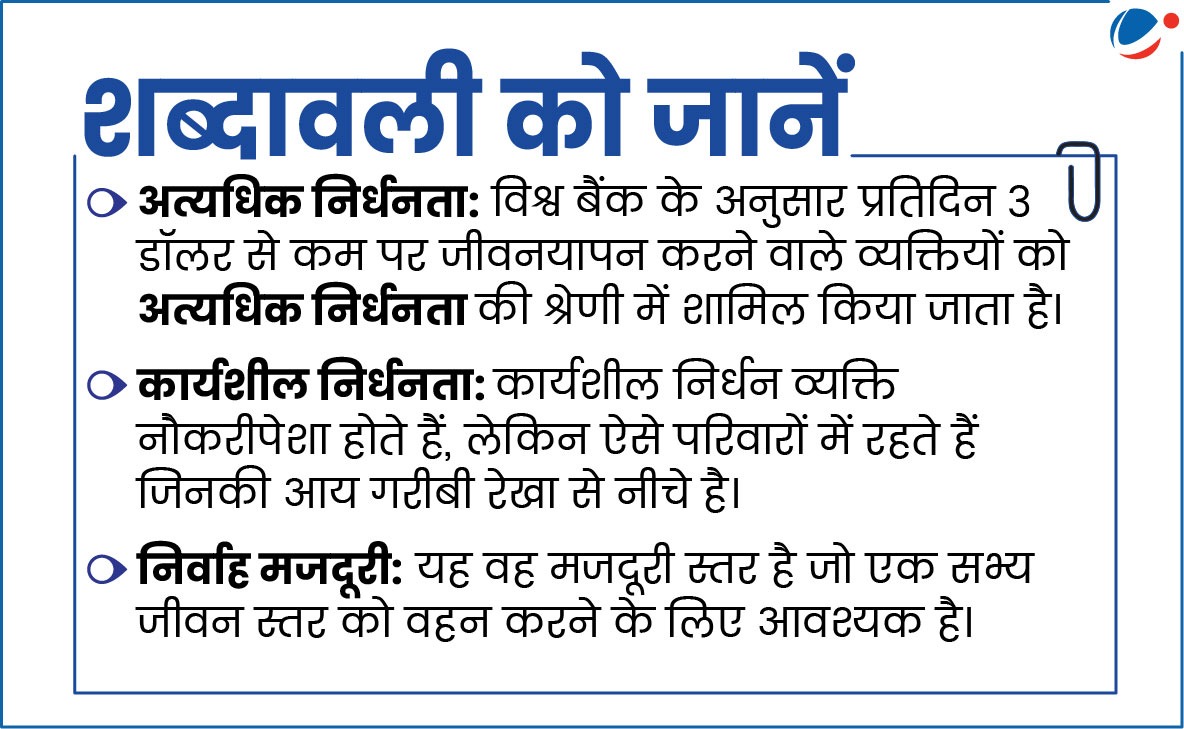
- चरम गरीबी में कमी: चरम गरीबी 1995 में 39% से घटकर 2025 में 10% हो गई है। वहीं, कामकाजी गरीबी 28% से गिरकर 7% हो गई है।
- अधिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज: इतिहास में पहली बार, दुनिया की आधी से अधिक आबादी कम-से-कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में आती है।
- श्रम बल भागीदारी में लैंगिक अंतराल में कमी: 2005 से 2025 तक यह अंतराल 26% से घटकर 24% रह गया है।
- असमानता में गिरावट: मध्य-आय वाले देशों में बढ़ती श्रमिक उत्पादकता के कारण, 2000 के दशक की शुरुआत से देशों के बीच असमानता कम हो रही है।
- बाल श्रम: यह 1995 के 20.6% से घटकर 2024 में 7.8% हो गया है।
हाल के समय में सामाजिक न्याय प्राप्त करने से संबंधित मुख्य चिंताएँ:
- मूल मानवाधिकारों से संबंधित चुनौतियाँ:
- वेतन असमानता: 2025 में, पुरुषों और महिलाओं के बीच आय का अनुपात 78% है। वर्तमान रुझानों के अनुसार, इस वेतन असमानता को दूर करने में 50-100 साल लग सकते है।
- बाल श्रम: 5-17 वर्ष की आयु के 138 मिलियन बच्चे बाल श्रमिक हैं। इनमें से लगभग 50% खतरनाक श्रम में लगे हुए हैं।
- जबरन श्रम: 2016 से 2021 के बीच जबरन मज़दूरी में लगे लोगों की संख्या 24.9 मिलियन से बढ़कर 27.6 मिलियन हो गई है।
- अवसरों की समानता से संबंधित चुनौतियाँ:
- असमानता: आबादी का शीर्ष 1% अभी भी 20% आय और 38% धन को नियंत्रित करता है।
- अनौपचारिक रोज़गार: कुल रोजगार में इसका हिस्सा लगभग 58% है।
- बुनियादी सेवाओं तक पहुंच: उदाहरण के लिए, 4 में से 1 व्यक्ति की स्वच्छ पानी तक पहुंच नहीं है।
- न्यायोचित बदलाव से संबंधित चुनौतियाँ:
- पर्यावरण संक्रमण: वैश्विक तापमान परिवर्तन को अधिकतम 2°C तक सीमित करने के लिए आवश्यक उपायों से लगभग 6 मिलियन नौकरियों का नुकसान हो सकता है। मुख्य रूप से यह नुकसान जीवाश्म ईंधन क्षेत्र से जुड़ी नौकरियों का होगा।
- डिजिटल बदलाव: नवीनतम ILO शोध से पता चलता है कि जनरेटिव AI की वजह से लगभग चार में से एक नौकरी रूपांतरित होने की संभावना है।
- जनसांख्यिकीय बदलाव: श्रम बाजारों में सुधार करना, उत्पादकता बढ़ाना और बेहतर रोज़गार तक पहुंच प्रदान करना (अधिकांश निम्न- और उच्च-मध्यम आय वाले देशों में) महत्वपूर्ण बना हुआ है। इसके साथ ही, उच्च और उच्च-मध्यम आय वाले देशों में बढ़ते कार्यबल की ज़रूरतों का समाधान करना भी महत्वपूर्ण है।
सामाजिक न्याय के लिए मुख्य पहलें
- वैश्विक:
- सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन: इसे ILO द्वारा 2023 में लॉन्च किया गया था। यह पहल सामाजिक न्याय के लिए सरकारों, श्रमिकों और नियोक्ता संगठनों और अन्य भागीदारों को एक साथ लाती है।
- सभ्य कार्य एजेंडा: ILO का सभ्य कार्य एजेंडा सभी लोगों के लिए उचित आय, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के साथ उत्पादक कार्य प्राप्त करने के अवसरों को बढ़ावा देता है।
- न्यायोचित वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर ILO घोषणा-पत्र: इसे 2008 में अपनाया गया था। यह घोषणा-पत्र सभ्य कार्य एजेंडा को ILO की नीतियों के केंद्र में लाता है।
- मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948): इसके तहत उन मौलिक मानवाधिकारों की घोषणा की गई है, जिन पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार हैं।
- अन्य पहलें: आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (1966), भुखमरी और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन (G20), सतत विकास लक्ष्य (SDGs), आदि।
- भारत:
- संवैधानिक उपाय: उदाहरण के लिए- संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है; मूल अधिकार (उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 23), राज्य की नीति के निदेशक तत्व (अनुच्छेद 38), आदि।
- विधायी उपाय: उदाहरण के लिए- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016, SC और ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, आदि।
- संस्थागत उपाय: उदाहरण के लिए- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC), राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), आदि।
- कल्याणकारी उपाय: उदाहरण के लिए- PM आवास योजना, आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY), आदि।
आगे की राह
- न्यायपूर्ण वितरण
- सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को प्रभावी ढंग से मान्यता दी जाए। न्यूनतम वेतन नीतियों को अपडेट किया जाए और ILO के सिद्धांतों के अनुरूप वेतन-निर्धारण प्रक्रिया के माध्यम से जीवन निर्वाह योग्य वेतन तय करने की प्रक्रिया लागू की जाए।
- भेदभाव-रोधी नीतियों की प्रभावशीलता बढ़ाई जाए और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की संधारणीयता, कवरेज और पर्याप्तता को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- अवसरों की समानता
- प्रशिक्षण और श्रम मध्यस्थता सहित सक्रिय श्रम बाजार नीतियों (Active labour market policies: ALMPs) को मजबूत किया जाना चाहिए।
- टिकाऊ उद्यम उपायों का समर्थन करना तथा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए औपचारिकता के तरीकों की पेशकश करना।
- सतत उद्यम को बढ़ावा दिया जाए और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए औपचारिकता के मार्ग पेश किए जाने चाहिए।
- सरकार को रोजगार सब्सिडी, जैसे कि वेतन सब्सिडी और भर्ती प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।
- सुव्यवस्थित लोक रोज़गार कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए। उदाहरण के लिए, भारत का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)।
- न्यायोचित बदलाव
- क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए। उदाहरण के लिए- उन भौगोलिक क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करना जहाँ अन्य ऊर्जा उत्पादन कम हो गया है।
- बुजुर्ग श्रमिकों को बनाए रखने और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए आंशिक सेवानिवृत्ति और आयु-आधारित भेदभाव-विरोधी कानून आवश्यक हैं।
- परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल के लिए सवैतनिक अवकाश के प्रावधानों का विस्तार करना चाहिए।
निष्कर्ष
गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और लैंगिक समानता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, सामाजिक न्याय अब भी अधूरी प्रक्रिया है। प्रगति को बनाए रखने के लिए, देशों को संरचनात्मक असमानताओं को कम करने, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आर्थिक संवृद्धि प्रत्येक व्यक्ति के लिए गरिमा और अवसर लेकर आए।



