सुर्ख़ियों में क्यों?
हाल ही में, ओडिशा सरकार ने एक सहयोगात्मक पहल 'सहयोग/ SAHAYOG' शुरू की है। इसका उद्देश्य शहरी गरीबों की सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाना है।
सहयोग/ SAHAYOG पहल के बारे में
- लक्ष्य: आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर में विविध सरकारी योजनाओं के माध्यम से सुधार लाना।
- प्रयोजन: शहरी गरीब समुदायों में पात्र लाभार्थियों की पहचान करना और उन्हें जन जागरूकता अभियान, डोर-स्टेप सेवा डिलीवरी आदि के माध्यम से चिन्हित सरकारी योजनाओं से जोड़ना।
- इसके पहले चरण में, 13 प्रमुख योजनाओं से वंचित लाभार्थियों की पहचान और पंजीकरण के लिए 8 जिलों के 44 शहरी क्षेत्रों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा।
भारत में शहरीकरण और शहरी गरीबी की वर्तमान स्थिति
विश्व बैंक की नवीनतम 'पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ' रिपोर्ट के अनुसार-
|
शहरी और ग्रामीण गरीबी के बीच अंतर
- मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच: शहरी गरीब व्यक्ति आवास की कमी और स्वच्छता जैसी मूलभूत सेवाओं की कमी का सामना करते हैं। वहीं ग्रामीण गरीब भू-स्वामित्व की सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित हैं।
- जीवन स्तर और परिस्थितियां: शहरी गरीबों को अत्यधिक भीड़-भाड़ और स्वच्छता की कमी जैसी समस्याओं की वजह से बीमारी एवं अपराध का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीण गरीबों को पक्के आवास की कमी, जातिगत भेदभाव आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- गरीबी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव: शहरी क्षेत्रों में सापेक्ष वंचन और सामाजिक अपवर्जन की भावना प्रबल होती है। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में गरीबी अधिक दिखाई देती है। उदाहरण के लिए- मुंबई में धारावी जैसे झुग्गी-बस्तियों का गगनचुंबी इमारतों के आस-पास होना।
- शहरी गरीबों को अक्सर अलगाव व अकेलेपन व संबद्ध चिंता का भी सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीण गरीबों को गरीबी का सांस्कृतिक रूप से संस्थागत प्रभाव झेलना पड़ता है, जिसका जाति या लिंग से अधिक गहरा संबंध होता है।
- आर्थिक संरचना: ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, जबकि शहरी अर्थव्यवस्था अधिक विविध और जटिल होती है। इस प्रकार, शहरी क्षेत्र में आर्थिक अवसर अधिक होते हैं। हालांकि, इसी वजह से शहरी गरीबी अधिक बहुआयामी व जटिल होती है।
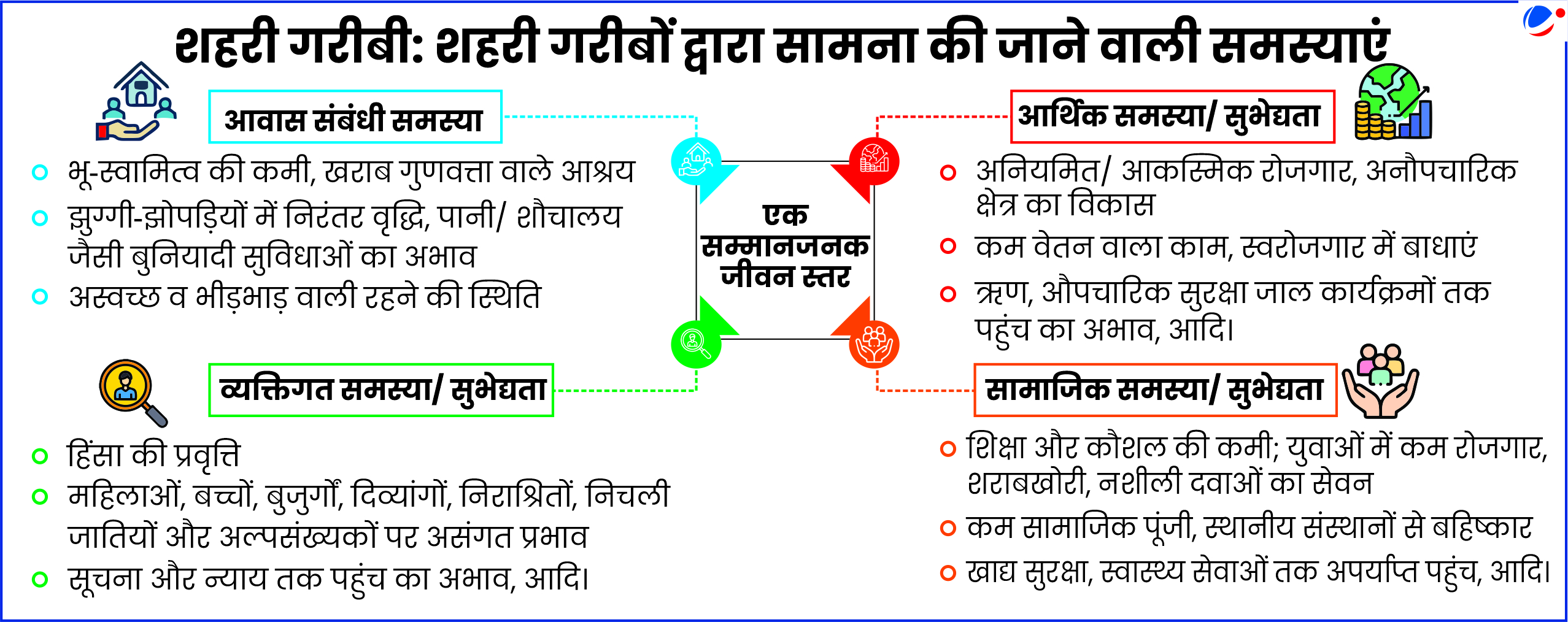
शहरी गरीबी के बने रहने के लिए जिम्मेदार कारक
- योजनाबद्ध शहरी विकास का अभाव: अव्यवस्थित शहरीकरण, गांव से शहर की ओर पलायन तथा शहरों की बढ़ती आबादी एवं नीति निर्माण में शहरी गरीबों को अनदेखा करना। उदाहरण के लिए- किफायती आवास योजनाओं की कमी।
- शहरीकरण में क्षेत्रीय असमानता: टियर-II और टियर-III शहरों के अपर्याप्त विकास के कारण दिल्ली, मुंबई जैसे महानगर अत्यधिक जनसंख्या के बोझ से जूझ रहे हैं।
- सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच का अभाव: शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कई गरीब प्रवासियों के पास पहचान-पत्र या निवास प्रमाण-पत्र नहीं होता, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते और गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रह जाते हैं।
- गरीबी का दुष्चक्र: गरीबी के कारण लोगों को शिक्षा, नौकरी आदि के सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता के अवसर नहीं मिलते, जिससे पीढ़ी-दर-पीढ़ी गरीबी बनी रहती है।
शहरी गरीबी को कम करने के लिए सरकारी पहलें
- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड: आधार/ AADHAAR आधारित यह योजना देश में कहीं से भी राशन लेने की सुविधा देती है। इससे गरीब और आंतरिक प्रवासी मजदूरों को भोजन की सुरक्षा मिलती है।
- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (SBM-U 2.0): यह एक स्वच्छता योजना है, जिसके तहत शहरी परिवारों के लिए व्यक्तिगत शौचालयों (IHHL) का निर्माण किया जाता है।
- प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U): इसके तहत झुग्गी-बस्तियों में रहने वालों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/ निम्न आय समूह (LIG) और मध्यम आय समूह (MIG) वर्गों को किफायती दर पर आवास उपलब्ध कराया जा रहा है।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM): यह योजना शहरी गरीबों को लाभकारी स्वरोजगार और कौशल प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करती है।
- पी.एम. स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि): इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती दर पर ऋण प्रदान किया जाता है।
- अन्य: अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 (AMRUT 2.0), स्मार्ट सिटीज़ मिशन, आदि।
आगे की राह
- समावेशी शहरीकरण: समावेशी शहरी विकास नियोजन के लिए लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ-साथ निर्णय प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने की भी आवश्यकता है। साथ ही, मिश्रित उपयोग विकास और समावेशी ज़ोनिंग नीतियों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि झुग्गी-बस्तियां न बनाई जा सकें तथा सभी को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।
- उदाहरण के लिए- झुग्गी-बस्ती पुनर्वास और पुनर्विकास में स्वयं सहायता समूह अहम भूमिका निभा सकते हैं। केरल में 'कुदुम्बश्री' महिला नेटवर्क का NULM में सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है।
- टियर-II और टियर-III शहरों का विकास: छोटे शहरों एवं कस्बों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करके संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना चाहिए। इससे महानगरों पर जनसंख्या का दबाव कम करने में मदद मिलेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना विकास और रोजगार के अवसरों में सुधार करके ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर रोक लगाई जा सकती है।
- सतत शहरीकरण: शहरी नियोजन और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में संधारणीयता को प्राथमिकता देने में शहरी स्थानीय निकायों की अहम भूमिका होनी चाहिए। उदाहरण के लिए- स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंदौर का स्वच्छता अभियान।
- शहरी गरीबों का सशक्तीकरण: ऋण, व्यवसाय विकास सेवाओं और बाजार लिंकेज तक बेहतर पहुंच के माध्यम से कौशल विकास, श्रम-गहन उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के विकास को बढ़ावा देना चाहिए।
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का लक्षित वितरण: योजनाओं की पोर्टेबिलिटी को बढ़ावा देने, समावेशन-अपवर्जन त्रुटियों को सुधारने और योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी में सुधार करने की आवश्यकता है।
निष्कर्ष
2050 तक भारत के शहरों द्वारा GDP में 75% से अधिक योगदान देने और इनसे लगभग 60% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होने की संभावना है। इसलिए, शहरी गरीबी की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान किया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि शहरी क्षेत्रों का संधारणीय विकास सुनिश्चित किया जा सके। यह प्रयास 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक होगा और भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मजबूत कदम होगा।



