परिचय
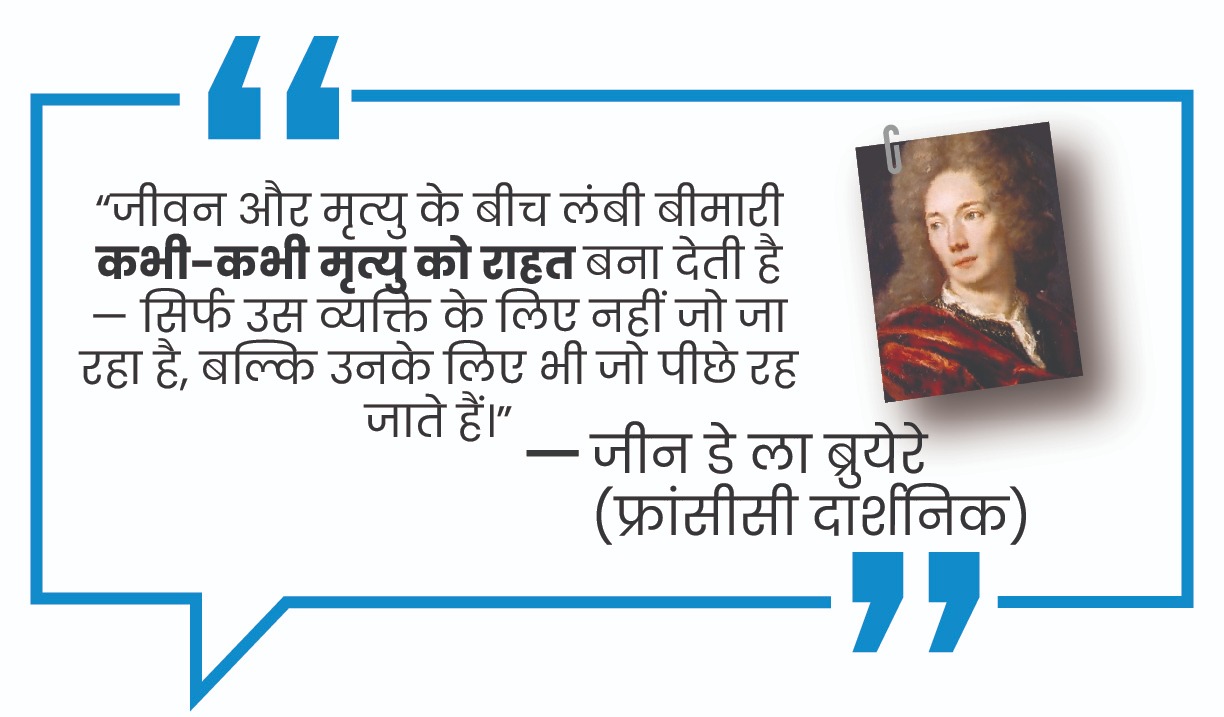
हाल ही में, जैन समुदाय की एक 3 वर्षीय बच्ची की संथारा (मृत्यु तक उपवास) की प्रथा के जरिए मृत्यु हो गई। वह बच्ची टर्मिनल ब्रेन ट्यूमर की समस्या से जूझ रही थी। इस घटना को लेकर चिंता व्यक्त की गई है कि क्या वह बच्ची अपने विवेक से निर्णय (Informed decision) लेने में सक्षम थी।
इसके अतिरिक्त, फ्रांस ने एक विधेयक पारित किया है, जो असहनीय और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित वयस्कों को चिकित्सकीय सहायता से मृत्यु (Assisted dying) चुनने की अनुमति देता है। उपर्युक्त घटनाक्रम गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार के सिद्धांतों को उजागर करते हैं।
गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार के बारे में
- अर्थ: गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार का तात्पर्य यह है कि लाइलाज या गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों के बारे में स्वयं निर्णय ले सके। इस अधिकार के तहत व्यक्ति यह तय कर सकता है कि वह कितनी पीड़ा और दर्द सहन करना चाहता है, और यदि वह चाहे तो उपचार या जीवन रक्षक उपायों को जारी रखने या बंद करने का विकल्प भी चुन सकता है।
- इच्छामृत्यु या यूथेनेशिया (अर्थात, "सम्मानजनक मृत्यु") गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान करने का एक अनिवार्य साधन है। यह दो प्रकार की होती है:
- सक्रिय यूथेनेशिया (Active): इसके तहत सक्रिय साधनों का उपयोग करके रोगी की इच्छामृत्यु में सहायता की जाती है, उदाहरण के लिए- जानलेवा दवा देना। सक्रिय यूथेनेशिया भारत में गैर-कानूनी है।
- निष्क्रिय यूथेनेशिया (Passive): रोगी को जीवन रक्षक प्रणाली (जैसे- वेंटिलेटर, फ़ीडिंग ट्यूब) से हटाकर स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त करने में सहायता करना।
- इच्छामृत्यु या यूथेनेशिया (अर्थात, "सम्मानजनक मृत्यु") गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान करने का एक अनिवार्य साधन है। यह दो प्रकार की होती है:
- भारत में स्थिति:
- 2011 में, अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी।
- कॉमन कॉज बनाम भारत सरकार (2018) वाद में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार भी शामिल है। इस प्रकार कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु की वैधता को बरकरार रखा और भारत में लिविंग विल के लिए प्रक्रिया निर्धारित की।
प्रमुख हितधारक और संबंधित नैतिक मुद्दे
गंभीर रोग से ग्रसित मरीज और उनका परिवार |
|
स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (डॉक्टर, नर्स, प्रशामक देखभाल पेशेवर) |
|
विधि और नीति निर्माता |
|
समाज |
|
गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार में शामिल नैतिक दुविधाएं
- जीवन की गुणवत्ता बनाम जीवन की पवित्रता: यदि असहनीय पीड़ा या गरिमा की हानि जीवन पर हावी हो जाए, तो क्या केवल जीवित रहना अर्थपूर्ण है?
- संवैधानिक नैतिकता बनाम स्वायत्तता का सम्मान: क्या किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा कानूनी और नैतिक सीमाओं से ऊपर होनी चाहिए?
- उपशामक देखभाल (Palliative Care) बनाम न्याय: क्या हमें केवल जीवन रक्षक प्रणाली पर निर्भर रहना चाहिए या जब देखभाल प्रणाली विफल हो जाती है, तब गरिमापूर्ण इच्छामृत्यु की अनुमति दी जानी चाहिए?
- गैर-हानिकारक सिद्धांत बनाम दोहरे प्रभाव का सिद्धांत: क्या डॉक्टरों द्वारा दर्द से राहत प्रदान की जानी चाहिए, भले ही इससे जीवन काल छोटा हो जाए?
गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार के पक्ष में तर्क
- जीवन की गुणवत्ता: जीवन की गुणवत्ता केवल एक साधारण जीवन जीने से कहीं बढ़कर है। इसमें मनोवैज्ञानिक कल्याण, संज्ञानात्मक क्षमता और सार्थक संबंध बनाने की क्षमता शामिल है।
- असहनीय दर्द या कार्य क्षमता के नष्ट होने के बाद भी जीवन को बनाए रखना उचित नहीं हो सकता है।
- स्वायत्तता का सम्मान: स्वायत्तता मानव नैतिक मूल्यों की आधारशिला है। सक्षम व्यक्तियों को मृत्यु का चुनाव करने का अधिकार होना चाहिए।
- भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु का विकल्प चुना और सुकरात ने निर्वासन के बजाय मृत्यु को चुना।
- डबल इफेक्ट सिद्धांत: यदि डॉक्टर का उद्देश्य दर्द से राहत देना है, तो इसके लिए ऐसी दवा देना नैतिक रूप से स्वीकार्य है, जो रोगी को दर्द से राहत पहुंचाती हो, भले ही उस प्रक्रिया में रोगी का जीवन काल छोटा क्यों ना हो जाए।
- न्याय: जब उपचारात्मक दवा विफल हो जाती है और पैलिएटिव देखभाल पर्याप्त रूप से पीड़ा को कम नहीं कर पाती है, तो उपचार जारी रखने से व्यक्ति को अधिक पीड़ा हो सकती है।
- न्याय की मांग है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के अंत में सहानुभूति पूर्ण विकल्प प्रदान किए जाए। लंबे समय तक भावनात्मक और वित्तीय दबाव रोगी और परिवार दोनों के लिए हानिकारक सिद्ध होती है।
गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार के विरुद्ध तर्क
- जीवन की पवित्रता: यह मानव जीवन को एक आंतरिक कल्याण मानता है, जो अमूल्य है। इसलिए एक निर्दोष व्यक्ति को मारना हमेशा अक्षम्य होता अपराध होता है।
- उदाहरण के लिए, बौद्ध धर्म अहिंसा और नुकसान न पहुंचाने की अवधारणा के माध्यम से जीवन की पवित्रता का प्रचार करता है।
- संवैधानिक नैतिकता: धर्म का एक आवश्यक हिस्सा होने के बावजूद धार्मिक प्रथाएं जीवन के अधिकार के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं।
- उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 25(1) के तहत धर्म की स्वतंत्रता पर लोक व्यवस्था, सदाचार (नैतिकता) और स्वास्थ्य के हित में उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं।
- पैलिएटिव देखभाल: इच्छामृत्यु के बिना भी अच्छी देखभाल करना रोगी की पीड़ा को कम कर सकती है। साथ ही, चिकित्सा विज्ञान हर रोज एक नई प्रगति कर रहा है। वर्तमान में जो बीमारी लाइलाज है, वह कल इलाज योग्य हो सकती है।
- हानि न पहुंचाने का सिद्धांत: हानि न पहुंचाने का सिद्धांत (कोई नुकसान न पहुंचाना) रोगी को नुकसान न पहुंचाने के महत्व को रेखांकित करता है।
- यह सिद्धांत चिकित्सा पेशेवरों की हिप्पोक्रेटिक शपथ के भी अनुरूप है, जिसमें "कोई हानि नहीं पहुंचाने" का संकल्प होता है।
- कांट के दर्शन के विपरीत: इमैनुएल कांट के अनुसार, जीवन की रक्षा करना एक सार्वभौमिक नैतिक कर्तव्य है। जीवन का एक आंतरिक मूल्य होता है। ऐसे में इसे समाप्त करना नैतिक दायित्व को कमजोर करता है।
- दुरुपयोग की संभावना: नाबालिग (युवा और संवेदनशील व्यक्ति) और गंभीर रूप से बीमार रोगियों (तार्किक सोच की कमी) के मामले में, स्वायत्तता के सिद्धांत का दुरुपयोग किया जा सकता है।
- इसके अलावा, कुछ चिकित्सक अपनी चिकित्सा संबंधी गलतियों को छिपाने के लिए रोगियों पर मृत्यु का विकल्प चुनने का दबाव डाल सकते हैं।
गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह
- विस्तृत संवाद स्थापित करना: रोगी के जीवन, स्वास्थ्य और बीमारी के प्रति दृष्टिकोण को समझने के लिए नियमित संवाद आवश्यक है। इससे उनकी इच्छाओं और चिंताओं को समझा जा सकता है।
- प्रभावी विनियमन: इच्छामृत्यु की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से विनियमित किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह केवल अस्पताल सेटिंग्स में कम-से-कम 2 चिकित्सकों के प्रमाणन के बाद ही किया जा सके।
- यह प्रक्रिया पूरी तरह डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और सभी संभावित चिकित्सकीय विकल्पों के विश्लेषण के बाद ही इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
- दुरुपयोग को रोकना: इच्छामृत्यु की अनुमति देने से पहले, एक पूर्ण मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, परामर्श, प्रतीक्षा अवधि होनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रोगी किसी दबाव या अस्थायी मानसिक स्थिति में निर्णय नहीं ले रहा है।
- देखभाल एक नैतिक दृष्टिकोण: विशेष रूप से नाबालिगों और मानसिक रूप से कमजोर रोगियों के मामलों में सहानुभूति और करुणा पर आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। रोगी के अनुभवों को समझने और उनके भावनात्मक पक्ष को मान्यता देने पर बल देना चाहिए।
निष्कर्ष
चिकित्सकीय प्रगति लोगों के जीवन को लंबा बना सकती है, लेकिन यह पीड़ा को हमेशा समाप्त नहीं कर सकती है। जब दर्द असहनीय हो जाता है, तो गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार विचारणीय हो जाता है। हालांकि, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए मजबूत नैतिक दिशा-निर्देशों और सख्त नियमों का पालन करना चाहिए।
जैसा कि भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने कहा था:
"मेरा मानना है कि जो लोग एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं और अत्यधिक पीड़ा झेल रहे हैं, उन्हें अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए, और जो लोग उनकी सहायता करते हैं उन्हें सजा से मुक्त होना चाहिए।"
यह हमारे समय के सबसे गहन नैतिक प्रश्नों में से एक अर्थात् गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार के प्रति एक करुणामय, मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है।
अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिएआपको हाल ही में एक दूरस्थ जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। आपको एक ऐसी महिला का मामला मिलता है जिसे हाल ही में सर्वाइकल ट्यूमर का पता चला था। उस महिला ने अपना अधिकांश जीवन अपने शराबी पति द्वारा की गई हिंसा और उत्पीड़न के बीच बिताया है। अब उसकी बीमारी अंतिम अवस्था में पहुँच चुकी है, जिससे वह असहनीय दर्द और बेबसी झेल रही है। उसका परिवार भी उसकी भलाई के प्रति बहुत विचारशील नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, उसने चिकित्सकीय सहायता से मृत्यु के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। हालांकि, क्षेत्र के लोग अत्यधिक धार्मिक हैं और यदि ऐसे कृत्य की बात फैल गई, तो अशांति उत्पन्न हो सकती है। इस स्थिति ने आपको एक कठिन दुविधा में डाल दिया है जहाँ एक ओर एक असहाय महिला की पीड़ा है, तो दूसरी ओर नागरिक अशांति का मुद्दा है। उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:
|



