सुर्ख़ियों में क्यों?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन योजना को मंजूरी दी। इसके लिए कुल 1,702 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य पशुधन और डेयरी क्षेत्रकों से किसानों की आय बढ़ाना है।
अन्य संबंधित तथ्य
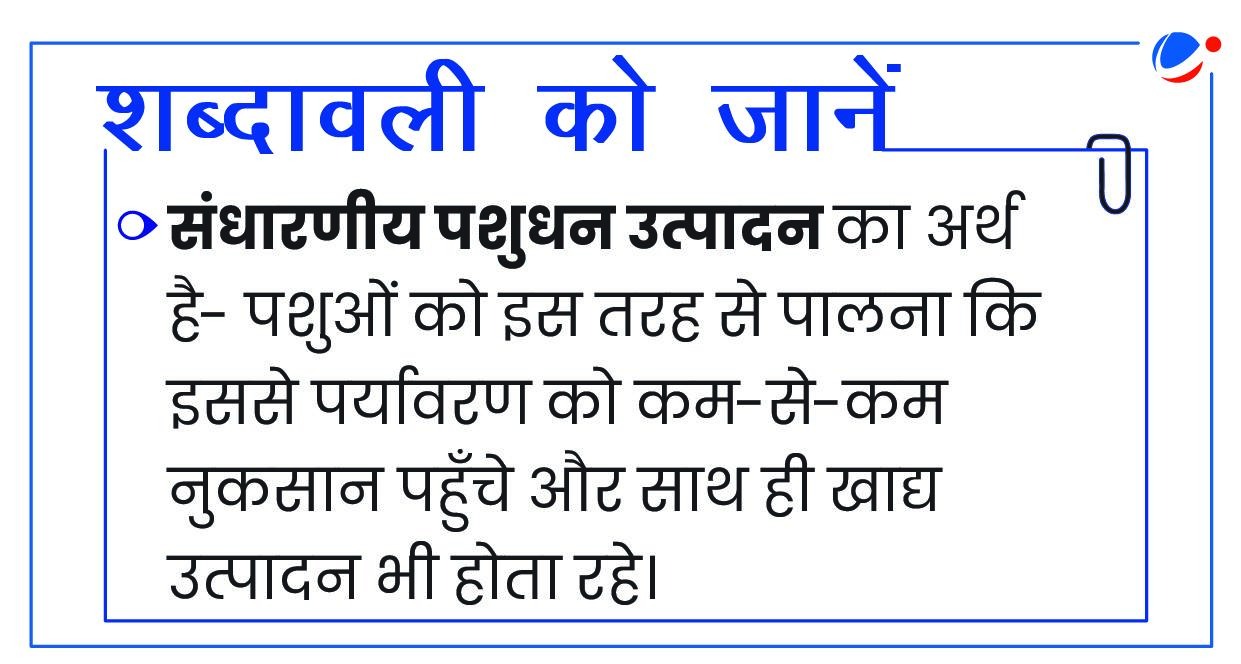
- योजना में निम्नलिखित शामिल हैं:
- पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु-चिकित्सा से संबंधित शिक्षा;
- डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास;
- पशु आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन, उत्पादन और सुधार;
- पशु पोषण और जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का उत्पादन व विकास।
भारत में पशुधन क्षेत्रक की स्थिति
- विश्व में पशुधन की सबसे अधिक संख्या भारत में है।
- भारत भैंस के मांस का सबसे बड़ा उत्पादक और बकरी के मांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
भारत में पशुधन क्षेत्रक का महत्त्व
- सकल घरेलू उत्पाद में योगदान: 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर कृषि और संबद्ध क्षेत्रक के GVA में पशुधन क्षेत्रक का योगदान 30.19% और कुल GVA में इसका योगदान 5.73% था।
- रोजगार सृजन: पशुपालन भारत में 70% से अधिक ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। इनमें बड़ा अनुपात लघु और सीमांत किसानों एवं भूमिहीन मजदूर परिवारों का है।
- कृषि-गतिविधियों के साथ अंतर्संबंध: पशुधन क्षेत्रक खाद जैसे ऑर्गेनिक इनपुट के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, कृषि अपशिष्ट का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है।
- खाद्य और पोषण सुरक्षा: दूध, मांस और अंडे जैसे उत्पादों में प्रचुर मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जो कुपोषण से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर बच्चों और महिलाओं में।
- भारत दूध उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है। विश्व में दूध उत्पादन में भारत 23% का योगदान देता है।
भारत में पशुधन क्षेत्रक से जुड़ी समस्याएं
- स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा संबंधी समस्याएं:
- पशु रोगों के कारण उच्च आर्थिक नुकसान: जैसे- रक्तस्रावी सैप्टिसीमिया, खुरपका और मुंहपका रोग, ब्रुसेलोसिस रोग, आदि।
- इसके अलावा, जानवरों से मनुष्यों में जूनोटिक रोग भी फैल सकते हैं, जैसा कि हाल ही में कोविड-19, इबोला और एवियन इन्फ्लूएंजा जैसी महामारियों के प्रकोप से स्पष्ट होता है।
- अवसंरचना और मानव संसाधन की कमी: भारत में मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 60 से भी कम है। इस वजह से भारत में आवश्यक संख्या में पशु-चिकित्सक या वेटनरी डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं।
- एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की चुनौती: पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। पोल्ट्री क्षेत्र में पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं का सबसे अधिक उपयोग होता है।
- पशु रोगों के कारण उच्च आर्थिक नुकसान: जैसे- रक्तस्रावी सैप्टिसीमिया, खुरपका और मुंहपका रोग, ब्रुसेलोसिस रोग, आदि।
- आर्थिक चिंताएं:
- कम उत्पादकता: इसकी वजहें हैं- पर्याप्त पोषण नहीं मिलना, पशुधन प्रबंधन की ख़राब व्यवस्था और स्थानीय पशु नस्लों की कम आनुवंशिक क्षमता।
- साल 2019-20 के दौरान भारत में मवेशियों की औसत वार्षिक उत्पादकता 1,777 किलोग्राम प्रति पशु रही, जबकि वैश्विक औसत 2,699 किलोग्राम प्रति पशु था।
- असंगठित क्षेत्र के रूप में मौजूद: कुल मांस उत्पादन का लगभग 50 फीसदी हिस्सा अपंजीकृत और अस्थायी बूचड़खानों से आता है।
- मार्केटिंग और लेन-देन की उच्च लागत: यह पशुधन उत्पादों की बिक्री मूल्य का लगभग 15-20% है।
- कम बीमा कवर प्राप्त होना: केवल 15.47% पशुधन बीमा कवर के तहत आते हैं।
- चारे की कमी: भारत में केवल 5% कृषि योग्य भूमि पर चारा उत्पादन होता है, जबकि वैश्विक पशुधन आबादी का 11% हिस्सा भारत में है। पशुओं की विशाल संख्या की वजह से भूमि, जल और अन्य संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है।
- कम उत्पादकता: इसकी वजहें हैं- पर्याप्त पोषण नहीं मिलना, पशुधन प्रबंधन की ख़राब व्यवस्था और स्थानीय पशु नस्लों की कम आनुवंशिक क्षमता।
- विस्तार सेवाओं पर अधिक ध्यान नहीं देना: पशुधन क्षेत्रक के लिए अलग से विस्तार कार्यक्रम नहीं है। पशुधन से जुड़ी अधिकांश सेवाएं पशु स्वास्थ्य से संबंधित हैं और ये "पशुधन विस्तार सेवाओं' से संबंधित नहीं हैं।
- ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन: भारत में पशुधन से होने वाला एंटरिक (जुगाली करने वाले पशुओं से) मीथेन उत्सर्जन, वैश्विक एंटरिक मीथेन उत्सर्जन में 15.1% का योगदान देता है।
भारत के पशुधन क्षेत्रक के लिए प्रमुख पहलें
|
आगे की राह
- राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली (NADRS) को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसमें पशु रोग प्रकोप की रियल टाइम रिपोर्टिंग के लिए अवसंरचनाओं का विकास और डिजिटलीकरण शामिल हैं।
- दूरदराज के क्षेत्रों के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएं शुरू की जानी चाहिए। इससे किसानों के घर तक पशु प्राथमिक चिकित्सा, कृत्रिम पशु गर्भाधान, डीवॉर्मिंग और टीकाकरण जैसी सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी।
- केंद्र सरकार के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग तथा राज्य पशुपालन और डेयरी विभागों में कर्मचारियों की संख्या और प्रशिक्षण आवश्यकताओं की समीक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य समूह की स्थापना की जानी चाहिए।
- फसलों की खेती, पशुपालन और अन्य कृषि गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए पशुधन आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) को बढ़ावा देना चाहिए। इससे संसाधनों का समुचित उपयोग किया जा सकेगा, उत्पादकता बढ़ाई जा सकेगी और संधारणीयता सुनिश्चित की जा सकेगी।
- बाजारों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना, दक्ष मूल्य श्रृंखला स्थापित करना तथा मार्केटिंग और सूचना प्रसार के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को बढ़ावा देना चाहिए।
- पशुधन क्षेत्रक में बीमा कवरेज बढ़ाना चाहिए ताकि पशुधन रखने वालों के ऊपर से जोखिम को बीमा कंपनियों पर स्थानांतरित किया जा सके।
- भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग-अलग नीतियां तैयार करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए- वर्षा सिंचित क्षेत्रों में नीति का मुख्य जोर पशुपालन या पशुधन आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली पर होना चाहिए।



