सुर्ख़ियों में क्यों?
हाल ही में, केंद्र सरकार में सचिव और संयुक्त सचिव के 45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिये भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा जारी विज्ञापन को वापस ले लिया गया।
अन्य संबंधित तथ्य
- लेटरल एंट्री के लिए जारी किए गए विज्ञापन को आलोचनाओं के कारण वापस ले लिया गया है। इस आलोचना का कारण यह है कि ऐसी भर्ती में अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) के उम्मीदवारों के लिए कोई आरक्षण नहीं होता है।
- नवंबर, 2018 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा UPSC को लिखे गए पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि-
- इन पदों को भरने की वर्तमान व्यवस्था को प्रतिनियुक्ति के रूप में माना जा सकता है, जहां SCs/ STs/ OBCs के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करना अनिवार्य नहीं है।
- हालांकि, यदि यथोचित योग्य SCs/ STs/ OBCs उम्मीदवार पात्र हैं, तो उन पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही, समग्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए समान स्थिति वाले मामलों में ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
लेटरल एंट्री में आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है?
|
लेटरल एंट्री के बारे में
- इसके माध्यम से सरकारी मंत्रालयों/ विभागों में मध्य और वरिष्ठ स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए पारंपरिक सरकारी सेवा संवर्गों के बाहर से व्यक्तियों की भर्ती की जाती है।
- यह उस पारंपरिक भर्ती प्रक्रिया से अलग है, जिसमें UPSC द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर पदों को भरा जाता है।
- यह सलाहकारी भूमिकाओं के लिए निजी क्षेत्रक के पेशेवरों की नियुक्ति करने से अलग है।
- उदाहरण के लिए- भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति, जो आमतौर पर एक प्रमुख अर्थशास्त्री होता है।
- यह 3 से 5 साल तक की अवधि के लिए की गई संविदात्मक भर्ती है, जिसमें प्रदर्शन के आधार पर कार्यकाल का विस्तार किया जा सकता है।
- ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में डायरेक्ट एंट्री (परीक्षा के माध्यम से) और लेटरल एंट्री, दोनों तरीकों को अपनाया गया है।
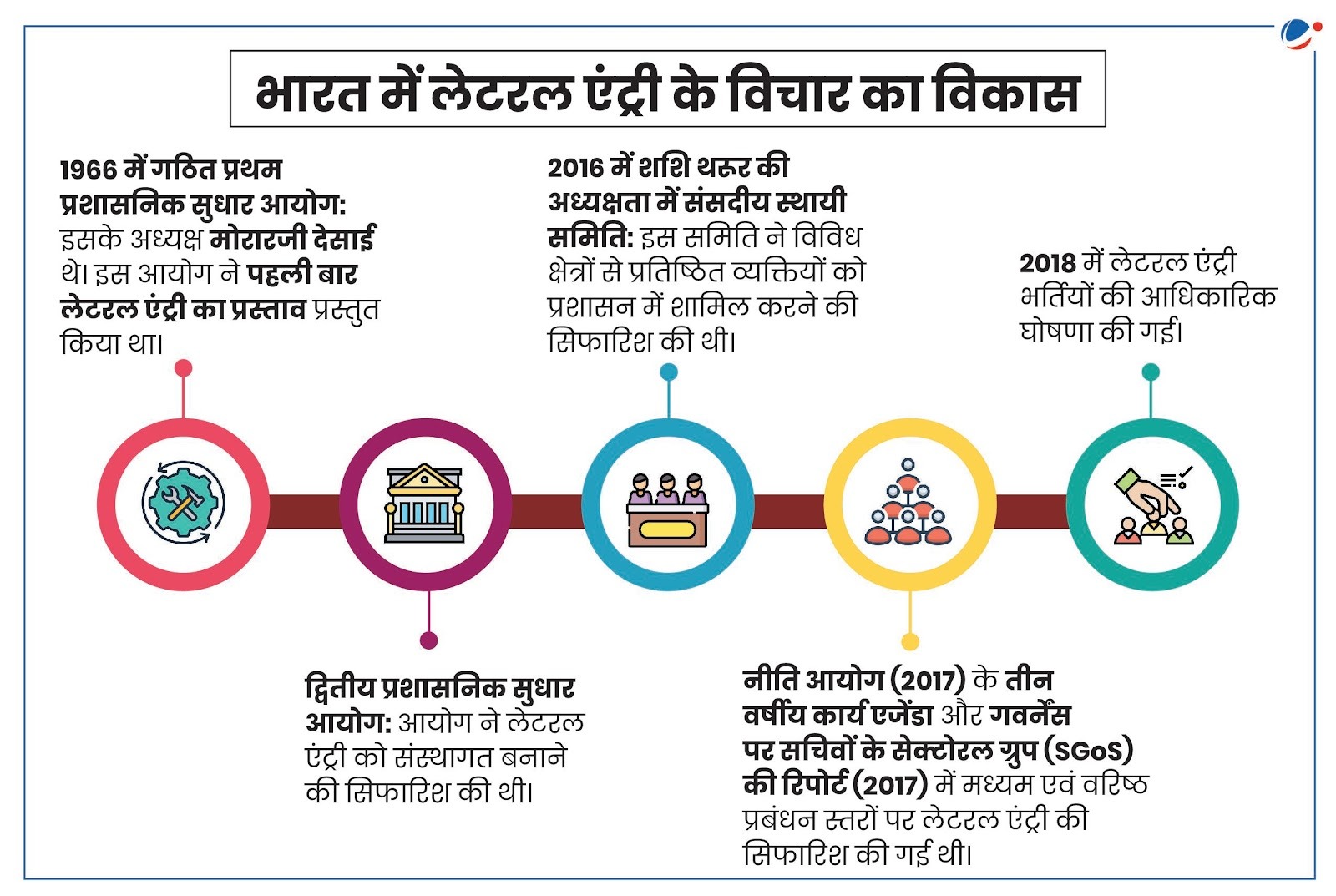
लेटरल एंट्री प्रणाली के लाभ
- अधिकारियों की कमी को दूर करना: DoPT की 2023-24 की अनुदान मांगों पर जारी रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के स्तर पर केवल 442 IAS अधिकारी काम कर रहे हैं, जबकि इनकी आवश्यक संख्या 1,469 है।
- बसवान समिति (2016) ने भी अधिकारियों की कमी को देखते हुए लेटरल एंट्री का समर्थन किया था।
- कार्यकुशलता और प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि: नीति आयोग के अनुसार, लेटरल एंट्री "स्थापित करियर आधारित नौकरशाही में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है।"
- विशिष्ट विषयों के विशेषज्ञों को शामिल करना: अर्थशास्त्र, वित्त, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टोकरेंसी जैसी तकनीकों में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को काम पर रखने से सार्वजनिक नीतियों में एक नया दृष्टिकोण आ सकता है।
- विभागीय आवश्यकताओं को पूरा करना: कुछ मंत्रालयों/ विभागों को नागर विमानन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर निजी क्षेत्रक के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है।
लेटरल एंट्री से जुड़े मुद्दे
- अल्पकालिक फोकस: 3 से 5 साल के लिए नियुक्तियां अल्पकालिक नीतिगत लक्ष्यों को जन्म दे सकती हैं, जिनमें दीर्घकालिक विज़न का अभाव होता है।
- संवैधानिक प्रावधानों के साथ टकराव: आरक्षण की नीति के दायरे से बाहर होने वाली भर्ती सामाजिक न्याय और समानता के उद्देश्य को प्रभावित करती है।
- हितों का टकराव: निजी क्षेत्रक के व्यक्ति लाभ के लिए सरकारी निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। इससे "रिवोल्विंग डोर" गवर्नेंस के जोखिम को बढ़ावा मिल सकता है।
- रिवोल्विंग डोर गवर्नेंस का आशय है लोक अधिकारियों का सार्वजनिक सेवा के दौरान अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लॉबिंग की भूमिका निभाना, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में देखा गया है।
- जवाबदेही से जुड़ी चिंताएं: निजी क्षेत्रक से नियुक्त अधिकारियों को उनके छोटे कार्यकाल के कारण जवाबदेह ठहराना मुश्किल होगा।
- जमीनी स्तर के अनुभव की कमी: प्रशासनिक नियमों के लिए विविध अनुभवों की आवश्यकता होती है, न कि केवल विशिष्ट कौशल की। साथ ही, उनके लिए स्थानीय गतिशीलता को समझना भी महत्वपूर्ण होता है।
- राजनीतिक हस्तक्षेप: चयन प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप से भाई-भतीजावाद और पक्षपात की संभावना उत्पन्न हो सकती है।
आगे की राह
निम्नलिखित कदमों को अपनाते हुए लेटरल एंट्री की प्रक्रिया में सुधार करके रिक्तियों की कमी को दूर किया जा सकता है। साथ ही, इससे अधिकारियों की क्षमता और योग्यता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।
- लोक प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना: यह सिविल सेवा से जुड़ने के आकांक्षी लोगों का एक बड़ा समूह तैयार कर सकता है। साथ ही, यह सेवारत नौकरशाहों को देश की अर्थव्यवस्था व अलग-अलग क्षेत्रकों से संबंधित विशेषज्ञता हासिल करने तथा बेहतर प्रबंधकीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बना सकता है।
- निजी क्षेत्रक में प्रतिनियुक्ति: निजी क्षेत्रक में IAS और IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से डोमेन आधारित विशेषज्ञता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सकती है।
- प्रत्येक विभाग के लिए लक्ष्य निर्धारण और ट्रैकिंग को संस्थागत बनाना: प्रत्येक मंत्रालय और सरकारी एजेंसी को स्पष्ट समय-सीमा के साथ परिणाम-आधारित लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।
- अधिकारियों की भूमिका में एकरूपता लाने के लिए, क्षमता निर्माण आयोग और मिशन कर्मयोगी का उपयोग करके मिड-करियर ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं।
- सिविल सेवाओं में करियर प्रबंधन को बढ़ावा देना: सिविल सेवकों को शुरुआती वर्षों में विविध क्षेत्रकों में ज्ञान प्राप्त करने तथा उसके बाद उनकी रुचियों वाले विशिष्ट डोमेन में विशेषज्ञता प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- इसके अलावा, उनकी रुचि के क्षेत्र में उनके द्वारा अधिक विशेषज्ञता हासिल करने के लिए उन्हें अध्ययन अवकाश भी प्रदान किया जाना चाहिए।
- दो-स्तरीय प्रवेश प्रक्रिया: पूर्व RBI गवर्नर डी. सुब्बाराव ने IAS में दो-स्तरीय प्रवेश प्रक्रिया की सिफारिश की थी, पहले सामान्य रूप से 25-30 वर्ष की आयु वर्ग के लिए और उसके बाद लेटरल एंट्री के जरिए 37-42 वर्ष के आयु वर्ग के लिए।
- इस तरह की मध्य-स्तरीय भर्ती से विविध क्षेत्रकों से विशेषज्ञों को सिविल सेवाओं में शामिल किया जा सकता है।



