सुर्ख़ियों में क्यों?
हाल ही में, रूस के कजान शहर में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। यह पहला ऐसा शिखर सम्मेलन था जिसमें ब्रिक्स के विस्तार के बाद नए सदस्य देश भी शामिल हुए।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में
- कज़ान घोषणा-पत्र को अपनाया गया: इस अवसर पर "कज़ान घोषणा-पत्र: न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना (Kazan Declaration: Strengthening Multilateralism for Just Global Development and Security)" को अपनाया गया।
- इसके अलावा, 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता और ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए ब्राजील को पूर्ण समर्थन देने की बात कही गई।
ब्रिक्स के बारे में
- उत्पत्ति: BRIC शब्द का इस्तेमाल ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ' नील ने 2001 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए किया था।
- BRIC ने 2006 में G-8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के अवसर पर एक औपचारिक समूह के रूप में कार्य करना आरंभ किया था। पहला BRIC शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में आयोजित किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के साथ ही BRIC, ब्रिक्स/ BRICS बन गया।
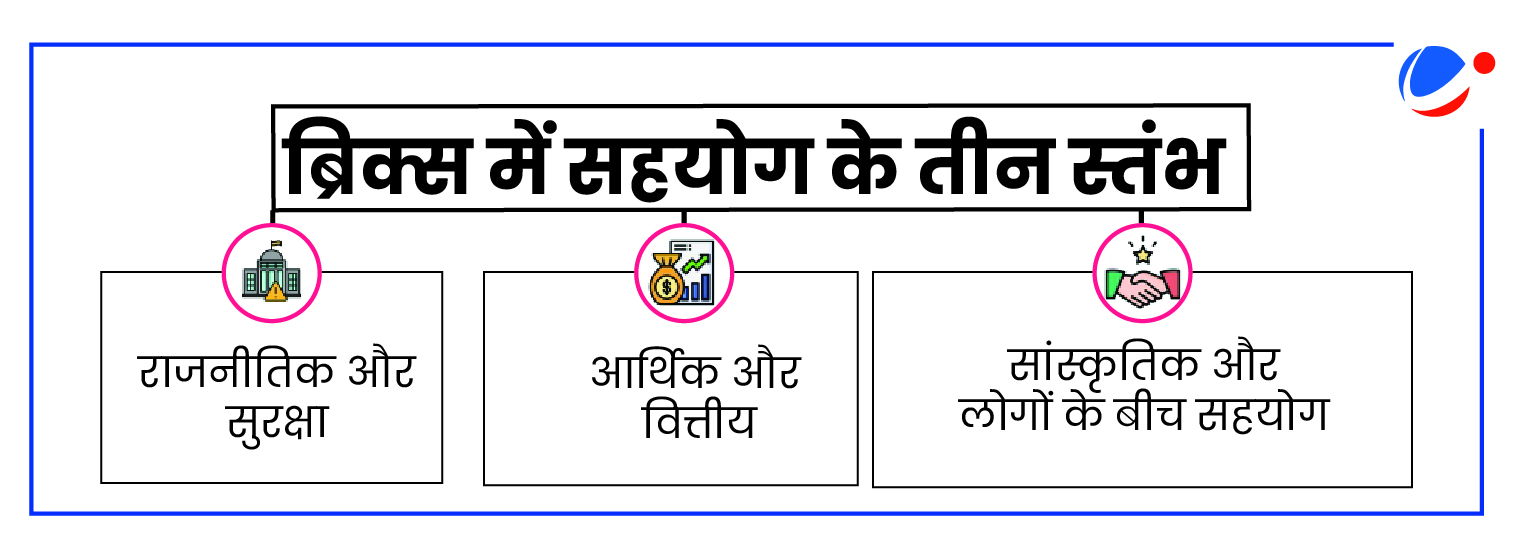
- सदस्य (10):
- आरंभिक पांच सदस्य (ब्रिक्स): ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साऊथ अफ्रीका; तथा
- पांच नए सदस्य (ब्रिक्स+): मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात।
- ब्रिक्स प्रतिनिधित्व करता है:
- विश्व की जनसंख्या का 45% हिस्सा ब्रिक्स देशों में रहता है।
- वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में यूरोपीय संघ के 14.5% और G-7 के 29.3% की तुलना में ब्रिक्स देशों का हिस्सा 37.3% है।
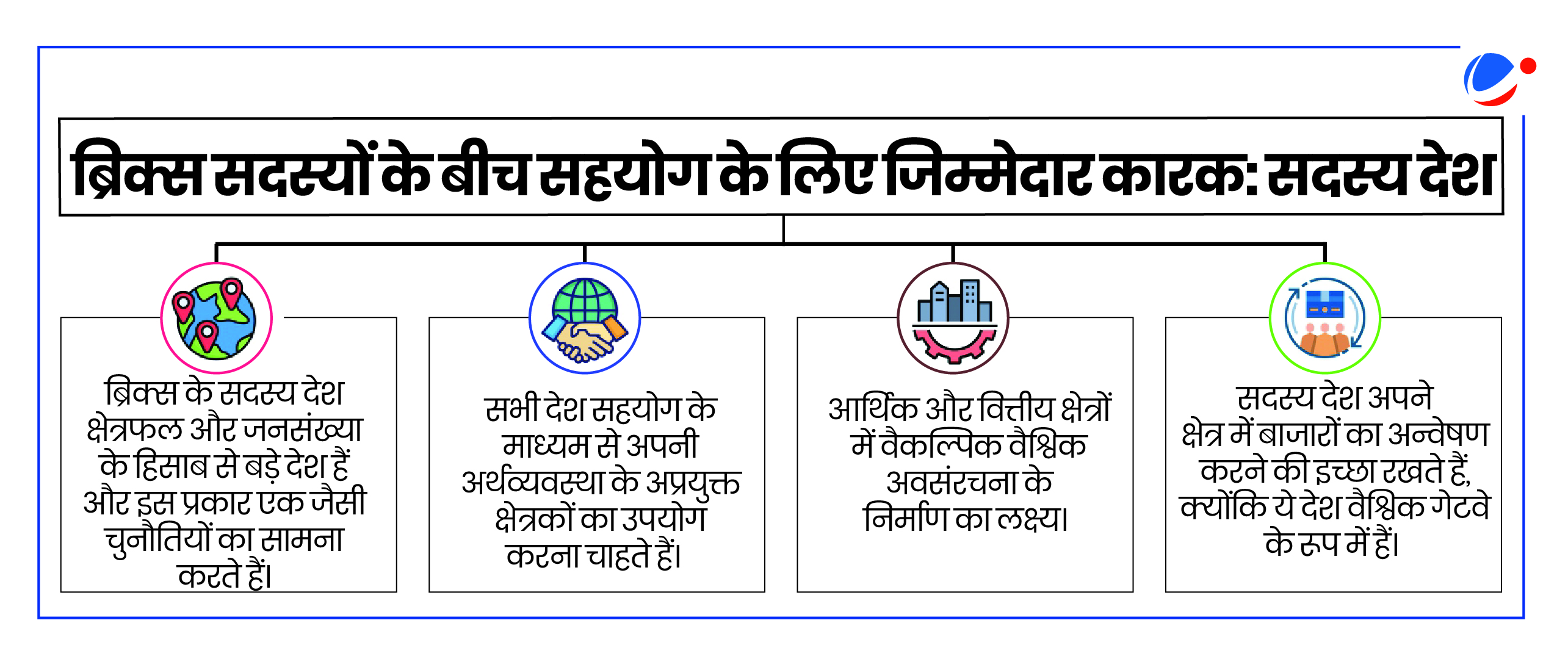
ब्रिक्स की महत्वपूर्ण पहलें:
क्षेत्र | पहलें |
वित्तीय |
|
| ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति |
|
सुरक्षा |
|
विज्ञान और प्रौद्योगिकी |
|
समकालीन विश्व में ब्रिक्स की प्रासंगिकता
- ऊर्जा सुरक्षा: ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे सदस्यों सहित ब्रिक्स देश विश्व के लगभग 44% क्रूड ऑयल का उत्पादन करते हैं।
- ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति: ब्रिक्स आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में कार्य करते हुए विकासशील देशों की चिंताओं को उठाने और उनके अधिकारों का समर्थन करने के लिए भारत को एक मंच प्रदान करता है।
- वार्ता के लिए सुरक्षित स्थान: ब्रिक्स भारत को द्विपक्षीय तनाव (भारत-चीन डोकलाम गतिरोध) के दौरान भी वार्ता में शामिल होने और संभावित प्रतिद्वंद्विता का प्रबंधन करने के लिए तटस्थ मंच प्रदान करता है।
- बहुपक्षीय संस्थानों में सुधारों की मांग को बढ़ावा देना: यह भारत को समान वैश्विक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) और WTO जैसे संस्थानों में सुधारों पर जोर देने की अनुमति देता है।
- उल्लेखनीय है कि इथियोपिया और ईरान को छोड़कर, सभी ब्रिक्स+ देश WTO के सदस्य हैं।
ब्रिक्स से जुड़ी चुनौतियां
ब्रिक्स का गठन सदस्य देशों के दीर्घकालिक सामान्य आर्थिक हितों में निहित था, लेकिन विविध चुनौतियों के कारण यह अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंच पाया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- आर्थिक क्षमता का कम उपयोग: उदाहरण के लिए-
- ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार: हालांकि, ब्रिक्स देशों का सामूहिक रूप से वैश्विक व्यापार में 18% हिस्सा है, परन्तु ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार 2.2% (2022 तक) के निचले स्तर पर बना हुआ है। व्यापार में चीन का भौगोलिक अलगाव और प्रभुत्व एक प्रमुख मुद्दा है।
- ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (CrRA): इसका प्रस्ताव 2018 में दिया गया था, लेकिन सदस्यों के बीच आम सहमति की कमी के कारण इसे अब तक नहीं अपनाया गया है।
- विडॉलरीकरण: ईरान, रूस और चीन जैसे कुछ सदस्य अब अपनी-अपनी मुद्रा में व्यापार करते हैं। हालांकि, एक साझा ब्रिक्स+ मुद्रा पर वार्ता चल रही है, लेकिन विशेषज्ञ खासकर ब्रिक्स समूह के हालिया विस्तार के साथ इसे असंभावित मानते हैं।
- वैकल्पिक वैश्विक वित्तीय संस्थान बनाने में असमर्थता: न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के पास विश्व बैंक और IMF या एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) के समान पहुंच एवं प्रभाव हासिल करने के लिए आवश्यक धन की कमी है। AIIB को 2013 में चीन द्वारा शुरू किया गया था।
- AIIB विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (ADB) आदि के साथ परियोजनाओं का सह-वित्तपोषण करता है। इसके विपरीत, NDB में सीमित भागीदारी और सह-वित्तपोषण व्यवस्था है।
- वैश्विक संस्थानों को प्रभावित करने में असमर्थता: उदाहरण के लिए, ब्रिक्स+ देशों के पास विश्व बैंक (IBRD) के भीतर सामूहिक रूप से केवल 19% वोटिंग पॉवर है, जबकि G-7 देशों के पास लगभग 40% और EU-27 के पास लगभग 23% वोटिंग पॉवर है।
- दूसरी ओर, भारत और ब्राजील 2023 में IBRD ऋण के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता थे, फिर भी उन्होंने पूंजी का केवल 5% योगदान दिया। यह असंतुलन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मानकों और नीतियों को प्रभावित करने के ब्रिक्स+ के प्रयासों को कमजोर करता है।
- समूह के भीतर एकजुटता का अभाव: ब्रिक्स सदस्यों के बीच भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता मौजूद है, जैसे भारत और चीन या सऊदी अरब और ईरान के बीच। यह प्रतिद्वंद्विता वैश्विक मुद्दों पर एक एकीकृत इकाई के रूप में कार्य करने की समूह की क्षमता को सीमित करती है।
- सदस्य अर्थव्यवस्थाएं अब तेजी से नहीं बढ़ रही हैं: उदाहरण के लिए- चीन इकोनॉमिक स्लोडाउन से जूझ रहा है, जबकि रूसी अर्थव्यवस्था में काफी समय से गिरावट जारी है। इसके अलावा, मौजूदा युद्ध रूसी अर्थव्यवस्था को और कमजोर बना सकता है।
- दक्षिण अफ्रीका भी उच्च बेरोजगारी और गंभीर शासन व्यवस्था तथा राजकोषीय चुनौतियों का सामना कर रहा है।
- पश्चिम विरोधी संगठन होने की धारणा: यह धारणा संभावित रूप से जलवायु परिवर्तन, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा जैसे साझा हित के क्षेत्रों में सहयोग को बाधित कर रही है।
- समान समूहों का अस्तित्व: उदाहरण के लिए- ब्रिक्स के विपरीत, जिसमें अलग-अलग प्रकार की राजनीतिक प्रणालियां शामिल हैं, IBSA में ऐसे लोकतांत्रिक देश शामिल हैं, जिनके लिए साझा एजेंडा तय करना और सहयोग को बढ़ावा देना आसान हो सकता है।
- इसी प्रकार, ब्रिक्स की तुलना में BASIC (बॉक्स देखें) को भी अधिक एकजुट समूह माना जाता है।
IBSA के बारे में
बेसिक/ BASIC के बारे में
|
आगे की राह
- स्पष्ट और साझा दृष्टिकोण विकसित करना: दीर्घकालिक लक्ष्यों व उद्देश्यों को रेखांकित करने से सदस्य देशों के विविध हितों को एकीकृत करने एवं एकता की भावना को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, एक स्थायी सचिवालय की स्थापना की भी जरूरत है।
- इस तरह के दृष्टिकोण से ब्रिक्स को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे मौजूदा वैश्विक संस्थानों के प्रभुत्व को चुनौती देने में मदद मिलेगी, जो पश्चिम से काफी प्रभावित हैं।
- सदस्यता मानदंड को परिभाषित करना: ब्रिक्स के लिए एक स्पष्ट सदस्यता मानदंड का समर्थन करने से भारत की इस संबंध में चिंताओं को कम करने में मदद मिलेगी कि ब्रिक्स के भावी सदस्य कौन हो सकते हैं।
- आम सहमति बनाना: मतभेदों को सुलझाने और सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाने के लिए कूटनीति एवं वार्ताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- संस्थागत क्षमताओं में वृद्धि करना: ब्रिक्स के संचालन का समर्थन करने तथा NDB, ब्रिक्स-पे आदि सहित इसकी पहलों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ब्रिक्स+ की संस्थागत क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- चीन के रणनीतिक प्रभाव को संतुलित करना: भारत को ब्रिक्स समूह में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अपनी आर्थिक कूटनीति को मजबूत करना होगा और रूस तथा ईरान जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को और गहरा करना होगा।
निष्कर्ष
ब्रिक्स+ की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि सदस्य आंतरिक मतभेदों को कितनी अच्छी तरह से दूर करते हैं, कैसे साझा आधार खोजते हैं और कैसी अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हैं। हालांकि, सदस्यता विस्तार वैश्विक गवर्नेंस में अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, परन्तु अभी इसकी क्षमताओं को साकार करने के लिए मजबूत सहयोग और प्रयास की आवश्यकता है।



