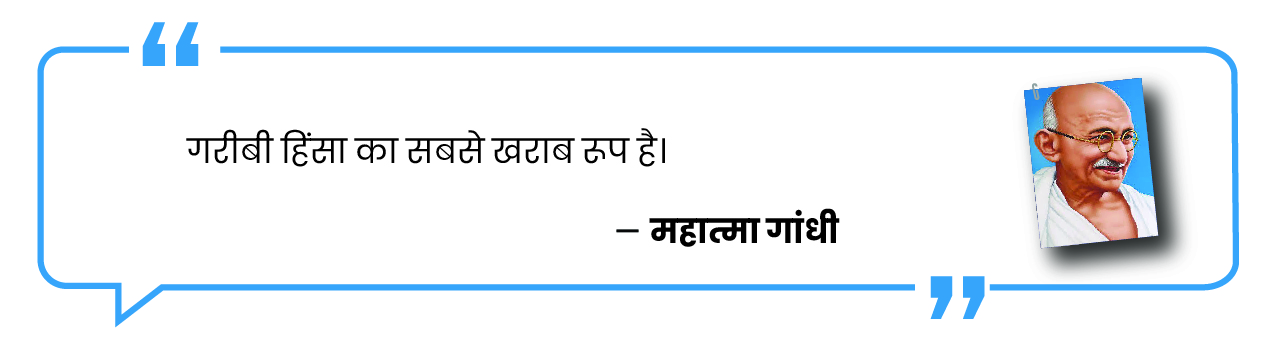सुर्ख़ियों में क्यों?
हाल ही में, विश्व बैंक ने 'पॉवर्टी, प्रोस्पेरिटी, एंड प्लैनेट रिपोर्ट 2024: पाथवेज आउट ऑफ द पॉलीक्राइसिस' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में आपस में जुड़े इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कोविड महामारी के बाद की वैश्विक प्रगति का पहला आकलन प्रस्तुत किया गया है।
भारत में निर्धनता की वर्तमान स्थिति (नीति आयोग के अनुसार)
|
रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:
- वैश्विक गरीबी में कमी के समक्ष बाधा: पॉलीक्राइसिस अथवा 'बहुसंकट' की वजह से पिछले 5 वर्षों के दौरान गरीबी में कमी की गति लगभग स्थिर हो गई है।
- पॉलीक्राइसिस एक ऐसी स्थिति है, जहां धीमी आर्थिक संवृद्धि, आर्थिक संकटों में बढ़ोतरी, जलवायु जोखिम और अधिक अनिश्चितता जैसे कई संकट एक ही समय में एक साथ पैदा हो जाते हैं। इसके चलते, राष्ट्रीय विकास रणनीतियों को लागू करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मुश्किल हो जाता है।
- लक्ष्यों की प्राप्ति न होना: ऐसा अनुमान है कि 2030 में विश्व की 7.3% आबादी चरम गरीबी में रह रही होगी जो विश्व बैंक के 3% के लक्ष्य से दोगुना से भी अधिक है। यह अनुमान संयुक्त राष्ट्र SDGs के गरीबी उन्मूलन लक्ष्य से तो काफी दूर है।
- 2024 में विश्व की 8.5% आबादी चरम गरीबी में जी रही है।
- वैश्विक समृद्धि में अंतर: वैश्विक समृद्धि में कोविड महामारी के बाद से प्रगति अवरुद्ध हो गई है। यह समावेशी इनकम ग्रोथ में गिरावट को उजागर करता है।
- समृद्धि अंतर (Prosperity Gap): विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया समृद्धि अंतर यह दर्शाता है कि विश्व की आबादी को एक दिन में 25 डॉलर की न्यूनतम आय (समृद्धि का बुनियादी स्तर) तक पहुंचाने के लिए कितने अतिरिक्त धन की आवश्यकता है। यह संकेतक वैश्विक आय असमानता को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है।
- भारत: चरम गरीबी में रहने वाले भारतीयों की संख्या 431 मिलियन (1990) से घटकर 129 मिलियन (2024) रह गई है।
- वर्तमान में, विश्व बैंक, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2.15 डॉलर से कम पर जीवन यापन को चरम गरीबी के रूप में परिभाषित करता है।
भारत में निर्धनता आकलन का इतिहासस्वतंत्रता के पूर्व
स्वतंत्रता के पश्चात्
2000 के बाद
|
भारत में निर्धनता के कारण
- ऐतिहासिक कारण: शोषणकारी औपनिवेशिक शासन ने स्थानीय उद्योगों को नष्ट कर दिया था। इससे विऔद्योगीकरण हुआ और धन की निकासी हुई, जिसके परिणामस्वरूप गरीबी बढ़ी।
- उदाहरण के लिए- ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारत को कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बना दिया था। इससे किसानों और कारीगरों की आय प्रभावित हुई।
- कृषि उत्पादकता में कमी: भूमि जोत का आकार छोटा होने, पूंजी की कमी और पारंपरिक कृषि पद्धतियों पर निर्भरता के कारण उपज कम होती है।
- उदाहरण के लिए- विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में फसलों की कम उपज किसानों की आय को प्रभावित करती है।
- जनसंख्या विस्फोट: भारत की तीव्र जनसंख्या वृद्धि ने संसाधनों और सेवाओं पर दबाव बढ़ा दिया है। इससे देश की आबादी में गरीबी के अनुपात में वृद्धि हुई है।
- उदाहरण के लिए- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक कार्य विभाग (UNDESA) के अनुसार, भारत की जनसंख्या 2060 के दशक के प्रारंभ में 1.7 बिलियन हो जाएगी। साथ ही, यह आशंका भी व्यक्त की गई है कि इस पूरी शताब्दी में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा।
- आर्थिक असमानता: आय और संपत्ति के वितरण में असमानता ने संसाधनों को कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित कर दिया है, जिससे सापेक्ष गरीबी बढ़ी है। उदाहरण के लिए- ऑक्सफैम के अनुसार भारतीय आबादी के सबसे धनी 10% लोगों के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77% हिस्सा है।
- सामाजिक असमानताएं: जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानताएं सामाजिक अपवंचन (सोशल एक्सक्लूजन) को बढ़ावा देती हैं। उदाहरण के लिए- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, भारत में 53% महिलाएं घर की देखभाल की ज़िम्मेदारियों के कारण कार्य बल में शामिल नहीं हो सकी हैं।
- इसके अलावा, कठोर जातिगत व्यवस्था वंचित समूहों को संसाधनों और अवसरों की प्राप्ति को सीमित करती है। इससे कई पीढ़ियों तक गरीबी का दुष्चक्र जारी रहता है। इससे समान पीढ़ी (बचपन से वयस्क तक गरीबी में जीना) एवं अगली पीढ़ी तक गरीबी में बने रहने से समानता का स्तर प्राप्त करने में समस्या पैदा होती है।
- भौगोलिक असमानताएं: घने जंगल, पहाड़ी क्षेत्र या प्राकृतिक आपदाओं के खतरे वाले क्षेत्रों में गरीबी की दर अधिक होती है।
- उदाहरण के लिए- असम और बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ प्रतिवर्ष लाखों लोगों को विस्थापित करती है और उन्हें पूर्ण निर्धनता में धकेल देती है।
निर्धनता से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां
|
गरीबी से निपटने के लिए उठाए गए कदम
वहनीय स्वास्थ्य देखभाल सेवा | सामाजिक सुरक्षा और सशक्तीकरण | वित्तीय समावेशन और कल्याण | रोजगार और कौशल विकास | उद्यमशीलता
|
|
|
|
|
|
आगे की राह
- निर्धनता कम करने के लिए नीति आयोग के सुझाव:
- रोजगार-सृजन करने वाले सतत व तीव्र विकास को बढ़ावा: बेहतर रोजगार सृजन और सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करके सामाजिक व्यय को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। आयोग ने विशेष रूप से पूर्वी भारत में कृषि क्षेत्रक में दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता पर जोर दिया है।
- गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्रभावी बनाना: समावेशन और अपवंचन संबंधी त्रुटियों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ-साथ योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाकर ऐसा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए- जन धन योजना, आधार नंबर, मोबाइल यानी जैम (JAM) ट्रिनिटी का उपयोग।
- "अमर्त्य सेन के 'स्वतंत्रता के रूप में विकास' और क्षमता दृष्टिकोण" पर ध्यान केंद्रित करना: यह लोगों की क्षमताओं में निवेश करने की आवश्यकता पर बल देता है, जिसमें शिक्षा, कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनके लिए अवसरों और स्वतंत्रताओं को बढ़ाया जा सके। इससे नागरिकों का सशक्तीकरण होगा और गरीबी में कमी आएगी।
- उदाहरण के लिए- स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कौशल क्षमताओं को बढ़ाने से उनके उद्यमिता विकास को बढ़ावा मिलता है और शहरी गरीबी में कमी लाई जा सकती है।