सुर्ख़ियों में क्यों?
हाल ही में, हैदराबाद स्थित एक निजी कंपनी ने इसरो को 400 किलोग्राम वर्ग के दो सैटेलाइट सौंपे हैं। ये सैटेलाइट्स इसरो के आगामी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरीमेंट (SPADEX) में इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसे 2024 के अंत तक लॉन्च किया जाना है।
स्पेस डॉकिंग के बारे में
- स्पेस डॉकिंग में दो अंतरिक्ष यानों (मानवयुक्त या मानव रहित) को एकदम सटीक तरीके से एक-दूसरे के साथ भौतिक रूप से जोड़ा जाता है। इससे दोनों अंतरिक्ष यान ईंधन भरने, मरम्मत करने और चालक दल के आदान-प्रदान जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों के लिए एक इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं।
- इससे अंतरिक्ष कक्षाओं में अत्याधुनिक फैसिलिटी (जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन) का निर्माण और अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलती है।
- कुछ अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ डॉक करते हैं और अन्य स्टेशन के साथ बर्थ के माध्यम से जुड़ते हैं।
- डॉकिंग में, अंतरिक्ष यान स्वयं अपनी कक्षा और गति में आवश्यक बदलाव करके स्टेशन से जुड़ जाता है।
- बर्थिंग में, एस्ट्रोनॉट अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की रोबोटिक आर्म की मदद से अंतरिक्ष यान को जोड़ता है। इसके बाद, मिशन कंट्रोल पृथ्वी से नियंत्रण संभालता है और रोबोटिक आर्म को अंतरिक्ष यान को अटैचमेंट साइट तक ले जाने का निर्देश देता है।
स्पेस डॉकिंग एक्सपेरीमेंट (SPADEX) के बारे में
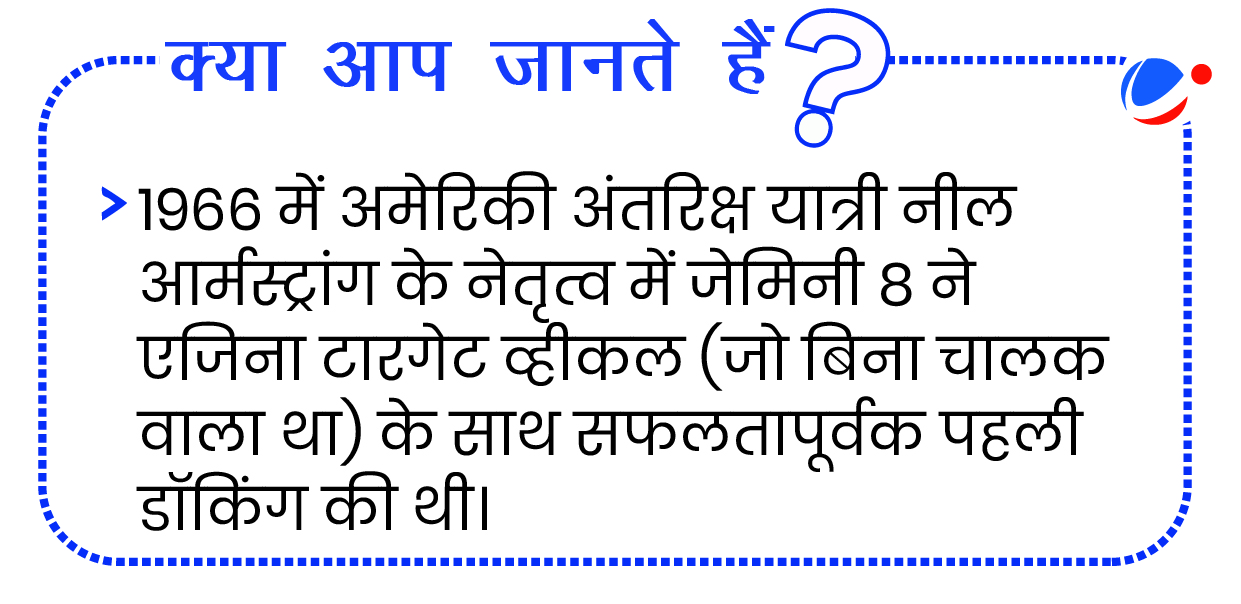
- इसरो का SPADEX (स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट) प्रौद्योगिकी प्रदर्शन संबंधी एक प्रयोग है। इसका उद्देश्य ऑटोनॉमस डॉकिंग में महारत हासिल करना है। यह अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षमता है, जिसे केवल कुछ गिने-चुने देश (जैसे- अमेरिका, रूस और चीन) ही विकसित कर पाए हैं।
- 'चेसर' और 'टारगेट' नामक दो उपग्रहों को एक ही PSLV द्वारा बहुत कम अंतराल पर स्थित अलग-अलग कक्षाओं (ऑर्बिट्स) में प्रक्षेपित किया जाएगा। तत्पश्चात इन्हें पृथ्वी से लगभग 700 कि.मी. की ऊंचाई पर डॉक किया जाएगा।
- ये उपग्रह लगभग 28,000 कि.मी./घंटा की गति से एक-दूसरे के साथ पूरी सटीकता से एक सीध में आते हुए डॉकिंग करेंगे। इसके परिणामस्वरूप वे एक एकल इकाई बनकर पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे।
- इस दौरान दोनों सैटेलाइट डॉकिंग के लिए अपनी कक्षा और गति जटिल बदलाव करेंगे:
- ऑटोनोमस रेंडेजवस और डॉकिंग: इस प्रक्रिया में अंतरिक्ष यान को एक-दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ऑटोनोमस नेविगेट, सटीक स्थान तक पहुंचना एवं सुरक्षित रूप से डॉक करना होगा।
- फॉर्मेशन फ्लाइंग: इसमें दोनों उपग्रहों के बीच सटीक सापेक्ष स्थिति को बनाए रखने हेतु सटीक कक्षीय नियंत्रण का प्रदर्शन किया जाएगा। यह भविष्य में अंतरिक्ष में उपग्रह या अंतरिक्ष स्टेशन को असेम्बल करने और उपग्रहों की सर्विसिंग के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है।
- रिमोट ऑपरेशन: इस मिशन के तहत डॉक्ड कॉन्फ़िगरेशन में एक उपग्रह को दूसरे उपग्रह के एटिट्यूड कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करके नियंत्रित करने का परीक्षण किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, यह अंतरिक्ष में संचालन और रखरखाव के लिए रोबोटिक आर्म प्रौद्योगिकियों के उपयोग की संभावना का भी पता लगाएगा।
इस मिशन का भारत के लिए महत्त्व
- अंतरिक्ष अन्वेषण: SPADEX भारत में विकसित स्केलेबल और लागत प्रभावी डॉकिंग तकनीक पर केंद्रित है, जो भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण संबंधी महत्वाकांक्षाओं के लिए आवश्यक है, जैसे कि-
- गगनयान: मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम
- चंद्रयान-4: चंद्रमा से सैंपल को धरती पर लाना,
- भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS): बाह्य अंतरिक्ष में स्थायी अवसंरचना का निर्माण करना, आदि।
- निजी क्षेत्रक की भागीदारी: 'इन-स्पेस (IN-SPACe)' का गठन अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्रक की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह किसी निजी कंपनी द्वारा असेम्बल किए गए सैटेलाइट का इसरो द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला उदाहरण है।
- भविष्य में प्रभाव: यह अंतरिक्ष आधारित अवसंरचनाओं के निर्माण और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ विदेशी मुद्रा अर्जन में भी मदद करेगा।
- अन्य संभावित उपयोग: इसमें भूस्थिर कक्षा में स्थित उपग्रहों का जीवन काल बढ़ाना; भविष्य के अंतरग्रहीय मिशन (जैसे मंगल ग्रह के लिए) में; सूर्य से बिजली पैदा करने के लिए अंतरिक्ष सौर स्टेशनों को असेंबल करने में, आदि शामिल हैं।
चुनौतियां
- जटिल डॉकिंग मैकेनिज्म: अत्यधिक तेज गति (लगभग 8-10 कि.मी. प्रति सेकंड) से यात्रा करने वाले उपग्रहों को डॉकिंग के लिए सटीक कम्यूनिकेश और कोर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है।
- नेविगेशन और नियंत्रण प्रणाली में किसी भी प्रकार की त्रुटि के परिणामस्वरूप टक्कर या डॉकिंग में विफलता हो सकती है। सुनीता विलियम्स के हालिया मिशन में हुई घटना इस बात का एक उदाहरण है।
- ऑटोमेटेड सिस्टम: कई जटिल कारकों जैसे- उपग्रहों की सापेक्ष गति और प्रक्षेप पथ आदि के कारण रियल टाइम में सटीकता के साथ डॉकिंग के लिए ऑटोनोमस सिस्टम का सफलतापूर्वक काम करना चुनौतीपूर्ण है।
- सेंसर की विश्वसनीयता: डॉकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सेंसर्स (जैसे- कैमरे, LIDAR और रडार) को अंतरिक्ष की कठोर दशाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
- अन्य चुनौतियां: इसमें अंतरिक्ष में मौजूद मलबे से खतरा, माइक्रोग्रैविटी का प्रभाव, डेटा ट्रांसफर और संचार का बने रहना आदि जैसे जटिल मुद्दे शामिल हैं।
निष्कर्ष
भारत द्वारा एडवांसड अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का विकास अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसी प्रगति वैज्ञानिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता के प्रति देश की प्रतिबद्धता एवं आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े अनुसंधान और विकास में अग्रणी बनने की भारत की आकांक्षाओं को दर्शाती है।



