सुर्ख़ियों में क्यों?
RBI ने स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स (SRVAs), UPI लिंकेज, करेंसी स्वैप समझौतों के माध्यम से रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर बल दिया है। इन क़दमों का उद्देश्य विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता को कम करना और वैश्विक डी-डॉलेराइजेशन में योगदान देना है।
डी-डॉलेराइजेशन क्या है?
- इसका उद्देश्य डॉलेराइजेशन (वैश्विक बाजार में अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक प्रभुत्व) को कमजोर करना है। ऐसा करने से वैश्विक व्यापार, रिजर्व मुद्रा के रूप में डॉलर की महत्ता और वित्तीय लेन-देन में इसके उपयोग में उल्लेखनीय कमी आएगी।

डी-डॉलेराइजेशन के प्रमुख कारण
- अमेरिका की आर्थिक शक्ति घट रही है, पर डॉलर का वर्चस्व बना हुआ है: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक GDP में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 45% थी जो वर्तमान में घटकर लगभग 25% रह गई है। इसके बावजूद डॉलर का प्रभुत्व बना हुआ है।
- डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता के नुकसान: अमेरिकी सरकार का भारी ऋण बोझ एवं 2023 में अमेरिकी ऋण के उच्चतम सीमा पर पहुंचने का संकट जैसी घटनाओं ने डॉलर की विश्वसनीयता को कमजोर किया है।
- अमेरिकी मौद्रिक नीति का नकारात्मक प्रभाव: फेडरल रिजर्व द्वारा उठाए गए कई कदमों (जैसे-2023 में ब्याज दरों में बढ़ोतरी) से कई देशों में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, ऋण की लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई और मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई।
- अमेरिकी डॉलर और पेमेंट क्लीयरिंग प्रणालियों का हथियार के रूप में उपयोग: वर्तमान में, लगभग 40 देशों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इनसे देशों की नीतियों और सरकार के संचालन पर असर पड़ता है।
- एक नई और अधिक लोकतांत्रिक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की आकांक्षा: डी-डॉलेराइजेशन के प्रयास एकध्रुवीय दुनिया से हटकर 'बहुध्रुवीय नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (New International Economic Order: NIEO)' की ओर बढ़ने की वैश्विक आकांक्षा को भी दर्शाते हैं।
- अमेरिका के बाहर सकारात्मक विकास: चीन में आर्थिक और राजनीतिक सुधारों जैसे कदम वैकल्पिक मुद्राओं की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं।
डी-डॉलेराइजेशन के समक्ष चुनौतियां
- अन्य विकल्पों की लागत: अमेरिकी डॉलर के बदले किसी अन्य मुद्रा पर निर्भरता बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रणालियों को अपडेट करने, अनुबंधों को समायोजित करने और व्यापार समझौतों पर दोबारा वार्ता करने पर भारी खर्च आएगा।
- बाजार में अस्थिरता: नई मुद्राएं अपनाने से बाजार में अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा हो सकती है। इससे वैश्विक व्यापार और निवेश प्रवाह प्रभावित हो सकता है।
- भू-राजनीतिक तनाव: अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने से राजनीतिक टकराव बढ़ सकता है। साथ ही, अमेरिका इस कदम को अपने आर्थिक प्रभाव के लिए चुनौती के रूप में देख सकता है।
- मुद्रा भंडार में विविधीकरण की चुनौतियां: वैकल्पिक मुद्राओं या स्वर्ण जैसी परिसंपत्तियों में रिजर्व रखने से नए खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। इसमें मुद्रा का अवमूल्यन या वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव आदि शामिल हैं।
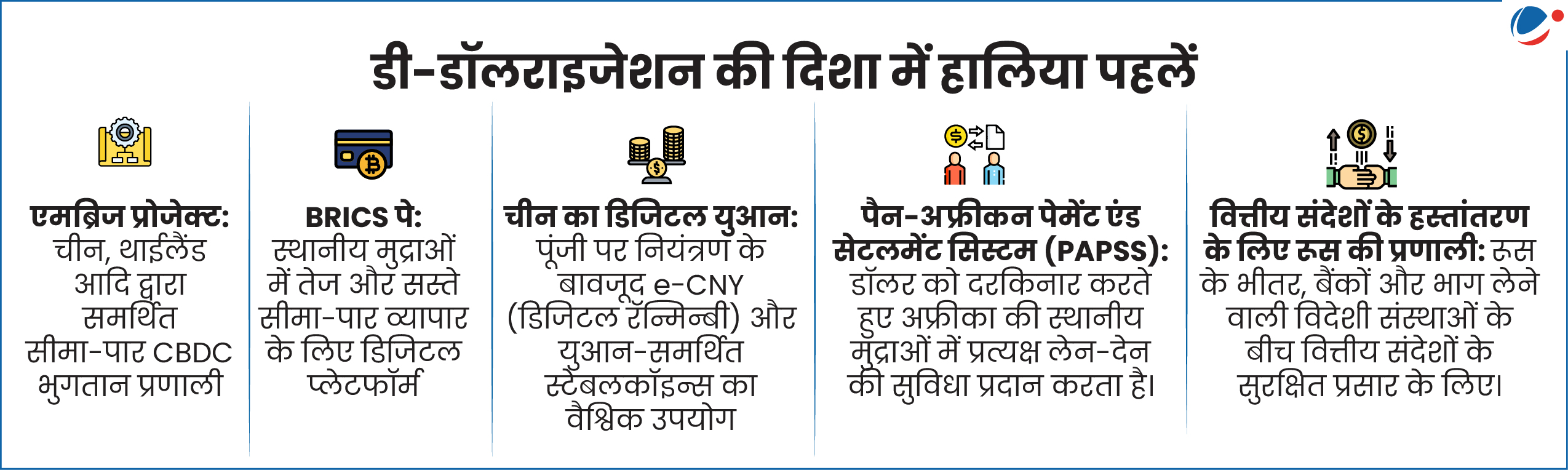
निष्कर्ष
भारत के मामले में, डी-डॉलेराइजेशन को रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण यानी रुपीफिकेशन से पूरा किया जा सकता है। इससे किसी भी संस्था को रुपया खरीदने और बेचने की पूरी स्वतंत्रता मिल जाएगी।



