सुर्ख़ियों में क्यों?
हाल ही में, IIT इंदौर द्वारा किए गए एक शोध में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन शहरों में दैनिक जीवन को एक नया रूप दे रहा है। कार्य, दिनचर्या और जीवनयापन की स्थितियों में निरंतर बदलाव ने शहरी प्रवासियों के सामने आने वाली व्यापक चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है।
प्रवासन क्या है?
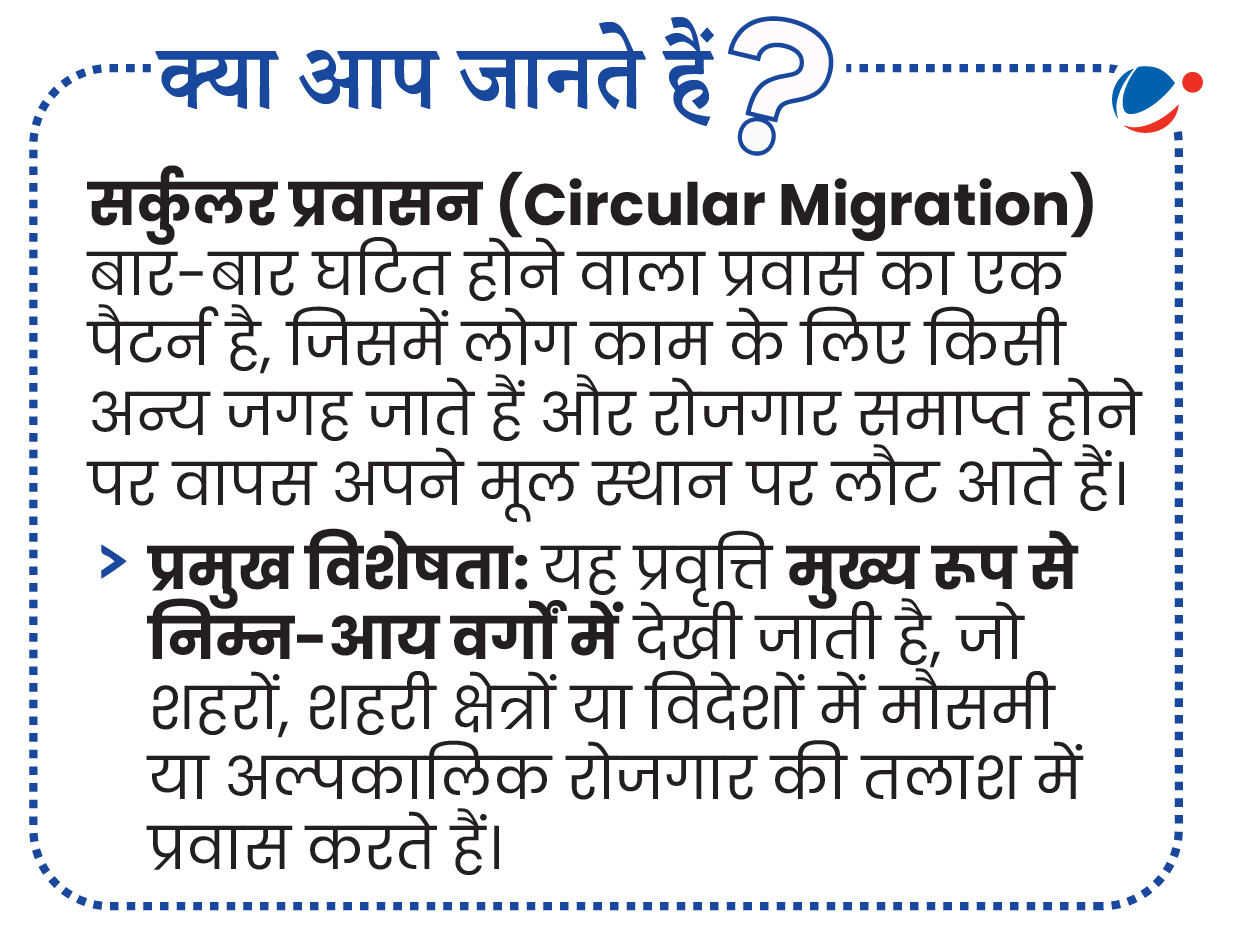
- अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (International Organisation for Migration: IOM) प्रवासन को लोगों के अपने सामान्य निवास स्थान से हटकर किसी नए निवास स्थान की ओर जाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है। यह निवास स्थान या तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा-पार हो सकता है या एक ही राज्य के भीतर हो सकता है।
- भारत में प्रवासी
- भारत की जनगणना प्रवासियों को जन्मस्थान (PoB) और उनके अंतिम निवास स्थान (PoLR) के आधार पर परिभाषित करती है।
- जन्मस्थान के मानदंड के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति का जन्मस्थान गणना स्थल (Enumeration place) से अलग है, तो गणना स्थल पर उस व्यक्ति को प्रवासी माना जाएगा।
- यदि किसी व्यक्ति का अंतिम निवास स्थान और गणना स्थल अलग है, तो गणना स्थल पर उस व्यक्ति को प्रवासी माना जाएगा।
- भारत की जनगणना प्रवासियों को जन्मस्थान (PoB) और उनके अंतिम निवास स्थान (PoLR) के आधार पर परिभाषित करती है।
भारत में प्रवासन की स्थिति
- शहरी प्रवासन: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर, 18.9% ग्रामीण से शहरी और 15.9% शहरी से शहरी प्रवासन हुआ है, जो कुल प्रवास का लगभग 35% है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक, भारत की 40% से अधिक जनसंख्या के शहरी क्षेत्रों में रहने की संभावना है।
- ग्राम से ग्राम प्रवासन 55% के साथ सबसे अधिक है, जबकि शहर से ग्राम प्रवासन 10% के साथ सबसे कम है।
- प्रवासियों का हिस्सा: 400 मिलियन ड्रीम्स! रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कुल आबादी में प्रवासियों की हिस्सेदारी कुल जनसंख्या के 28.88% (40.20 करोड़) थी, जो 2011 के 37.64% से कम है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, 45.57 करोड़ लोग प्रवासी हैं।
- पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से कुल बाहर जाने वाले प्रवासियों का हिस्सा लगभग 48% है, जबकि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आने वाले प्रवासियों का हिस्सा लगभग समान ही है।
- प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद - EAC-PM के अनुसार पश्चिम बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक में आने वाले प्रवासियों की दर सबसे तेजी से बढ़ रही है, जबकि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में घट रही है।
शहरी प्रवासन को बढ़ावा देने वाले कारक
- 2011 की जनगणना के अनुसार, ग्रामीण से शहरी प्रवास के प्रमुख कारण:
- विवाह (29%),
- परिवार के साथ स्थानांतरण (26%),
- कार्य (24%),
- जन्म के बाद स्थानांतरण (5.5%),
- शिक्षा (2%), और
- अन्य कारण (12%)
प्रवास को प्रभावित करने वाले दो प्रकार के कारक हैं-
| प्रतिकर्ष कारक (मूल स्थान छोड़ने के कारण) | अपकर्ष कारक (गंतव्य स्थल चुनने के कारण) |
सामाजिक और राजनीतिक |
|
|
जनसांख्यिकीय और आर्थिक |
|
|
पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी कारक |
|
|
शहरी प्रवास के परिणाम
- आर्थिक परिणाम
- आर्थिक विकास: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार कुशल प्रवासी विकास को बढ़ावा देते हैं, जबकि मौसमी और अस्थायी प्रवासी राष्ट्रीय GDP में लगभग 10% का योगदान करते हैं।
- जीवन स्तर में सुधार: धन प्रेषण आवास, भूमि, शिक्षा और व्यवसाय के माध्यम से जीवन स्तर को बढ़ाता है।
- आर्थिक सुभेद्यताएं: अनौपचारिक क्षेत्रक में संकेन्द्रण, कम वेतन, और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच की कमी प्रवासियों के लिए लगातार बनी रहने वाली चुनौतियां हैं।
- उदाहरण के लिए- भारत के कार्यबल का लगभग 90% हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रक में है, जहां अधिकांश प्रवासी कामगार कार्यरत हैं।
- उदाहरण के लिए- कोविड-19 के कारण भारत में लगभग 11.4 मिलियन प्रवासियों का वापस घर की ओर पलायन हुआ था।
- जनसांख्यिकीय परिणाम
- जनसंख्या संरचना: प्रवासन जनसंख्या संतुलन को बदल देता है, जिससे लिंगानुपात असंतुलित होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर घटती है।
- उदाहरण के लिए- महिलाओं के पलायन के कारण कोट्टायम का लिंगानुपात (1040) केरल के औसत लिंगानुपात (1084) से कम है।
- जनसंख्या संरचना: प्रवासन जनसंख्या संतुलन को बदल देता है, जिससे लिंगानुपात असंतुलित होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर घटती है।
- सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम
- सामाजिक परिवर्तन: प्रवासी नई सोच, तकनीक और उपभोक्तावादी संस्कृति के साथ आते हैं, जिससे मूल क्षेत्रों का आधुनिकीकरण होता है।
- सामाजिक चुनौतियां: इसमें जाति, धर्म और क्षेत्रीय मूल के आधार पर भेदभाव; भाषा संबंधी बाधाएं, घेट्टो (बस्तियों) का निर्माण आदि शामिल हैं।
- उदाहरण के लिए- महाराष्ट्र में 2008 में प्रवासियों पर हुए हमले।
- आवास और अवसंरचना पर दबाव: उदाहरण के लिए- पुणे में 564 झुग्गी-झोपड़ियां हैं, जिनमें अनुमानित 30-40% आबादी रहती है।
प्रवासी श्रमिकों के लिए सरकारी पहलें
|
आगे की राह
- प्रवासन पर कार्य समूह (2015) की सिफारिशें
- कानूनी और नीतिगत ढांचा:
- प्रवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय लागू करने चाहिए।
- प्रवासियों की जाति-आधारित गणना हेतु रजिस्ट्रार जनरल के प्रोटोकॉल में संशोधन किया जाना चाहिए।
- भेदभाव-रोधी उपाय: नौकरियों और सेवाओं के लिए निवास प्रमाण (Domicile) की शर्त को समाप्त करना चाहिए, ताकि आवागमन एवं निवास की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके।
- सर्व शिक्षा अभियान (SSA) की वार्षिक कार्य योजनाओं में प्रवासी बच्चों को शामिल करने जैसे मूलभूत अधिकारों तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए।
- वित्तीय समावेशन: अनौपचारिक धन हस्तांतरण को रोकने के लिए इंडिया पोस्ट के नेटवर्क का उपयोग करके प्रेषण की लागत को कम करना चाहिए।
- कानूनी और नीतिगत ढांचा:
- सर्वोत्तम प्रथाओं का विस्तार करना: 1998 से हर पांच साल में आयोजित किए जाने वाले केरल प्रवासन सर्वेक्षण मॉडल का देश भर में विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि प्रवासन के गवर्नेंस और नीतिगत प्रतिक्रियाओं को मजबूत किया जा सके।



