सुर्ख़ियों में क्यों?
हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन (UN Convention on Biological Diversity: UNCBD) के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन (COP16) कोलंबिया के कैली में संपन्न हुआ।
अन्य संबंधित तथ्य
- इस वर्ष के सम्मेलन की थीम थी: "प्रकृति के साथ शांति (Peace with Nature)"।
- यह कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (KMGBF) को अपनाने के बाद UNCBD के पक्षकारों का पहला सम्मेलन था। यह KMGB फ्रेमवर्क की प्रगति का आकलन करने और उसके सामने आ रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।
UNCBD के बारे में
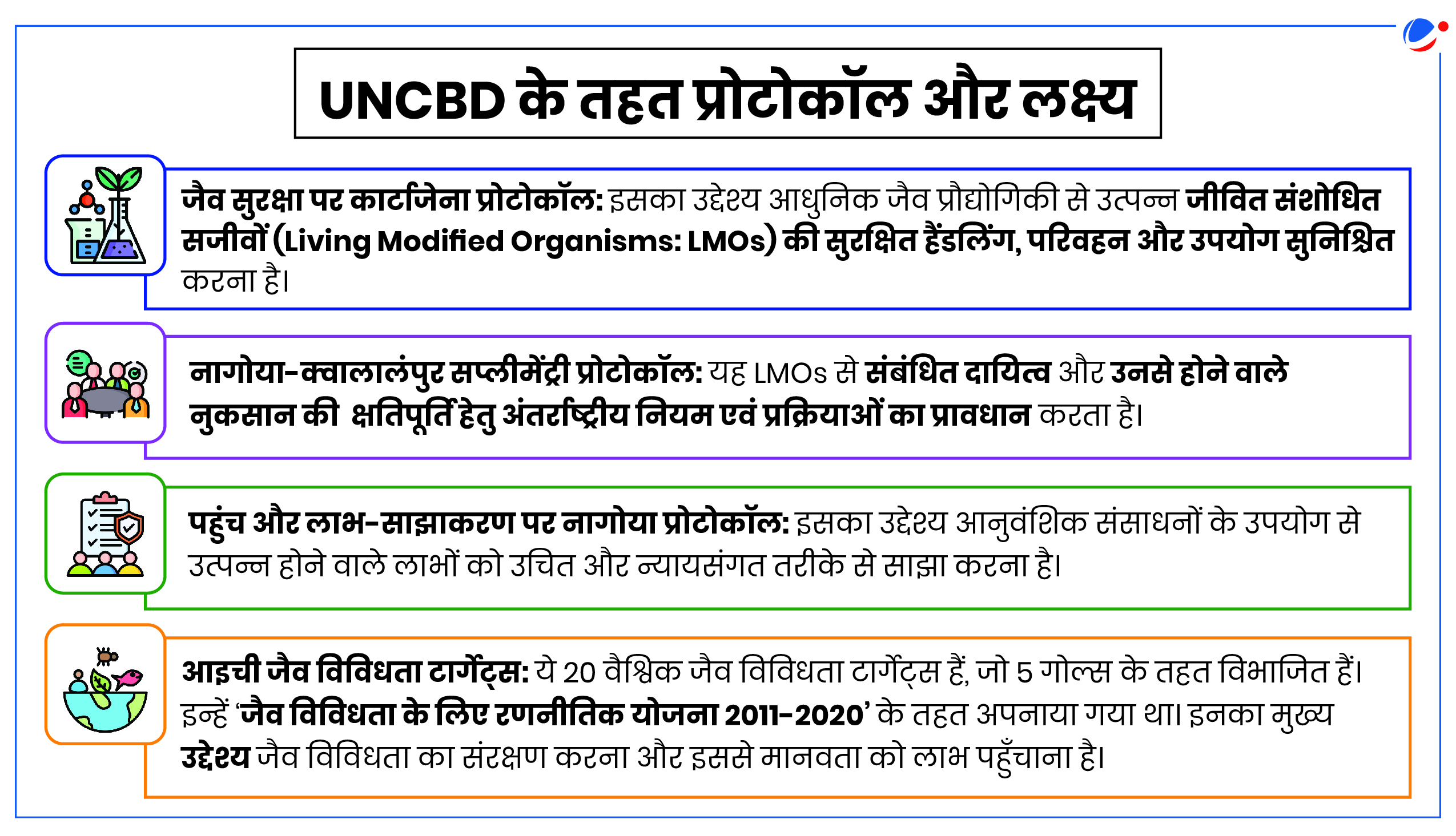
- उत्पत्ति: UNCBD कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन (United Nation's Conference on Environment and Development: UNCED) के दौरान अपनाया गया था। UNCED को "पृथ्वी शिखर सम्मेलन" के रूप में भी जाना जाता है।
- यह 1993 में लागू हुआ और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के तहत कार्य करता है।
- उद्देश्य: जैव विविधता का संरक्षण करना; इसके अलग-अलग घटकों का संधारणीय तरीके से उपयोग करना; तथा आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से मिलने वाले लाभों का उचित एवं न्यायसंगत साझाकरण सुनिश्चित करना।
- सचिवालय: मॉन्ट्रियल, कनाडा
- सदस्य: इसकी अभिपुष्टि 196 सदस्य देशों द्वारा की गयी है (भारत 1994 में इस कन्वेंशन का पक्षकार बना)।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि नहीं की है।
- संचालन तंत्र: COP की बैठक हर दो साल में (द्वि-वार्षिक) आयोजित की जाती है। इस बैठक में जैव विविधता के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की जाती है, प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती है एवं विभिन्न कार्य योजनाओं को लागू करने के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया जाता है।
कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (KMGBF) के बारे में
|
COP16 के प्रमुख आउटकम्स
- DSI के लिए वित्तीय तंत्र: जैविक संसाधनों पर DSI के उपयोग से होने वाले लाभों को अधिक निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से साझा करने के लिए कैली फंड की शुरुआत की गई है।
- DSI से व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने वाली कंपनियों को अपने लाभ का 1% (राजस्व का 0.1%) देशज लोगों और स्थानीय समुदायों की सहायता में खर्च करना होगा।
- देशज समुदायों के अधिकारों को मान्यता: UNCBD के अनुच्छेद 8(j) के तहत एक स्थायी सहायक निकाय की स्थापना और कैली फंड की शुरुआत से सभी कन्वेंशन प्रक्रियाओं में देशज लोगों की भागीदारी बढ़ाई जा सकेगी।
- कैली फंड का कम-से-कम 50% हिस्सा देशज समुदायों, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के नेतृत्व में उनके द्वारा ही निर्धारित विकास परियोजनाओं के लिए समर्पित होगा।
- वित्तीय संसाधन जुटाना: ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (GEF) के अंतर्गत कुनमिंग जैव विविधता फंड (KBF) की शुरुआत की जाएगी। इससे KMGBF के लक्ष्यों और टारगेट्स को हासिल करने हेतु त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।
- इससे पहले COP15 में, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड (GBFF) पर सहमति बनी थी, जिसकी स्थापना GEF द्वारा की गई थी।
- पारिस्थितिकी या जैविक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों (Ecologically or Biologically Significant Marine Areas: EBSAs) की पहचान: EBSAs की पहचान और मौजूदा EBSAs को अपडेट करने के लिए नए और विकसित तंत्रों की स्थापना पर सहमति बनी है।
- यह KMGBF के 30-बाई-30 टार्गेट्स और बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन (BBNJ) समझौते (हाई सी ट्रिटी) के लिए महत्वपूर्ण है।
- थीमैटिक एक्शन प्लान: इसका उद्देश्य विकासशील देशों और स्थानीय समुदायों के लिए सिंथेटिक बायोलॉजी के क्षेत्र में क्षमता विकास एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि में मौजूद असमानताओं को दूर करना है।
- आक्रामक विदेशज प्रजातियों का प्रबंधन: KMGBF के टारगेट्स के अनुरूप नए डेटाबेस, बेहतर सीमा-पार व्यापार विनियमन आदि के माध्यम से आक्रामक विदेशज प्रजातियों के प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- वैश्विक जैव विविधता और स्वास्थ्य कार्य योजना (Global Action Plan on Biodiversity and Health) पर सहमति: इस रणनीति में जूनोटिक रोगों के उद्भव को रोकने, गैर-संचारी रोगों की रोकथाम आदि के लिए 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण को अपनाया गया है।
COP16 में भारत की प्रतिबद्धता
|
COP16 की कमियां
- संसाधन एवं वित्त जुटाना: विकसित देश 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वित्त-पोषण में प्रतिवर्ष 20 बिलियन डॉलर उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने में पिछड़ गए।
- इसके अलावा, COP16 में GBFF (ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड) के लिए केवल 163 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।
- KMGBF के लिए निगरानी फ्रेमवर्क: KMGBF को लागू करने में हुई प्रगति को ट्रैक करने के लिए निगरानी फ्रेमवर्क और इसके संकेतकों को अपडेट करने और पूरा करने का निर्णय नहीं लिया गया है।
- योजना, निगरानी, रिपोर्टिंग और समीक्षा (Planning, Monitoring, Reporting, and Review: PMRR) तंत्र में देरी: ये तंत्र KMGBF टारगेट्स के मामले में वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति की समीक्षा की प्रक्रियाएं स्थापित करते हैं।
- NBSAPs की प्रस्तुति: 196 सदस्य देशों में से केवल 44 देशों ने KMGBF के अनुरूप अपने अपडेटेड NBSAPs प्रस्तुत किए हैं। साथ ही, 119 देशों ने केवल अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों की रिपोर्ट सौंपी है (जो NBSAP तैयार करने का पहला चरण है)।
- कैली फंड (DSI फंड): हालांकि यह फंड शुरू हो गया है, लेकिन इसमें योगदान और वित्तीय एवं तकनीकी संसाधनों के आवंटन के तरीकों पर सहमति नहीं बन पाई है।
- जैव विविधता क्रेडिट और ऑफसेट्स पर असहमति: KMGBF ने जैव विविधता संरक्षण के लिए वित्तीय संसाधन में वृद्धि करने के लिए इन्हें 'नवाचार योजना (Innovative scheme)' के रूप में शामिल किया, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन सकी है।
निष्कर्ष
2026 में आर्मेनिया की राजधानी येरेवान में होने वाले COP17 के लिए रोडमैप निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित है:
- KMGBF के टारगेट 19 के तहत वित्तीय तंत्र को मजबूत करना, जिसके लिए अगली अंतरिम बैठक बैंकॉक में होगी।
- जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क और PMRR तंत्र को मजबूत करना।
- NBSAPs को समयबद्ध कार्य योजनाओं के साथ बेहतर बनाना, जो पेरिस समझौते के तहत NDCs के अनुरूप हों।
साथ ही, वैश्विक सहयोग, समावेशी साझेदारी, और तकनीकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना 2030 तक KMGBF टारगेट्स को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
डिजिटल अनुक्रम जानकारी (Digital Sequence Information: DSI) के बारे मेंहाल ही में सम्पन्न हुए COP16 में, CBD के तहत कैली फंड को कार्यान्वित किया गया। इसका उद्देश्य जैविक संसाधनों के DSI के उपयोग से उत्पन्न लाभों को अधिक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से साझाकरण सुनिश्चित करना है। यह CBD के तीसरे उद्देश्य यानी जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करने से संबंधित है। DSI के बारे में
DSI का महत्त्व:
DSI के समक्ष चुनौतियां:
DSI के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलें
|





