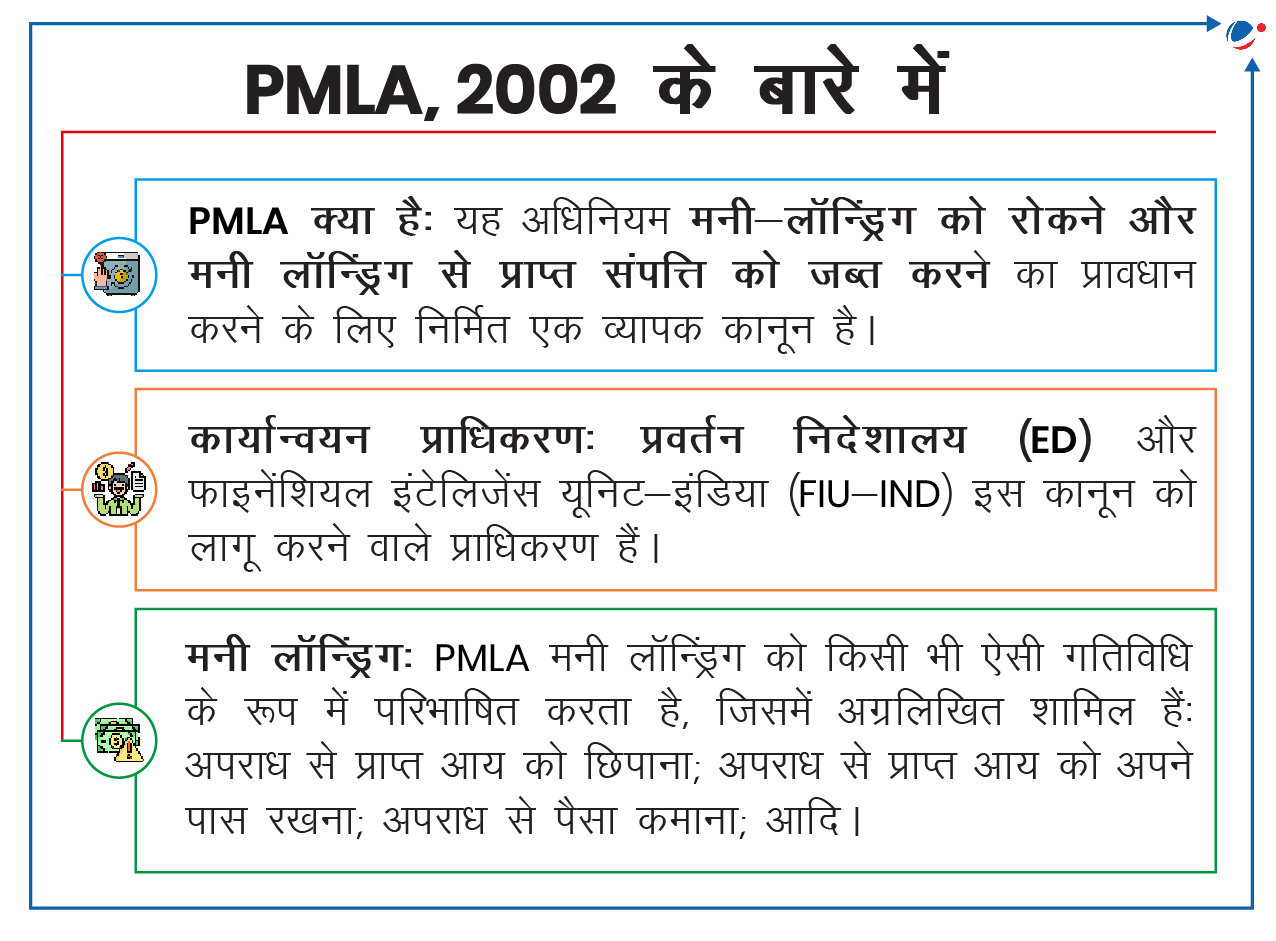हाल ही में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (GRAI) 2023 जारी किया।
GRAI के बारे में
- अवधारणा: इसे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश पर DARPG ने शुरू किया है।
- यह सूचकांक 4 आयामों और 11 संकेतकों पर केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा अपनाए गए शिकायत निवारण तंत्र का आकलन करता है।
- ये 4 आयाम हैं- दक्षता, फीडबैक, डोमेन और संगठनात्मक प्रतिबद्धता।
- उद्देश्य: अलग-अलग संगठनों में शिकायत निवारण तंत्र के सबल पक्ष एवं सुधार वाले क्षेत्रों को रेखांकित करना।
- रैंकिंग: 2023 की रैंकिंग में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग सबसे ऊपर है। उसके बाद पदस्थापन विभाग ग्रुप A है।
Article Sources
1 sourceहाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया।
- इस एप्लिकेशन को भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने विकसित किया है। इस ऐप की मदद से पंजीकरण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी ।
CRS के बारे में:
- CRS व्यक्ति के जीवन से जुड़ी मुख्य घटनाओं, जैसे कि जन्म, मृत्यु और मृत बच्चे के जन्म तथा इनसे संबंधित विवरणों को दर्ज करने हेतु एक एकीकृत प्रणाली है। इसमें इन घटनाओं और विवरणों का निरंतर और स्थायी रूप से पंजीकरण करना अनिवार्य है।
- जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार, सभी जन्म और मृत्यु को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत किया जाना चाहिए।
- इसका संचालन भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के अधीन किया जाता है।
- इसे संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची में शामिल किया गया है।
राष्ट्रपति ने ‘भारत में जेल: जेल मैनुअल की मैपिंग और सुधार तथा कैदियों की संख्या कम करने के उपाय’ रिपोर्ट जारी की।
- यह रिपोर्ट भारत के सुप्रीम कोर्ट की शोध शाखा, सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ने तैयार की है। यह रिपोर्ट भारत की जेल प्रणाली की जटिलताओं को उजागर करने का प्रयास करती है। इसमें प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:
- रूढ़िवादिता: जेल मैनुअल्स में आवश्यक सफाई और मैला साफ करने के कार्य को "हीन" या "अपमानजनक" माना जाता है। यह श्रम के संबंध में एक पदानुक्रमित दृष्टिकोण को बनाए रखता है।
- जमानत अस्वीकृति: जमानत आवेदनों की अस्वीकृति दर उच्च है। सत्र न्यायालयों में 32.3% और मजिस्ट्रेट न्यायालयों में 16.2% जमानत आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाते हैं।
- धीमी सुनवाई: 2023 में 52% से अधिक ऐसे मामले साक्ष्य चरण में लंबित थे, जहां आरोपी एक वर्ष से अधिक समय से हिरासत में हैं।
- अन्य: जेलों में हाथ से मैला उठाने की प्रथा का जारी रहना; जाति व्यवस्था के आधार पर जेल में कार्यों का विभाजन; खुली जेलों का कम उपयोग आदि।
- उल्लेखनीय है कि जाति व्यवस्था के आधार पर जेल में कार्यों के विभाजन को सुकन्या शांता मामले में असंवैधानिक घोषित किया गया है।
जेल सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग
- ई-प्रिज़न्स: इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने विकसित किया है। यह जेल और कैदियों के प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों को एकीकृत करने पर केंद्रित है।
- मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम, 2023: इसमें कैदियों को जेल से छुट्टी देने की शर्त के रूप में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रावधान किया गया है।
- सुप्रीम कोर्ट की फास्टर/ FASTER (फ़ास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स) प्रणाली: इसने अदालतों से जेल तक जमानत आदेशों के पहुंचने में होने वाली देरी को कम किया है।
- इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS): यह अदालतों, पुलिस और जेलों के बीच एक स्वचालित चैनल बना सकता है तथा हिरासत के मामलों में होने वाली अनुचित देरी को कम कर सकता है।
हाल ही में, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ली।
- राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को पद की शपथ दिलाई।
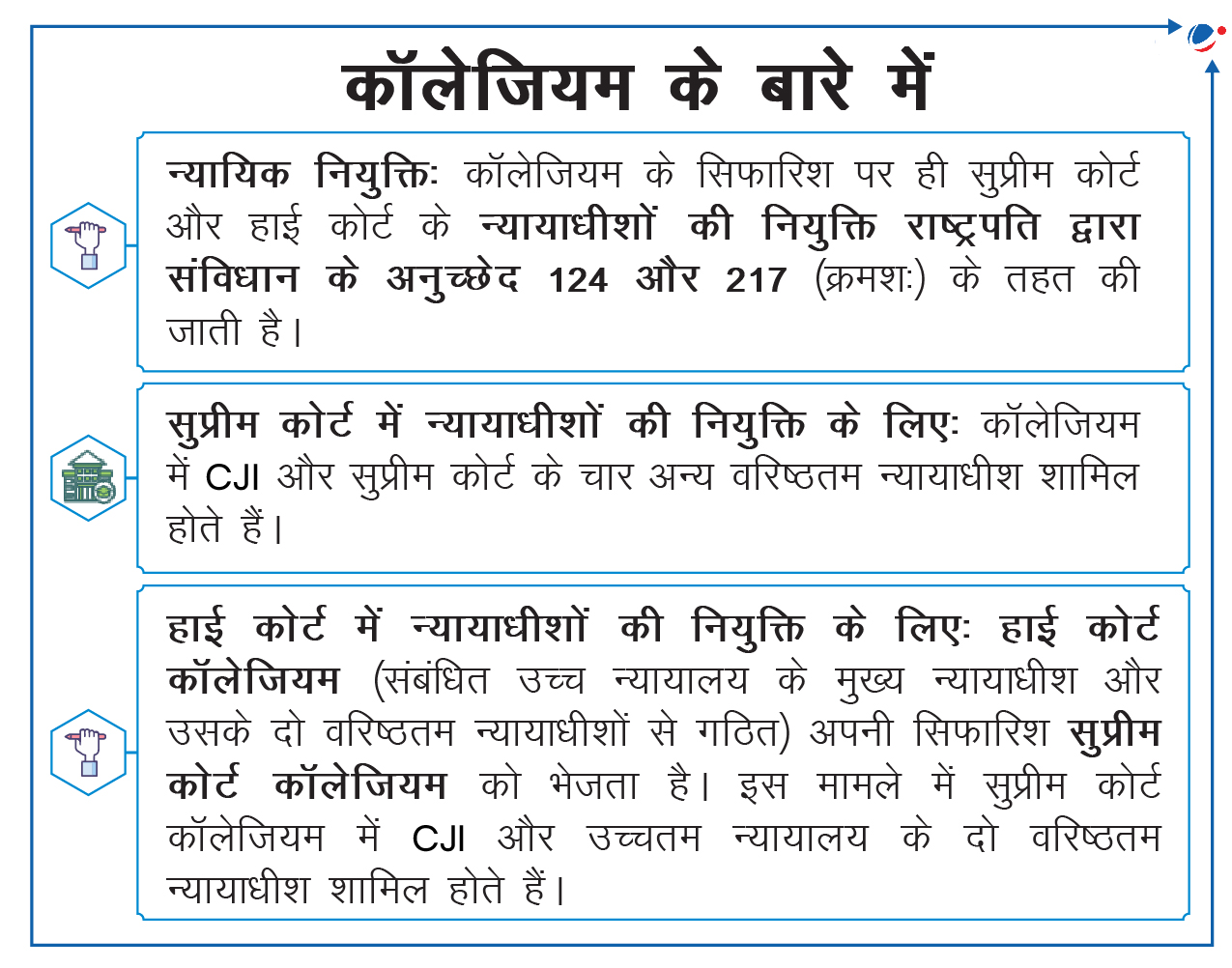
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति के बारे में
- आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर CJI के रूप में नियुक्त किया जाता है।
- हालांकि, इस परंपरा का 1964, 1973 और 1977 में उल्लंघन किया गया था।
- इस संबंध में केंद्रीय विधि और न्याय कार्य मंत्री सिफारिश मांगते हैं, जिसे फिर प्रधान मंत्री के पास भेजा जाता है। अंत में प्रधान मंत्री CJI की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत, सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बना रहेगा।
CJI की प्रमुख भूमिका
- फर्स्ट अमंग इक्वल्स: राजस्थान राज्य बनाम प्रकाश चंद (1997) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि CJI न्यायपालिका का प्रमुख होता है और एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाता है। हालांकि, CJI को सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की तुलना में कोई उच्चतर न्यायिक प्राधिकार प्राप्त नहीं होता है।
- मास्टर ऑफ़ दी रोस्टर: केसों की सुनवाई के लिए पीठों (संविधान पीठों सहित) का गठन करना CJI का अनन्य अधिकार है।
- कॉलेजियम का प्रमुख: CJI, उच्चतर न्यायपालिका में न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम का प्रमुख होता है।
- सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति: संविधान के अनुच्छेद 146 के तहत यह CJI या उसके द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा।
हाल ही में, अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया।
अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में
- यह एक मंच है, जहां केंद्र और राज्य सरकारें एक-दूसरे के साथ समन्वय एवं सहयोग करती हैं।
- स्थापना: इसकी स्थापना सरकारिया आयोग की सिफारिश पर की गई थी। इसे राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से 1990 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत की गई है।
- संरचना: इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-
- अध्यक्ष: प्रधान मंत्री
- सदस्य:
- सभी राज्यों के मुख्यमंत्री;
- विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक; तथा
- केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री, जिन्हें प्रधान मंत्री द्वारा नामित किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से इनकार करने वाले अपने फैसले को पलट दिया।
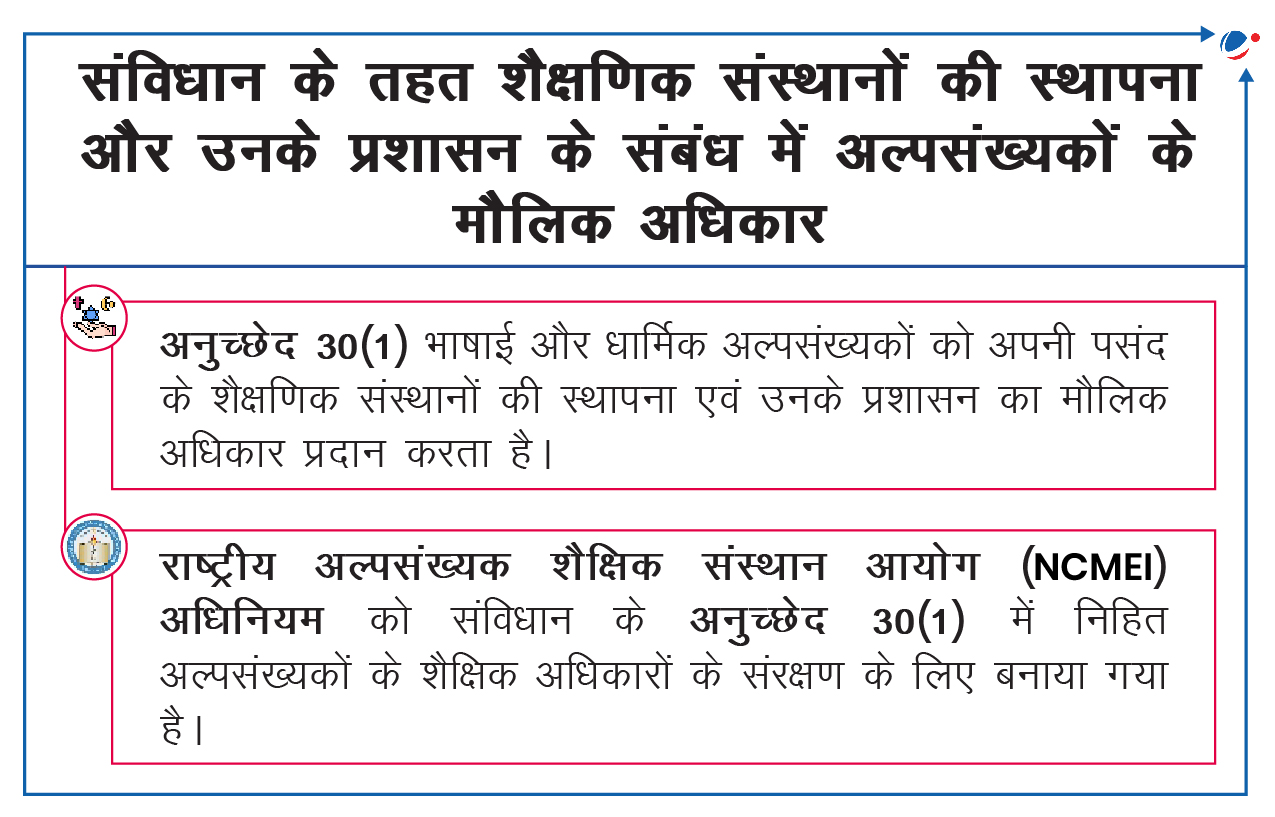
- सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने 4-3 बहुमत से एस. अजीज बाशा बनाम भारत संघ वाद (1967) के अपने फैसले को पलट दिया। 1967 के निर्णय में कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि इसे एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था।
- सुप्रीम कोर्ट ने एस. अजीज बाशा बनाम भारत संघ वाद (1967) में कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) न तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किया गया था और न ही इसका संचालन मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा किया जाता है। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसे AMU अधिनियम 1920 के तहत स्थापित किया गया था।
- हालांकि बाद में, संसद ने AMU (संशोधन) अधिनियम, 1981 के माध्यम से AMU का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल कर दिया था।
- हालांकि, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2006 में AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को रद्द कर दिया था। इस निर्णय को बाद में 2019 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले में स्थापित सिद्धांतों के आधार पर संविधान के 'अनुच्छेद 30 के तहत AMU के अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे को' नियमित पीठ के पास भेज दिया है।
इस निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र
- यह साबित करने के लिए कि कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, इसके लिए उसके प्रशासन पर अल्पसंख्यकों का नियंत्रण होना अनिवार्य नहीं है।
- कोर्ट को संस्थान की उत्पत्ति का पता लगाना चाहिए और संस्थान की स्थापना करने वाले की मंशा की पहचान करनी चाहिए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि संस्था की स्थापना किसने की है।
- किसी संस्थान का अल्पसंख्यक का दर्जा केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता, कि इसकी स्थापना किसी कानून द्वारा या विश्वविद्यालय के रूप में की गई है।
- जो समुदाय संविधान के लागू होने से पहले अल्पसंख्यक नहीं थे, वे भी स्वतंत्रता से पहले स्थापित संस्थाओं के लिए अनुच्छेद 30(1) के तहत संरक्षण के हकदार हैं।