सुर्ख़ियों में क्यों?
विश्व बैंक ने "बेंचमार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट" रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में विश्व की 140 अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के विनियामकीय परिदृश्य का विश्लेषण किया गया है।
रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र
- लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (Public Fiscal Management System: PFMS): केवल 19 देशों ने विशिष्ट बजटिंग, रिपोर्टिंग और लेखांकन प्रावधानों को अपनाया है।
- पारदर्शिता में कमी: केवल 22 प्रतिशत मामलों में ही कॉन्ट्रैक्ट में किए गए किसी प्रकार के संशोधनों का ऑनलाइन प्रकाशन किया गया।
- निगरानी एवं मूल्यांकन: केवल 37 प्रतिशत अर्थव्यवस्थाओं ने "प्रदर्शन के अनुसार भुगतान (Payments linked to performance)" प्रणाली को अपनाया है।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और भारत में PPP के अलग-अलग मॉडल्स के बारे मेंPPP वास्तव में सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने या बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकारों और निजी कंपनियों के बीच एक प्रकार का सहयोग है।
भारत में PPP के अलग-अलग मॉडल्स
|
भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल की आवश्यकता क्यों है?
- पर्याप्त अवसंरचना नहीं: भारत में परिवहन, ऊर्जा और शहरी विकास में बड़ी संख्या में अवसंरचनाओं के विकास की आवश्यकता है।
- उदाहरण के लिए- PPP मॉडल के तहत विकसित मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का उद्देश्य निजी निवेश को आकर्षित करते हुए यातायात की भीड़ को कम करना और तटीय क्षेत्रों तक आवागमन को बढ़ाना है।
- संसाधन जुटाने के लिए: सरकार के पास अक्सर बड़ी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है। ऐसे में PPP परियोजनाएं सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से वित्त-पोषण जुटाने में सहायता करती हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक की 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कई राज्यों का राजकोषीय घाटा 3% से अधिक है। इस वजह से उनके पास अवसंरचनाओं के विकास के लिए फंड कम पड़ जाता है।
- दक्षता और इनोवेशन: निजी क्षेत्रक की भागीदारी दक्षता और इनोवेशन को बढ़ाती है।
- उदाहरण के लिए- दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में ऑटोमेटेड चेक-इन और बेहतर बैगेज हैंडलिंग जैसी सुविधाओं के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है।
- जोखिम साझा करना: PPP मॉडल में नुकसान का वहन सार्वजनिक और निजी संस्था, दोनों साझा करते हैं। इससे परियोजना को जारी रखने में मदद मिलती है क्योंकि किसी एक पर बोझ नहीं पड़ता है।
- सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना: अवसंरचना विकास के क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए PPP मॉडल महत्वपूर्ण है।
- SDGs प्रत्यक्ष तौर पर सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना क्षेत्रों से जुड़े हैं।
- सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करना: निजी क्षेत्रक के साथ सहयोग करने से सरकार विनियमन और निगरानी पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, जिससे सेवा वितरण को और अधिक बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
- उदाहरण के लिए- भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन के पुनर्विकास में PPP मॉडल की मदद ली गई है।
भारत में PPP के समक्ष कौन-कौन सी चुनौतियां मौजूद हैं?
- विनियामकीय मुद्दे: केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अनुसार, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों, पर्यावरण मंजूरी में देरी, आदि के कारण 449 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत में कुल 5.01 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है (मार्च, 2024 में)।
- वित्त-पोषण की समस्या: अवसंरचना के विकास में अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है और इसमें जोखिम भी अधिक होता है। इसलिए ऐसी परियोजनाओं के लिए फंड जुटाने में समस्या आती है।
- उदाहरण के लिए- राष्ट्रीय अवसंरचना योजना के लिए अगले पांच वर्षों में 111 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है।
- दीर्घकालिक कॉन्ट्रैक्ट संबंधी मुद्दे: 20-30 वर्षों तक चलने वाली परियोजनाओं से "अप्रासंगिक सौदेबाजी (Obsolescing bargains)" की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतिगत या आर्थिक परिवर्तनों के कारण निजी क्षेत्रक ऐसी परियोजनाएं या कारोबार में अपनी सौदेबाजी की क्षमता को खो देता है।
- विवाद समाधान तंत्र: विवाद समाधान के लिए प्रभावी तंत्र नहीं होने की वजह से परियोजना की गुणवत्ता एवं हितधारकों की प्रतिबद्धता कम होती है। इससे परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होती है और यह समय पर पूर्ण भी नहीं होती है।
- राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं की भागीदारी: सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों को अक्सर सरकारी संस्थाओं के रूप में देखा जाता है। इससे PPP में इन संस्थाओं की भागीदारी कम दिखती है।
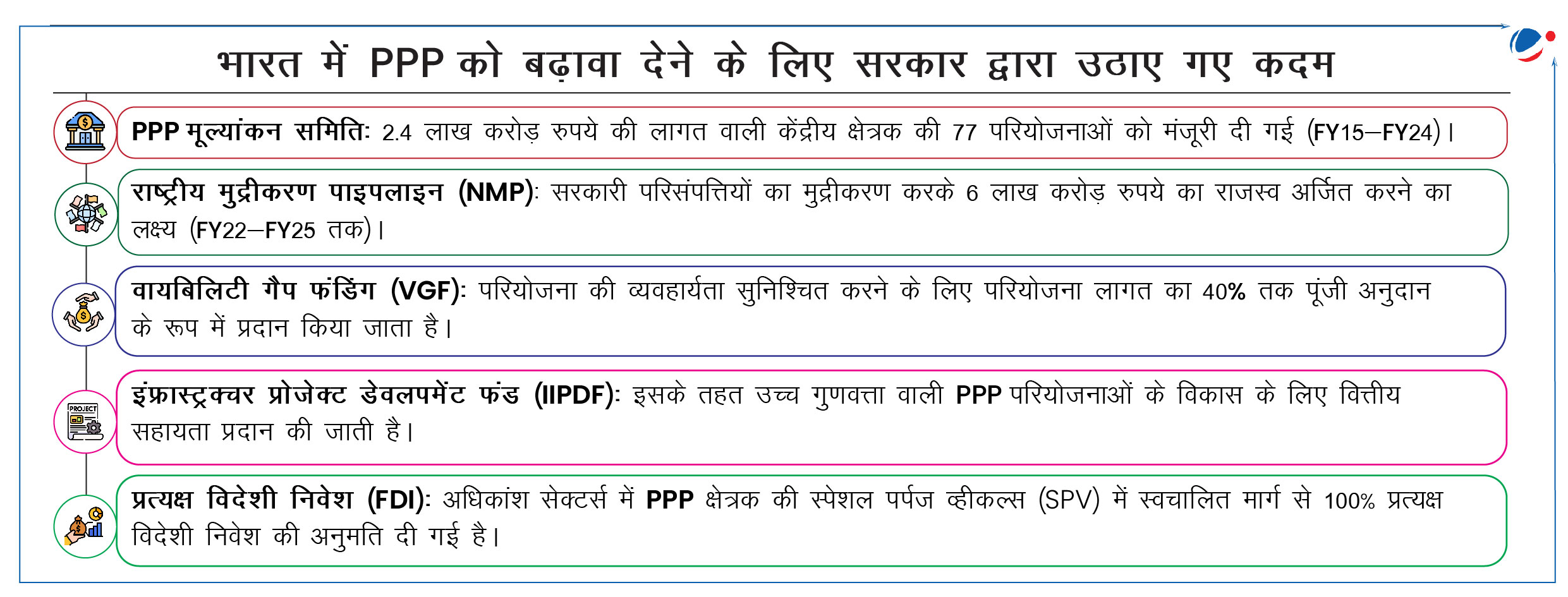
भारत में PPP में सुधार के लिए आगे की राह (विजय केलकर समिति के अनुसार)
- सेवा वितरण पर फोकस करना: कॉन्ट्रैक्ट में केवल वित्तीय लाभ अर्जित करने की बजाय सेवा वितरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- जोखिम प्रबंधन: अत्याधुनिक मॉडलिंग अपनाकर जोखिम प्रबंधन दक्षता और परियोजना के लाभकारी होने का आकलन किया जाना चाहिए।
- विशेषज्ञ तंत्र: जटिल समस्याओं को सुलझाने और अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए PPP परियोजना समीक्षा समिति और ट्रिब्यूनल की स्थापना की जानी चाहिए।
- कानून में संशोधन: निर्णय लेने में हुई वास्तविक त्रुटियों और भ्रष्टाचार के कृत्यों के बीच अंतर करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन की आवश्यकता है।
- एक PPP संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए और परियोजनाओं को समय पर मंजूरी देने के लिए राष्ट्रीय सुविधा समिति (National Facilitation Committee) का गठन किया जाना चाहिए।
- स्वतंत्र विनियमन: अलग-अलग क्षेत्रकों के लिए एक स्वतंत्र विनियामक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। साथ ही, सड़कों और बंदरगाहों से संबंधित परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने की भी जरूरत है।





