सुर्ख़ियों में क्यों?
हाल ही में अंकुश विपन कपूर बनाम NIA मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की शक्तियां केवल NIA अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट अपराधों की जांच करने या ऐसे "अनुसूचित अपराध" करने वाले आरोपी व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं हैं।
अन्य संबंधित तथ्य
- इस निर्णय ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें पाकिस्तान से भारत में हेरोइन की तस्करी में शामिल एक आरोपी को दी गई जमानत रद्द कर दी गई थी।
- इस मामले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS एक्ट) के तहत किए गए अपराध शामिल थे। इन अपराधों को NIA अधिनियम में अनुसूचित अपराधों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।
- यह मामला मादक पदार्थों की तस्करी, हवाला चैनलों और आतंकवाद के वित्त-पोषण से जुड़ा था।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- सुप्रीम कोर्ट ने NIA के प्राधिकार के पक्ष में निर्णय दिया। इससे यह साफ हो गया है कि एजेंसी अनुसूचित अपराधों से जुड़े गैर-अनुसूचित अपराधों की जांच भी कर सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने NIA अधिनियम की धारा 8 की समग्र रूप से व्याख्या की।
- NIA अधिनियम की धारा 8: इसके तहत किसी भी अनुसूचित अपराध की जांच करते समय, एजेंसी उस अन्य अपराध की भी जांच कर सकती है, जिसे आरोपी ने कथित तौर पर किया है, यदि वह अपराध कहीं-न-कहीं अनुसूचित अपराध से जुड़ा हुआ है।
- NIA निम्नलिखित शर्तों पर किसी अन्य आरोपी की जांच भी कर सकती है, भले ही वह किसी अनुसूचित अपराध के लिए जांच के दायरे में न आता हो-
- NIA की राय: यदि NIA को लगता है कि किसी अन्य आरोपी द्वारा किया गया अपराध अनुसूचित अपराध से जुड़ा हुआ है, तो उसकी भी जांच की जानी चाहिए।
- केंद्र सरकार की मंजूरी: NIA को अपनी राय केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी, जो जांच को अधिकृत कर सकती है।
- संयुक्त जांच: किसी भी अन्य आरोपी की जांच, जहां तक संभव हो, अनुसूचित अपराध से संबंधित आरोपी की चल रही जांच के साथ संयुक्त रूप से की जानी चाहिए।
NIA निम्नलिखित कानूनों के तहत अपराधों की जांच करती है:
1A. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962
(a) भारतीय दंड संहिता का अध्याय VI (b) भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVI की धारा 370 और 370A (c) भारतीय दंड संहिता की धारा 489-A से 489-E (दोनों सम्मिलित) (d) शस्त्र अधिनियम, 1959 के अध्याय V की धारा 25 की उपधारा (1AA) (e) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अध्याय XI की धारा 66F |
राष्ट्रीय जांच एजेंसी या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के बारे में
- स्थापना: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की स्थापना 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद अधिनियमित NIA अधिनियम, 2008 के तहत की गई थी।
- उद्देश्य: NIA का मुख्य उद्देश्य उन अपराधों की जांच करना और मुकदमा चलाना है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा तथा अखंडता को खतरा पहुंचाते हैं। साथ ही, विदेशी राज्यों के साथ देश के मित्रतापूर्ण संबंधों एवं अंतर्राष्ट्रीय संधियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।
- अपराधों की अनुसूची: इस अधिनियम में उन कानूनों की एक अनुसूची शामिल है जिनके तहत NIA अपराधों की जांच कर सकती है और उन पर मुकदमा चला सकती है (ऊपर दिए गए बॉक्स में देखें)।
- मुख्यालय: NIA का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा गुवाहाटी और जम्मू में इसके दो क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
- अध्यक्ष: NIA का अध्य्क्ष एक महानिदेशक (DG) होता है, जो भारतीय पुलिस सेवा (IPS) का एक वरिष्ठ अधिकारी होता है।
- अधिकार क्षेत्र: NIA का अधिकार क्षेत्र पूरे भारत में फैला हुआ है और यह निम्नलिखित पर भी लागू होता है:
- भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पर;
- सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों पर, चाहे वे कहीं भी हों;
- भारत में पंजीकृत जहाजों और विमान में सवार व्यक्तियों पर, चाहे वे कहीं भी हों;
- उन व्यक्तियों पर जिन्होंने भारत के नागरिकों के खिलाफ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले अनुसूचित अपराध किए हैं आदि।
- NIA की शक्तियां:
- जांच: यदि केंद्र सरकार को लगता है कि कोई अनुसूचित अपराध हुआ है, तो वह NIA को जांच करने का निर्देश दे सकती है।
- अभियोजन: NIA के पास विशेष रूप से नामित NIA न्यायालयों में मामलों पर मुकदमा चलाने का अधिकार है।
- राज्य पुलिस के साथ समन्वय: NIA जांच के दौरान राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है।
- राज्यक्षेत्रातीत (Extraterritorial) कार्रवाइयां: एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समझौतों के अधीन, भारत के बाहर किए गए अपराधों की जांच कर सकती है और मुकदमा चला सकती है।
- दोषसिद्धि दर: NIA ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक 640 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से 147 मामलों में अदालतों द्वारा फैसला सुनाया गया है तथा इनमें दोषसिद्धि दर 95.23% है।
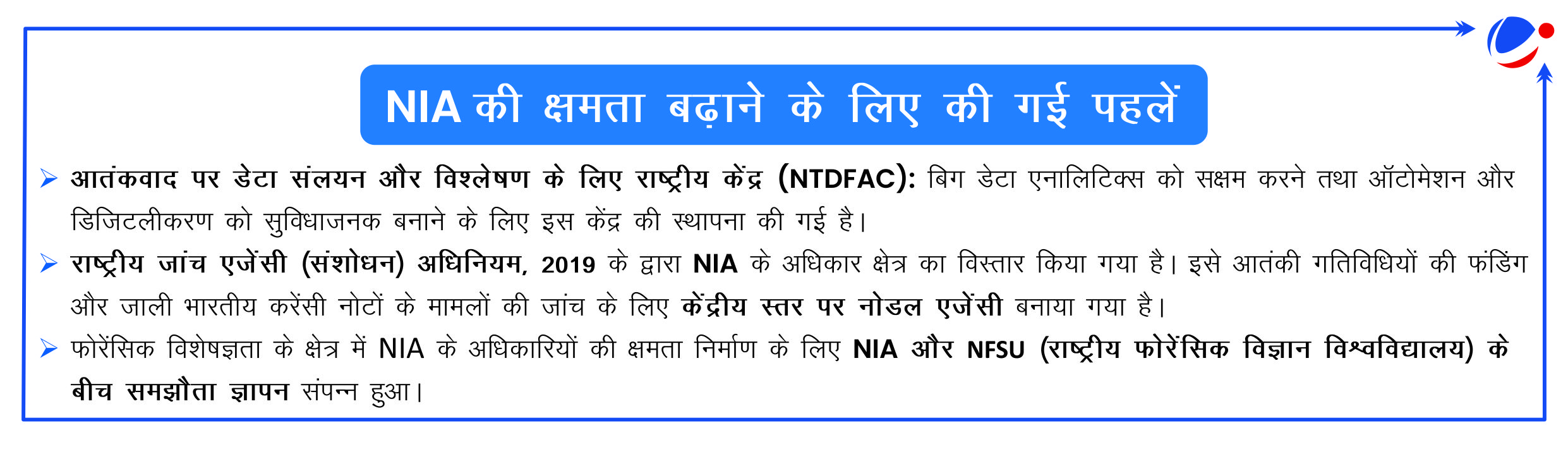
निष्कर्ष
जैसे-जैसे NIA विकसित हो रही है, इसके लिए नए चुनौतियों का सामना करना तथा राज्य और विदेशी संगठनों के साथ समन्वय करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, ताकि संगठित अपराध एवं आतंकवाद से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके।




