सुर्ख़ियों में क्यों?
सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसद की स्थायी समिति ने कई राज्यों की इस विफलता पर चिंता व्यक्त की है कि वे अनुसूचित जातियों (SCs) के खिलाफ होने वाले अत्याचारों से निपटने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित करने में विफल रहे हैं।
अनुसूचित जातियां (SCs) और उनकी पृष्ठभूमि क्या है?
- संविधान के अनुच्छेद 366 में 'अनुसूचित जाति' शब्द को परिभाषित किया गया है।
- अनुच्छेद 341 के तहत, राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वह राज्यपाल से परामर्श के बाद किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ समूहों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जातियों के रूप में अधिसूचित कर सकता है। संसद कानून बनाकर इस सूची में संशोधन कर सकती है।
- "अनुसूचित जाति" शब्द को पहली बार भारत शासन अधिनियम, 1935 में शामिल किया गया था।
जाति आधारित अत्याचारों से निपटने के लिए तंत्र
|
सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर स्थायी समिति की रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:
- SCs के खिलाफ अत्याचार रोकने में विफलता: कुछ राज्य नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित नहीं कर सके हैं।
- स्वच्छता कर्मी: नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (नमस्ते/ NAMASTE) योजना के तहत स्वच्छता से जुड़े कार्यों (सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई) में शून्य मृत्यु दर सुनिश्चित करने का लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है।
- उद्देश्यों/ लक्ष्यों का अभाव: कई योजनाओं जैसे प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) और अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (VCF) में भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया गया है।
- योजनाओं में धनराशि का व्यय न होना: उदाहरण के लिए- SCs हेतु लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा (SHRESHTA) योजना के मामले में, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा केंद्र को समय पर प्रस्ताव नहीं भेजने के कारण धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका है।
- उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) का लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई: अनुसूचित जातियों के लिए 2025-26 तक उच्चतर शिक्षा में 27 प्रतिशत GER का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। इसका कारण यह है कि कई राज्य अपनी वार्षिक कार्य योजना को कम करके प्रस्तुत कर रहे हैं या उनके प्रस्तुतिकरण में देरी कर रहे हैं।
- प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) का प्रभावी कार्यान्वयन नहीं: अधिक-से-अधिक गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में घोषित करने की आवश्यकता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में किया गया है।
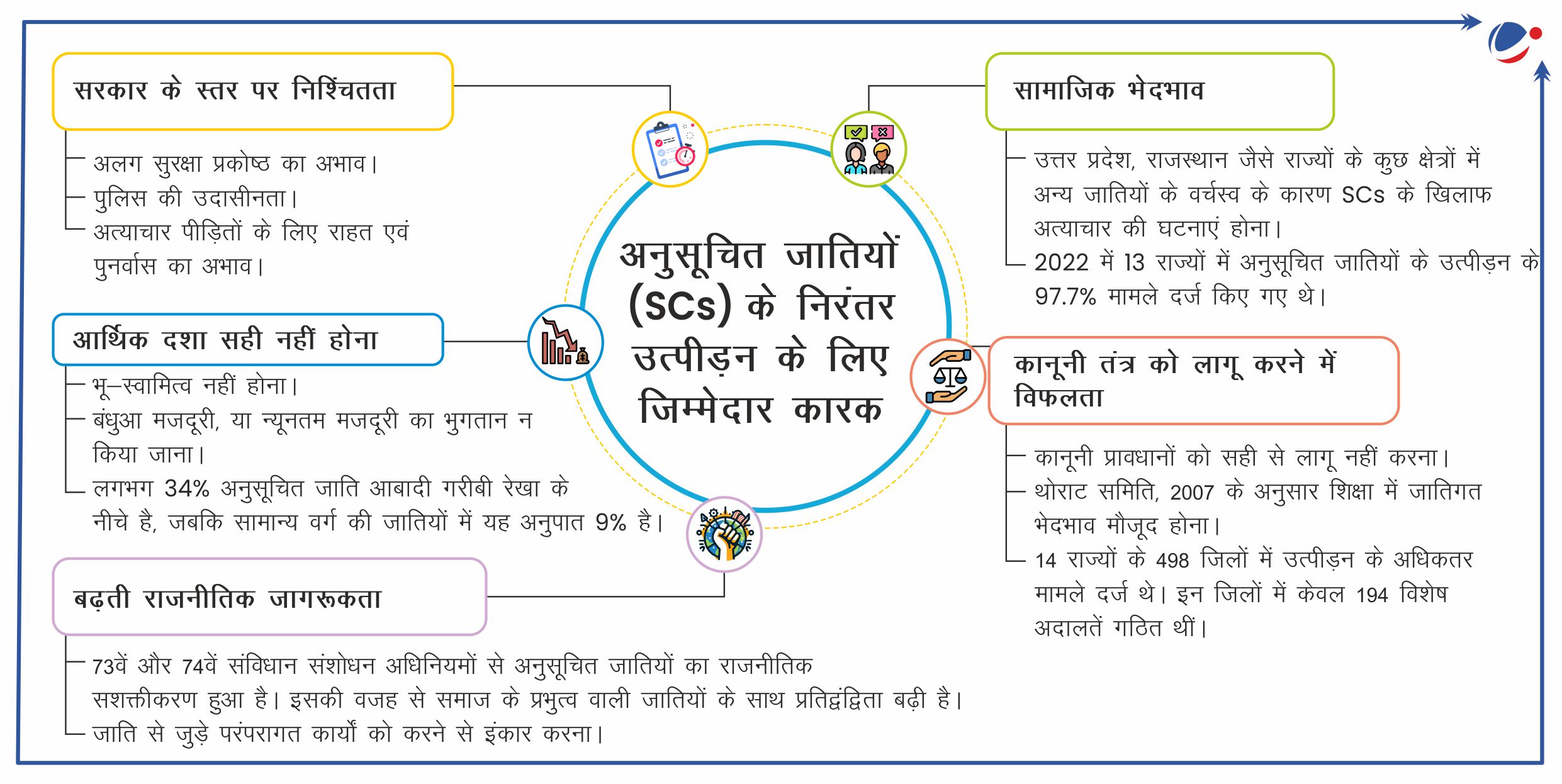
आगे की राह
- कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन का उपयोग: ऐसे राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश, जो कल्याणकारी योजनाओं को उचित रूप से लागू नहीं कर पाते हैं, उनसे सख्ती से निपटना चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी लाभार्थी को किसी भी योजना से वंचित न रखा जाए।
- सहकारी संघवाद की भावना के तहत, राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए अपने हिस्से के संसाधनों का सक्रिय रूप से योगदान करना चाहिए।
- परिमाणात्मक लक्ष्य तय करना: सभी कल्याणकारी योजनाओं के भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए, ताकि योजनाओं के कार्यान्वयन के किसी भी चरण में राज्यों या अन्य एजेंसियों द्वारा लापरवाही न बरती जाए।
- राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (NISD) को सशक्त बनाना: यह संस्थान मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम; सामाजिक रूप से हाशिए पर मौजूद समुदायों और कमजोर वर्गों के पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करता है।
- अनुसूचित जातियों के सबसे गरीब परिवारों की पहचान की प्रक्रिया: विविध योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना, जैसे "स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स (SHREYAS)" के तहत पात्र SC छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।
- कौशल प्रशिक्षण: "प्रधान मंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना (PM-DAKSH)" जैसी योजनाओं का बजट बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, स्वच्छता कर्मियों और अन्य वंचित समुदायों को इसका लाभ मिल सके।



