सुर्खियों में क्यों?
यह वर्ष आत्म-सम्मान आंदोलन के सौ वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। यह एक ऐसा आंदोलन था, जिसने दक्षिण भारत की राजनीतिक परिचर्चा को एक नई दिशा प्रदान की थी।
आत्म-सम्मान आंदोलन के विषय में
- आरंभ: इस आंदोलन की शुरुआत 1925 में ई.वी. रामासामी ने की थी। उन्हें आमतौर पर पेरियार के नाम से भी जाना जाता है।
- आत्म-सम्मान की अवधारणा: यह एक वैचारिक अवधारणा है, जिसका उद्देश्य एक ऐसे समतावादी समाज की स्थापना करना है, जो जाति, धर्म और लिंग पर आधारित सभी प्रकार के विभेद और द्वेष से मुक्त हो।
- विवरण: पेरियार द्वारा इसे 'अरिवु विदूतलाई इयक्कम' अर्थात् बौद्धिक मुक्ति का आंदोलन कहा गया।
- इस आंदोलन के उद्देश्यों का विवरण दो पुस्तिकाओं में किया गया है: नमतु कुरिक्कोल और तिरावितक कालक लेईयम्।
इस आंदोलन की कुछ विशेषताओं पर एक नजर
- सामाजिक उत्थान: इस आंदोलन ने विधवा पुनर्विवाह पर रोक, देवदासी प्रथा और जातीय भेदभाव का विरोध किया तथा सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया।
- आत्म-सम्मान विवाह: इसने बिना पुरोहितों के संपन्न हुए विवाहों को मान्यता दी, जिससे ब्राह्मण पुरोहितों के एकाधिकार को चुनौती मिली और अनुष्ठान संबंधी खर्चों में कमी आई।
- अंतर-जातीय विवाह: इसने बाल विवाह का विरोध किया तथा प्रेम विवाह और अंतर-जातीय विवाह को बढ़ावा दिया।
- आत्म-सम्मान सम्मेलन: 1929 में, पेरियार ने चेंगलपट्टु में पहला प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डब्ल्यू.पी.ए. सौंदर पांडियन ने की थी।
ई. वी. रामास्वामी (पेरियार) के बारे में (1879-1973)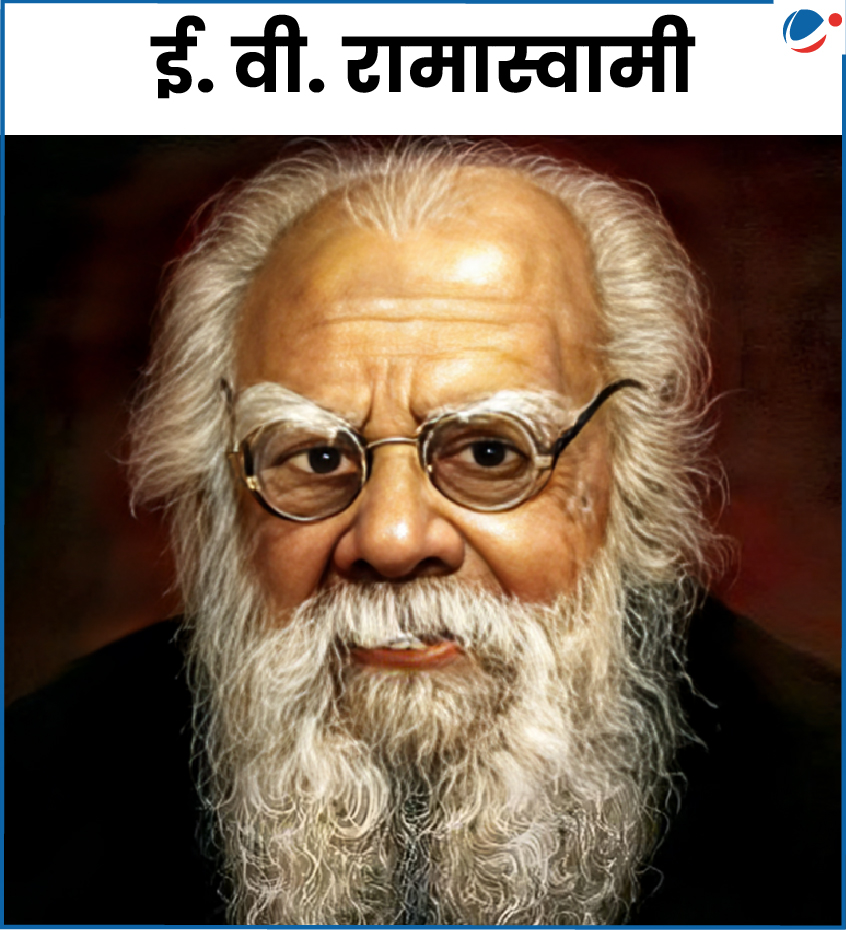
|
आत्म-सम्मान आंदोलन का महत्व
- ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती: इसने तमिलनाडु में उच्च जातियों को विशेष अधिकार देने वाली सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था की वैधता पर सवाल उठाया और जाति-विरोधी राजनीति की नींव रखी।
- महिला अधिकार: इसने विधवा पुनर्विवाह, संपत्ति के अधिकार, विवाह-विच्छेद के अधिकार और जनन संबंधी अधिकार जैसे सुधारों में अग्रणी भूमिका निभाई, जिससे लैंगिक न्याय की प्रारंभिक मिसालें कायम हुई।
- तर्कवाद को बढ़ावा: इसने तार्किक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अंधविश्वास के खंडन को बढ़ावा किया, जिससे सामाजिक दृष्टिकोणों के आधुनिकीकरण में मदद मिली।
- भाषा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण: इसने तमिल भाषा, द्रविड़ संस्कृति और स्थानीय पहचान को मजबूत किया।
- शिक्षा तक पहुँच: इसने वंचित समुदायों के लिए साक्षरता और शिक्षा की वकालत की, जिससे गैर-ब्राह्मणों को ज्ञान से दूर रखने की पारंपरिक प्रथा को चुनौती मिली।
- आर्थिक न्याय: इसने जातीय असमानता को आर्थिक शोषण के साथ जोड़ा तथा सरकारी नौकरियों एवं संसाधनों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग उठाई।
- राजनीतिक प्रभाव: इसने द्रविड़ पार्टियों (जस्टिस पार्टी, DMK, AIADMK) के उत्थान हेतु वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की तथा तमिलनाडु की विशिष्ट कल्याणकारी राजनीति को दिशा दी।
- वैश्विक प्रभाव: इसने मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों में तमिल प्रवासियों के आंदोलनों को प्रेरणा दी, जिससे विदेशों में उनकी पहचान और अधिकारों के प्रति चेतना सुदृढ़ हुई।
अन्य समाज सुधार एवं जाति-विरोधी आंदोलन
- सत्यशोधक समाज (1873): इसकी स्थापना महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले द्वारा ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का मुकाबला करने, निम्न जातियों एवं महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करने तथा धार्मिक कट्टरता पर प्रश्न उठाने के उद्देश्य से की गई थी।
- श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन (1903): इसे नारायण गुरु द्वारा शुरू किया गया, जिन्होंने मानवता के लिए "एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर" के सिद्धांत का प्रचार किया। साथ ही, इन्होंने केरल में एझावा समुदाय के मध्य जातीय भेदभाव का भी विरोध किया।
- बहिष्कृत हितकारिणी सभा (1924): इसे डॉ. बी. आर. अंबेडकर द्वारा दलित समुदाय के शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु गठित किया गया था।
- वायकोम सत्याग्रह (1924-25): यह त्रावणकोर (केरल) में शोषित जातियों के लिए मंदिर के आस-पास की सड़कों का उपयोग करने के अधिकार की मांग हेतु एक सामाजिक आंदोलन था।
- अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ (1930): यह डॉ. बी. आर. अंबेडकर द्वारा अनुसूचित जातियों (दलितों) के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था।
- अखिल भारतीय अस्पृश्यता-विरोधी लीग (1932): इसे समाज से अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए गांधी जी द्वारा गठित किया गया था।
निष्कर्ष
आत्म-सम्मान आंदोलन दक्षिण भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने जाति व्यवस्था और धार्मिक कट्टरता को चुनौती दी। इस आंदोलन ने तर्कवाद, लैंगिक न्याय और सामाजिक समानता की नींव रखी, जिससे तमिल समाज और राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया। आज भी इसका प्रभाव सामाजिक सुधार, समावेशन और सशक्तीकरण संबंधी आंदोलनों को प्रेरित करता है।



