परिचय
सुप्रीम कोर्ट ने "इंडियाज गॉट लैटेंट" नामक यूट्यूब शो में अश्लील टिप्पणियों से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल से अनुरोध किया कि वे ऑनलाइन दिखाए जाने वाले भद्दे कंटेंट पर नियंत्रण के लिए एक संतुलित नियामक उपाय प्रस्तुत करें, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Free Speech) पर संतुलन बना रहे।
इसके साथ ही, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने OTT (ओवर द टॉप) प्लेटफॉर्म्स को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वे ऐसा कोई भी कंटेंट प्रसारित न करें जो कानून द्वारा प्रतिबंधित हो। मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म्स से "सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021" के अनुसार आयु-आधारित वर्गीकरण का सख्ती से पालन करने और परिपक्व कंटेंट के लिए आयु-नियंत्रण (Age-gating) की अनिवार्यताओं को लागू करने का निर्देश दिया है। सरल शब्दों में, मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म्स से कहा है कि वे 2021 के नियमों के अनुसार कंटेंट को उम्र के हिसाब से बांटें और बड़ों के लिए बनी सामग्री को देखने के लिए उम्र की पुष्टि करने का एक सिस्टम तैयार करें।
अश्लीलता (Obscenity) क्या है?
'अश्लील' का मतलब है ऐसी चीजें जो देखने या सुनने में बहुत बुरी लगें या जिनका मकसद लोगों को यौन रूप से उत्तेजित करना हो। ऐसी चीजें लोगों में गलत इच्छाएं या वासना पैदा कर सकती हैं।
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट स्ट्रीमिंग में प्रमुख हितधारक
| प्रमुख हितधारक | संबद्ध हित |
| कंटेंट क्रिएटर्स और कलाकार |
|
| डिजिटल प्लेटफॉर्म |
|
| सरकार एवं नियामक निकाय |
|
| समाज |
|
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता को विनियमित करने की आवश्यकता क्यों?
- सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण: अनियंत्रित अश्लील कंटेंट की अनुमति देने से समाज का नैतिक चरित्र कमजोर होता है, तथा अनादर और नैतिक पतन को बढ़ावा मिलता है।
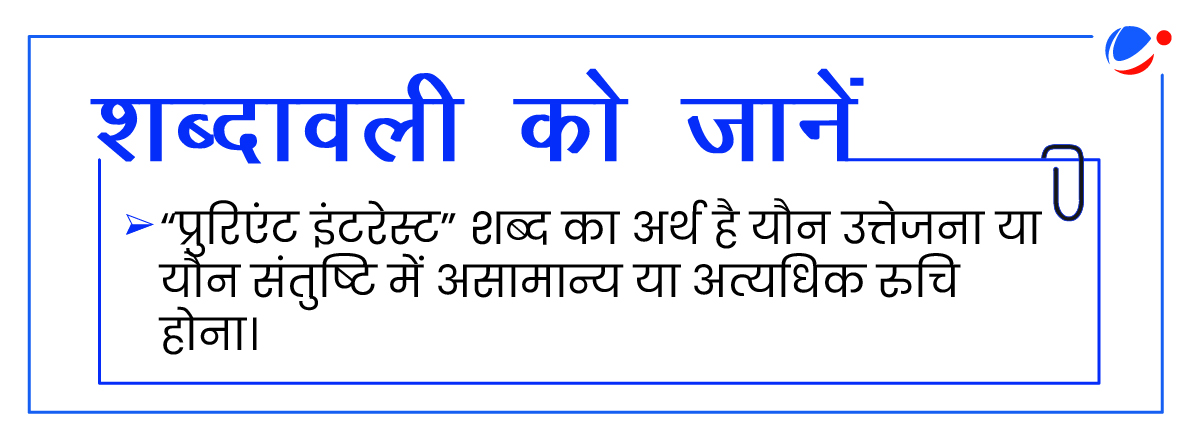
- उदाहरण के लिए- 2021 की "बुल्ली बाई" ऐप की घटना में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की तस्वीरों की ऑनलाइन नीलामी की गई थी। इस घटना ने दिखाया कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग महिलाओं को अपमानित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे सख्त नियमन की आवश्यकता उजागर हुई।
- मानव गरिमा की रक्षा: कांट का मानना था कि मनुष्यों को कभी भी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। लोगों को कामुक रुचि की वस्तु तक सीमित कर देने वाले कंटेंट गरिमा और व्यक्तिगत स्वायत्तता के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं।
- अश्लीलता के सामान्यीकरण से बचना: जॉन स्टुअर्ट मिल का हानि सिद्धांत सुझाव देता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से समाज को हानि नहीं होनी चाहिए।
- लगातार अश्लील कंटेंट देखने से व्यक्ति असंवेदनशील हो सकता है, सहानुभूति खत्म हो सकती है और हानिकारक रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिल सकता है।
- प्लेटफॉर्म्स की नैतिक जिम्मेदारी: उपयोगितावाद का दर्शन कहता है कि कोई भी कार्य समाज के अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम कल्याण को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। इस प्रकार, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को नैतिक रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका कंटेंट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखें। इससे एक सुरक्षित डिजिटल परिवेश को बढ़ावा मिलता है।
- संवैधानिक नैतिकता को कायम रखना: संवैधानिक नैतिकता सामाजिक न्याय और समानता जैसे आधारभूत मूल्यों की रक्षा करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि डिजिटल कंटेंट इन सिद्धांतों के अनुरूप हो।
- अनुच्छेद 19(2) प्रावधान करता है कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। ऐसे अधिकारों पर लोक व्यवस्था, सदाचार या शालीनता, नैतिकता, अपराध के लिए उकसाने सहित विभिन्न आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
अश्लील डिजिटल कंटेंट को विनियमित करने में नैतिक मुद्दे
- अस्पष्टता और व्यक्तिपरकता (Vagueness and Subjectivity): वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि सदाचार और नैतिकता समय और क्षेत्रों के अनुसार बदलती रहती है। हालांकि, इंडियाज गॉट लैटेंट में इस्तेमाल की गई भाषा अनुचित थी, लेकिन यह अपराध की कानूनी परिभाषा को पूरा नहीं कर सकती है, क्योंकि इस तरह की भाषा समाज में रोजमर्रा की बातचीत में आम है।
- सेंसरशिप बनाम उचित प्रतिबंध: हालांकि, कानून नैतिकता की रक्षा करते हैं, लेकिन अत्यधिक विनियमन रचनात्मकता को प्रभावित कर सकता है। चूंकि अश्लीलता व्यक्तिपरक और निरंतर परिवर्तनीय है, इसलिए अत्यधिक प्रतिबंध मीडिया में विविध दृष्टिकोणों को सीमित कर सकते हैं।
- उदाहरण के लिए- 2024 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने "अश्लील और अभद्र" कंटेंट करार देते हुए 18 OTT प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसे मनमाना माना गया और कुछ ने इसे रचनात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने वाला बताया।
- बदलते सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक संवेदनशीलता: अश्लीलता एक सांस्कृतिक अवधारणा है जो समय के साथ बदलती रहती है। खजुराहो और कोणार्क के प्राचीन मंदिरों में कामुक मूर्तियां उत्कीर्णित हैं, लेकिन अगर वर्तमान में इस तरह की मूर्तियां लगाने/ उकेरने का प्रयास किया जाए तो सेंसरशिप का सामना करना पड़ सकता है।
- सत्ता की गतिशीलता: प्रश्न उठता है कि यह तय करने का अधिकार किसे होगा कि कौन सा कंटेंट स्वीकार्य है? सेंसरशिप का दुरुपयोग हाशिए पर मौजूद समुदायों के खिलाफ किया जा सकता है।
- एजेंसी और संरक्षकवाद (Paternalism): कंटेंट के उपयोगकर्ताओं को हानिकारक कंटेंट से बचाने और अपना कंटेंट चुनने की उनकी स्वायत्तता का सम्मान करने के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
- अत्यधिक विनियमन से यह धारणा बन सकती है कि उपयोगकर्ता स्वयं कंटेंट के संबंध में अपनी पसंद के बारे में सही निर्णय नहीं ले सकते हैं।
- अश्लीलता का विनियमन बनाम कलात्मक स्वतंत्रता: सार्वजनिक नैतिकता की रक्षा के लिए सेंसरशिप और कलाकारों की रचनात्मक अभिव्यक्ति के बीच संघर्ष बना रहता है।
- उदाहरण के लिए- मकबूल फिदा हुसैन बनाम राज कुमार पांडे मामले में, न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि केवल नग्नता (Nudity) मात्र से कोई कंटेंट अश्लील नहीं हो जाता। इससे यह स्पष्ट हुआ कि कलात्मक अभिव्यक्ति और सामाजिक मानकों के बीच नैतिक दुविधा बनी रहती है।
अश्लीलता वाले कंटेंट पर प्रतिबंध के संबंध में कानून और नैतिकता के बीच संघर्षभारतीय न्यायशास्त्र में अश्लीलता पर कानूनी प्रतिबंध और बदलते नैतिक मानकों के बीच संघर्ष एक जटिल चुनौती के रूप में उभरा है। यह संघर्ष मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होता है: स्पष्ट परिभाषा के बिना कानूनी ढांचा
विकसित होती न्यायिक व्याख्या
इन सभी बातों के अलावा, एक ही अपराध के लिए कई FIR दर्ज करने की बढ़ती प्रवृत्ति को उत्पीड़न के रूप में आलोचना झेलनी पड़ी है, क्योंकि यह आरोपी के खिलाफ अनुचित पूर्वाग्रह पैदा करता है और उनके निष्पक्ष बचाव के अधिकार को कमजोर करता है। वहीं लोक संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कंटेंट को आलोचना या बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता हैं, लेकिन अत्यधिक कानूनी कार्रवाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण का खतरा उत्पन्न करती है। |
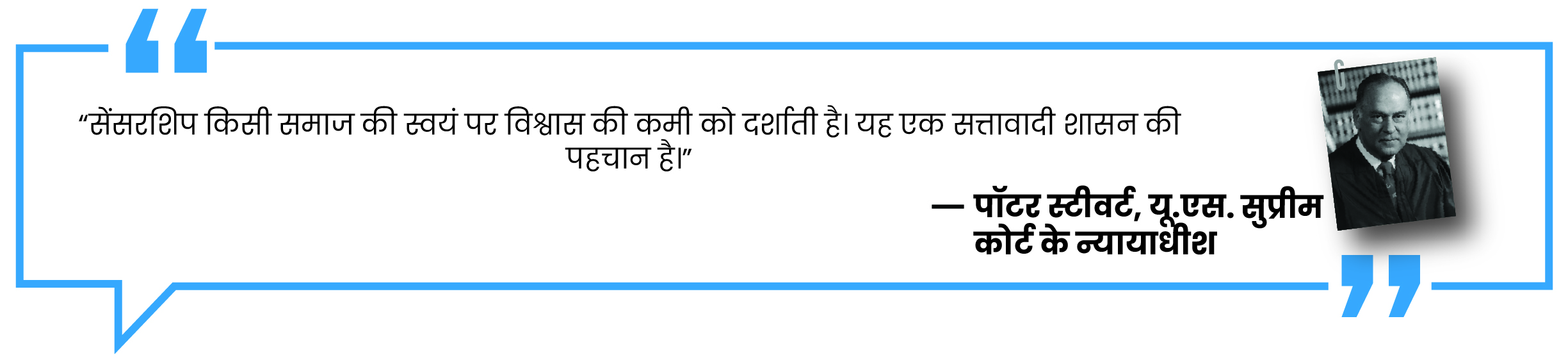
आगे की राह
- न्याय एवं वस्तुनिष्ठता (Justice & Objectivity): भारत की सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट एवं सुसंगत दिशा-निर्देश तैयार किए जाने चाहिए, जिससे पक्षपात या न्यायिक निर्णयों में व्यक्तिनिष्ठता/ व्यक्तिपरकता को रोका जा सके।
- जवाबदेही एवं जिम्मेदारी: OTT कंटेंट, डिजिटल समाचार और उभरती तकनीकों को विनियमित करने के लिए एक ब्रॉडकास्टिंग विधेयक लाया जाना चाहिए, जिससे नैतिक और सामाजिक रूप से उत्तरदायी मीडिया सुनिश्चित हो सके।
- नैतिक कंटेंट क्रिएशन को प्रोत्साहित करना: सामाजिक उत्तरदायित्व और सांस्कृतिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करने के लिए, स्व-विनियमन और ऐसी नैतिक स्टोरीटेलिंग को बढ़ावा देना चाहिए, जो सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक सम्मान को प्रतिबिंबित करती हो।
- सशक्तीकरण एवं सूचित विकल्प: युवाओं को मीडिया एथिक्स, जिम्मेदारीपूर्ण कंटेंट व्यवहार और ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम लागू करना चाहिए।
निष्कर्ष
अश्लीलता अत्यधिक व्यक्तिपरक है, जो संस्कृतियों और समय के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए, एक जिम्मेदार डिजिटल मीडिया स्पेस बनाने के लिए कानूनी स्पष्टता, स्व-नियमन, लोक जागरूकता और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होती है। न्याय, गरिमा, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे नैतिक मूल्यों को कायम रखते हुए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रचनात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बना सकते हैं।
अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिएडिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती अश्लीलता (Obscenity) और अपशब्दों (Profanity) को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिया है कि वे ऑनलाइन कंटेंट में "गंदी भाषा" और "अश्लीलता" पर अंकुश लगाने के उपायों का प्रस्ताव करें। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नैतिक मानकों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इस संदर्भ में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:
|




